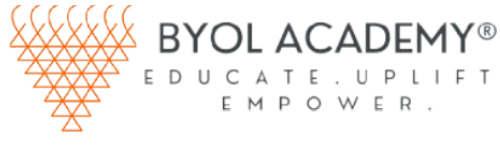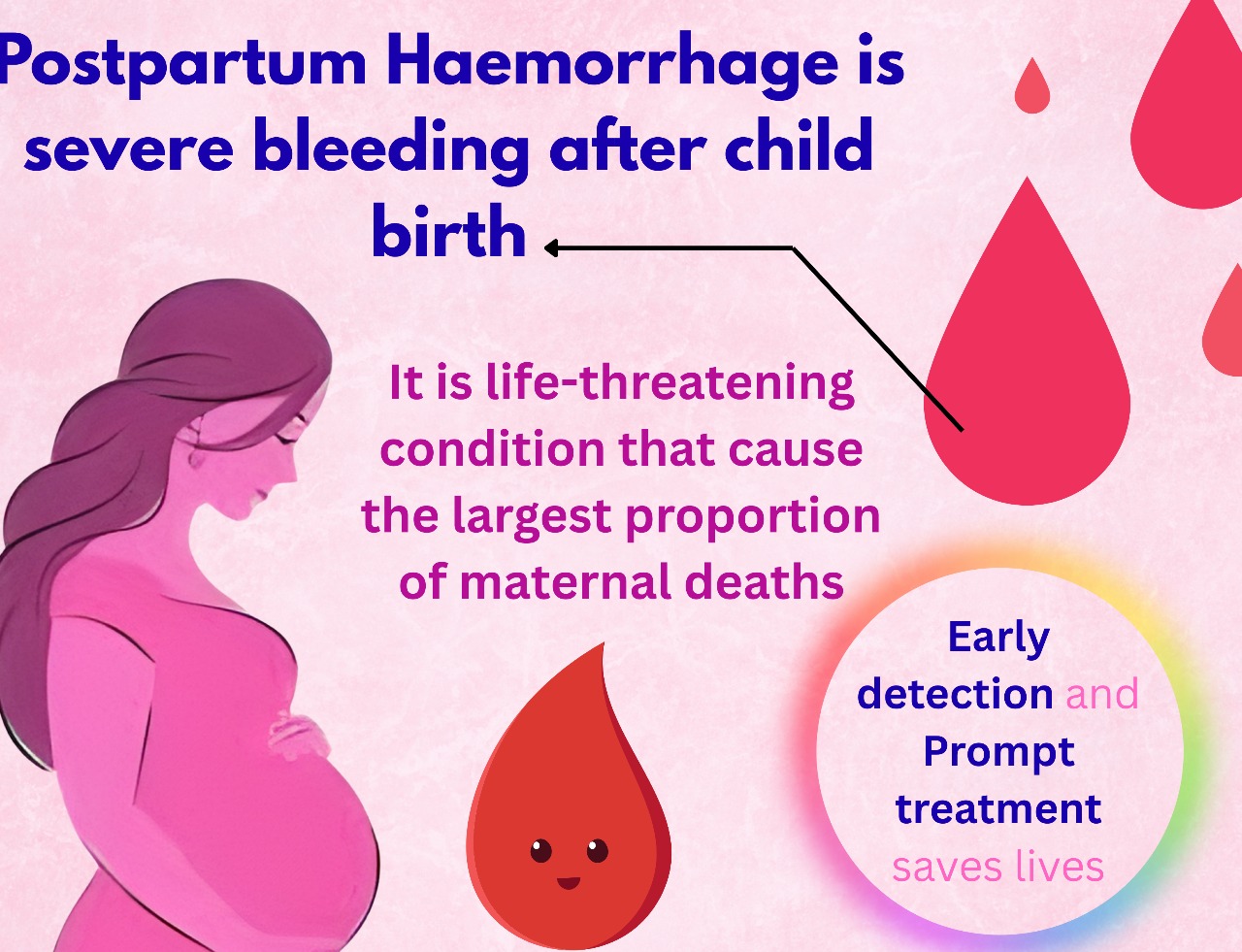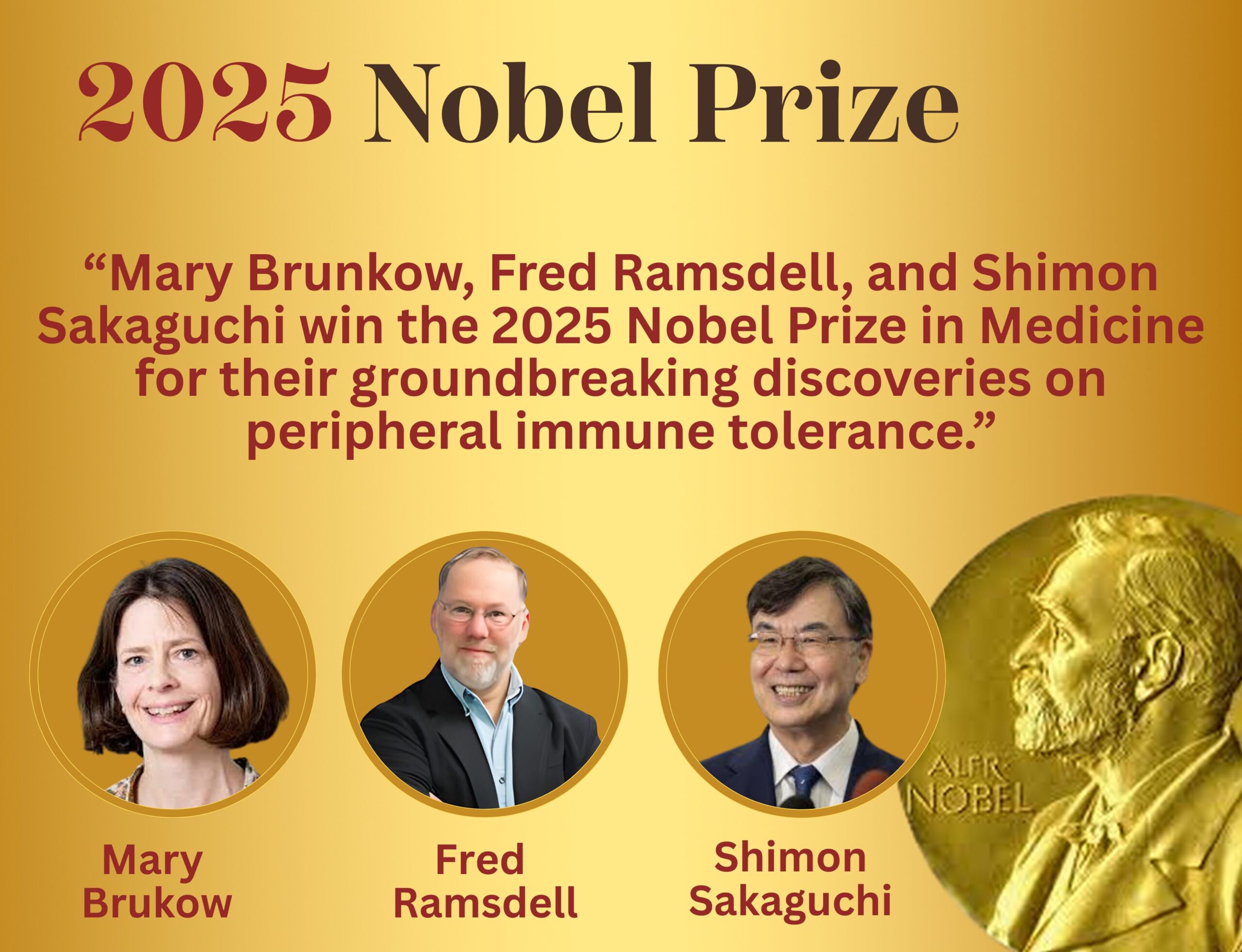एक वित्तीय संस्थान (FI) एक ऐसा संगठन है जो मौद्रिक लेनदेन, जैसे जमा, ऋण, निवेश और मुद्रा विनिमय के व्यवसाय में लगा हुआ है। ये संस्थान वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं जो अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को प्रबंधित करने में मदद करते हैं और वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। वे बचत करने वालों और उधार लेने वालों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जिससे पूरे अर्थव्यस्था में धन का कुशल आवंटन (efficient allocation) हो पाता है। वित्तीय संस्थानों के प्रकारों में बैंक, क्रेडिट यूनियन, बीमा कंपनियाँ, ब्रोकरेज फर्म और परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म (asset management firms) शामिल हैं। अपने संचालन के माध्यम से, वित्तीय संस्थान व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को अपने वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने, जोखिमों का आकलन और उन्हें कम करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं।
- उदाहरण के लिए, बैंक जमाकर्ताओं (जो बैंक को पैसा उधार देते हैं) और उधारकर्ताओं (जिन्हें बैंक पैसा उधार देता है) के बीच मध्यस्थ होते हैं। वे पैसे वाले लोगों से पैसा लेते हैं जिसे जमा कहते हैं, जमा को पूल करते हैं, और जिन्हें धन की आवश्यकता होती है उन्हें उधार देते हैं। बीमा कंपनियाँ प्रीमियम भुगतान के बदले किसी संपत्ति या व्यक्ति को संभावित नुकसान या क्षति के लिए कवरेज प्रदान करती हैं। ब्रोकरेज फर्म एक खरीदार और एक विक्रेता के बीच वित्तीय प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करती हैं। निवेश डीलर ग्राहकों को निवेश सलाह और सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- वित्तीय संस्थान (FIs) आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, जोखिमों को प्रबंधित करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं। यहाँ भारत के एक हालिया उदाहरण के साथ, उनकी बहुआयामी भूमिकाओं के बारे में बताया गया है:
संसाधन आवंटन (Resource Allocation):-
- 🔄 वित्तीय संस्थान (FIs) बचत को निवेश में परिवर्तित करते हैं, जो पूंजी निर्माण (capital formation) और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
क्रेडिट प्रावधान (Credit Provision):-
- 🏦 क्रेडिट बढ़ाकर, वे खर्च और निवेश को बढ़ावा देते हैं, और व्यक्तियों तथा संगठनों की तरलता (liquidity) संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं।
जोखिम प्रबंधन (Risk Management):-
- 🛡️ बीमा और डेरिवेटिव्स की पेशकश करते हुए, FIs वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं।
भुगतान प्रणाली (Payment Systems):-
- 💳 वे सुचारू लेनदेन सुनिश्चित करते हैं, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
परिसंपत्ति प्रबंधन (Asset Management):-
- 📈 ग्राहकों की ओर से धन का प्रबंधन करके, वे धन संचय (wealth accumulation) और वित्तीय योजना बनाने में मदद करते हैं।
नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance):-
- 📜 नियमों का पालन करना स्थिरता सुनिश्चित करता है, हितधारकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देता है।
वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion):-
- 🌐 बिना बैंक खाते वाले लोगों को सेवाएँ प्रदान करके, वे गरीबी कम करने और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं।
तकनीकी नवाचार (Technological Innovation):-
- 🖥️ फिनटेक नवाचारों (fintech innovations) को अपनाकर, वे दक्षता बढ़ाते हैं, लागत कम करते हैं और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाते हैं।
बाजार तरलता (Market Liquidity):-
- 🔄 बाजार निर्माता के रूप में कार्य करके, वे तरलता प्रदान करते हैं, बाजार की दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
सतत वित्त (Sustainable Finance):-
- 🌿 वे तेजी से पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी निवेशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिल रहा है।
- उदाहरण: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) – डिजिटल परिवर्तन
- SBI, भारत में एक प्रमुख वित्तीय संस्थान, ने अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। उदाहरण के लिए, YONO (You Only Need One) ऐप का लॉन्च एक ही मंच के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग, खरीदारी, निवेश और बीमा की सुविधा प्रदान करता है।
SBI द्वारा समग्र पूर्ति (Holistic Fulfillment by SBI):-
- 📲 डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion): YONO ऐप बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को उपयोगकर्ताओं की उंगलियों पर लाता है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है
- 🛍️ लेनदेन की सुविधा (Facilitating Transactions): विभिन्न वित्तीय जरूरतों के लिए एक-स्टॉप समाधान प्रदान करके, SBI लेनदेन को सरल बनाता है, जो भुगतान की सुविधा में FIs के सार का प्रतीक है।
- 🌱 सतत वित्त (Sustainable Finance): SBI ने ग्रीन फाइनेंसिंग (green financing) में भी कदम रखा है, जो FIs की स्थिरता को बढ़ावा देने में विकसित भूमिका को रेखांकित करता है।
यह इस बात का उदाहरण है कि SBI जैसे आधुनिक वित्तीय संस्थान न केवल पारंपरिक भूमिकाओं को पूरा कर रहे हैं बल्कि समकालीन जरूरतों के अनुकूल भी हो रहे हैं, जो वित्तीय संस्थानों द्वारा सेवा किए जाने वाले उद्देश्यों की समग्र पूर्ति को दर्शाता है। डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से, SBI वित्तीय समावेशन सुनिश्चित कर रहा है, सहज लेनदेन की सुविधा प्रदान कर रहा है, और सतत वित्त में कदम रख रहा है, जो आधुनिक आर्थिक परिदृश्य में वित्तीय संस्थानों द्वारा निभाई जाने वाली विविध, महत्वपूर्ण भूमिकाओं को दर्शाता है।
बैंक और प्रतिभूतियाँ (Banks and Securities):-
बैंक और प्रतिभूति फर्म वित्तीय क्षेत्र के अभिन्न अंग हैं, प्रत्येक अद्वितीय लेकिन पूरक भूमिकाओं की सेवा करता है। यहाँ उनके कार्यों का एक उदाहरण भारत के एक हालिया उदाहरण के साथ दिया गया है:
बैंक:-
- पूंजी संरक्षक (Capital Custodians): 🏦 बैंक जमा राशि की सुरक्षा करते हैं, व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए एक सुरक्षित भंडार प्रदान करते हैं।
- क्रेडिट प्रावधान (Credit Provision): 💳 ऋण बढ़ाकर, वे व्यक्तिगत और वाणिज्यिक व्यय की सुविधा प्रदान करते हैं, आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करते हैं।
- भुगतान प्रसंस्करण (Payment Processing): 💸 वे लेन-देन की एक विशाल सरणी (vast array) को संभालते हैं, जिससे सुचारू वित्तीय आदान-प्रदान सुनिश्चित होता है।
- मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Policy Transmission): 🎛️ बैंक मौद्रिक नीति के संचरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो समग्र आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करता है।
- जोखिम प्रबंधन (Risk Management): 🛡️ बीमा और डेरिवेटिव जैसे विभिन्न उत्पादों के माध्यम से, वे वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन में मदद करते हैं।
- वित्तीय सलाहकार (Financial Advisory): 🧠 सलाहकार सेवाएँ प्रदान करते हुए, बैंक ठोस वित्तीय निर्णय लेने में सहायता करते हैं।
प्रतिभूति फर्म (Securities Firms):-
- पूंजी बाजार तक पहुंच (Capital Market Access): 📈 वे पूंजी बाजारों तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे इक्विटी और ऋण के माध्यम से धन जुटाने में सहायता मिलती है।
- निवेश सेवाएँ (Investment Services): 📊 निवेश विकल्प प्रदान करते हुए, वे परिसंपत्ति संचय (asset accumulation) और धन प्रबंधन (wealth management) में मदद करते हैं।
- बाजार निर्माण (Market Making): 🔄 प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचकर, वे तरलता प्रदान करते हैं, जिससे बाजार की दक्षता सुनिश्चित होती है।
- जोखिम विविधीकरण (Risk Diversification): 🌐 विभिन्न वित्तीय साधनों के माध्यम से, वे जोखिम विविधीकरण को सक्षम करते हैं।
- अनुसंधान और विश्लेषण (Research and Analysis): 🔍 बाजार की जानकारी प्रदान करते हुए, वे निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में सहायता करते हैं।
- नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance): 📜 बाजार नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, बाजार की अखंडता को बनाए रखना।
- उदाहरण: कोटक महिंद्रा बैंक और उसकी प्रतिभूति शाखा
कोटक महिंद्रा बैंक, भारत में एक उल्लेखनीय बैंक, अपनी प्रतिभूति शाखा, कोटक सिक्योरिटीज के साथ, बैंकों और प्रतिभूति फर्मों की समग्र भूमिका का उदाहरण है।
कोटक संस्थाओं द्वारा समग्र पूर्ति (Holistic Fulfillment by Kotak Entities):-
- 📲 डिजिटल नवाचार (Digital Innovation): कोटक ने अपने ग्राहकों के लिए पहुंच और सुविधा को बढ़ाते हुए डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ शुरू कीं।
- 📊 निवेश सेवाएँ (Investment Services): कोटक सिक्योरिटीज धन सृजन में व्यक्तियों की सहायता करते हुए निवेश विकल्पों की अधिकता प्रदान करती है।
- 🌿 सतत निवेश (Sustainable Investing): बैंक ने सतत निवेश के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है, जो वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित है।
- 🎓 बाजार शिक्षा (Market Education): विभिन्न पहलों के माध्यम से, वे निवेशकों को शिक्षित करते हैं, एक अच्छी तरह से सूचित बाजार को बढ़ावा देते हैं।
व्यापक उद्देश्य से जुड़ते हुए, कोटक महिंद्रा बैंक और कोटक सिक्योरिटीज प्रदर्शित करते हैं कि कैसे वित्तीय संस्थान पारंपरिक बैंकिंग क्षेत्र और गतिशील पूंजी बाजारों के बीच एक संबंध के रूप में कार्य करते हैं। उनकी अभिनव सेवाएँ, स्थिरता का पालन, और निवेशक शिक्षा पर ध्यान एक आर्थिक रूप से मजबूत और वित्तीय रूप से साक्षर समाज के पोषण में वित्तीय संस्थानों द्वारा निभाई जाने वाली बहु-आयामी भूमिकाओं को दर्शाती हैं। अपने विविध प्रस्तावों के माध्यम से, वे वित्तीय समावेशन, आर्थिक विकास और बाजार विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, जो आधुनिक आर्थिक ढांचे में वित्तीय संस्थानों के सार को दर्शाते हैं।
वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों और प्रतिभूतियों के लिए कुछ सिद्धांत (Some theories for FI like Banks and securities):-
वित्तीय संस्थानों के रूप में बैंकों और प्रतिभूतियों से जुड़े सिद्धांत पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास में उनकी भूमिका को समझने के लिए एक ढाँचा प्रदान करते हैं। बेहतर विज़ुअलाइज़ेशन के लिए इमोजी के साथ समर्थित कुछ प्रमुख सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं:
- वित्तीय मध्यस्थता सिद्धांत (Financial Intermediation Theory):-
- 🔄 बैंक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जमाकर्ताओं से उधारकर्ताओं तक बचत को प्रसारित करते हैं, पूंजी निर्माण की सुविधा प्रदान करते हैं, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
- तरलता वरीयता सिद्धांत (Liquidity Preference Theory):-
- 💧 लोग तरलता पसंद करते हैं, और बैंक अपनी उधार और जमा सेवाओं के माध्यम से तरलता वरीयता को दीर्घकालिक निवेश जरूरतों के साथ संतुलित करने का एक तरीका प्रदान करते हैं।
- मोदिग्लिआनी-मिलर प्रमेय (Modigliani-Miller Theorem):-
- 🏢 एक आदर्श बाजार में, एक फर्म का मूल्य इस बात से अप्रभावित रहता है कि इसे कैसे वित्तपोषित किया जाता है, चाहे इक्विटी (प्रतिभूतियों) या ऋण (बैंकों से ऋण) के माध्यम से।
- कुशल बाजार परिकल्पना (Efficient Market Hypothesis – EMH):-
- 📊 प्रतिभूति बाजारों को कुशल के रूप में देखा जाता है, जिसमें कीमतें सभी उपलब्ध जानकारी को दर्शाती हैं, जिससे पूंजी को इसके सबसे उत्पादक उपयोगों के लिए आवंटित करने में सहायता मिलती है।
- पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल (Capital Asset Pricing Model – CAPM):-
- 📈 अपेक्षित प्रतिफल और जोखिम के बीच संबंध को समझने में मदद करता है, प्रतिभूति बाजारों में निवेश निर्णयों का मार्गदर्शन करता है।
- पेकिंग ऑर्डर सिद्धांत (Pecking Order Theory):-
- 🐦 फर्मों के पास वित्तपोषण के लिए एक वरीयता क्रम होता है, जो अक्सर आंतरिक वित्तपोषण, फिर ऋण (बैंक ऋण), और अंत में इक्विटी (प्रतिभूतियों) को पसंद करते हैं, जो धन की लागत और उपलब्धता पर आधारित होता है।
- एजेंसी सिद्धांत (Agency Theory):-
- 👥 प्रबंधकों और शेयरधारकों के बीच के संघर्षों को संबोधित करता है, जो बैंकों और प्रतिभूति दोनों बाजारों में पूंजी संरचना निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
- क्वांटम वित्तीय प्रणाली (Quantum Financial System – QFS):-
- 🔐 एक सैद्धांतिक ढाँचा जो परिसंपत्तियों के कुशल हस्तांतरण के लिए एक अत्यधिक सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय प्रणाली का सुझाव देता है।
- व्यवहार वित्त सिद्धांत (Behavioral Finance Theory):-
- 🧠 यह जाँच करता है कि मनोवैज्ञानिक कारक बाजार के परिणामों और वित्तीय निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करते हैं, जिससे बैंकिंग और प्रतिभूति दोनों बाजारों पर प्रभाव पड़ता है।
बाजार सूक्ष्म संरचना सिद्धांत (Market Microstructure Theory):-
🎛️ यह पता लगाता है कि बाजार तंत्र, व्यापार नियम, और सूचना विषमता (information asymmetry) प्रतिभूतियों की कीमतों और व्यापार व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है।
- सूचना विषमता सिद्धांत (Information Asymmetry Theory):-
- 📑 यह जाँच करता है कि सूचना तक असमान पहुँच बैंकिंग और प्रतिभूति दोनों क्षेत्रों में बाजार लेनदेन और पूंजी आवंटन को कैसे प्रभावित करती है।
- पूंजी निर्माण में अनुप्रयोग (Application in Capital Formation):-
- इन सिद्धांतों का संलयन (fusion) इस बात की एक सूक्ष्म समझ प्रदान करता है कि बैंक और प्रतिभूति फर्म वित्तीय संस्थानों के रूप में कैसे काम करते हैं, पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
- उदाहरण के लिए, वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से, बैंक बचत जुटाते हैं और उन्हें निवेश में प्रसारित करते हैं, जबकि प्रतिभूति बाजार, EMH और CAPM द्वारा निर्देशित, विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी को कुशलता से आवंटित करने में मदद करते हैं। ये सैद्धांतिक ढाँचे सामूहिक रूप से बैंकों, प्रतिभूति बाजारों, और व्यापक आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहजीवी संबंध को स्पष्ट करते हैं, पूंजी निर्माण के पोषण, बाजार दक्षता को बढ़ाने, और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।
पूंजी या नकदी प्रवाह के निर्माण में प्रतिभूतियों की सहायता (Securities assistance in creation of Capital or cash flow):-
प्रतिभूतियाँ, जिनमें स्टॉक, बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधन शामिल हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर पूंजी और नकदी प्रवाह में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ प्रासंगिक उदाहरणों के साथ कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं:
- पूंजी जुटाना (Capital Raising):-
- 📈 प्रतिभूतियाँ व्यवसायों को जनता को शेयर या बॉन्ड जारी करके पूंजी जुटाने के लिए एक चैनल प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, Zomato और Paytm जैसी कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs) ने पर्याप्त निवेश आकर्षित किया, जिससे उन्हें संचालन का विस्तार करने के लिए पूंजी मिली।
- निवेश के अवसर (Investment Opportunities)
- 🏦 वे व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश के रास्ते प्रदान करते हैं, जिससे धन सृजन और बचत सक्षम होती है।
- बाजार तरलता (Market Liquidity)
- 🔄 स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों का व्यापार तरलता की सुविधा प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर धन को आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सके।
- मूल्य खोज (Price Discovery)
- 🎯 प्रतिभूति बाजार परिसंपत्तियों की मूल्य खोज में मदद करते हैं, जो निवेशकों द्वारा कंपनियों के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाते हैं।
- जोखिम प्रबंधन (Risk Management)
- 🛡️ डेरिवेटिव जैसी प्रतिभूतियाँ बाजार जोखिमों के खिलाफ बचाव (hedging) की अनुमति देती हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता में सहायता मिलती है।
- आर्थिक संकेतक (Economic Indicators)
- 📊 प्रतिभूति बाजारों का प्रदर्शन अक्सर आर्थिक स्वास्थ्य और निवेशक विश्वास का एक संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- संसाधन आवंटन (Resource Allocation)
- 🔄 कुशल प्रतिभूति बाजार उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में धन प्रसारित करके संसाधनों के इष्टतम आवंटन में मदद करते हैं।
- कॉर्पोरेट प्रशासन (Corporate Governance)
- 🏢 प्रतिभूति एक्सचेंजों पर लिस्टिंग के लिए अक्सर सख्त प्रशासन और प्रकटीकरण मानकों (disclosure standards) का पालन करने की आवश्यकता होती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Policy Transmission):-
🎛️ प्रतिभूति बाजार अर्थव्यवस्था के माध्यम से मौद्रिक नीति प्रभावों के संचरण में एक भूमिका निभाते हैं।
- वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion):-
- 🌐 डिजिटल प्लेटफॉर्म के आगमन के साथ, आबादी का एक व्यापक वर्ग अब प्रतिभूति बाजारों में भाग ले सकता है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है।
- नवाचार और उद्यमिता (Innovation and Entrepreneurship):-
- 🚀 प्रतिभूति बाजारों के माध्यम से पूंजी तक पहुंच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देती है, जिससे आर्थिक विकास होता है।
- वैश्विक पूंजी तक पहुंच (Global Capital Access):-
- 🌐 भारतीय कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिभूतियाँ जारी करके वैश्विक पूंजी तक पहुंच बना सकती हैं, और इसी तरह, विदेशी कंपनियाँ भारत में पूंजी जुटा सकती हैं।
- नकदी प्रवाह और पूंजी सुधार से जुड़ना (Connecting to Cash Flow and Capital Betterment):-
- प्रतिभूतियों के माध्यम से पूंजी जुटाने, जोखिम प्रबंधन, और निवेश के अवसरों की सुविधा सीधे भारत में पूंजी और नकदी प्रवाह के सुधार को प्रभावित करती है। प्रतिभूति बाजार पूंजी के एकत्रीकरण और आवंटन के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं, जो बदले में, व्यापार वृद्धि, नवाचार, और समग्र आर्थिक विकास का समर्थन करता है।
- विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों की पेशकश करके और निवेश और व्यापार के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाकर, प्रतिभूति बाजार भारत में वित्तीय प्रणाली की मजबूती और लचीलेपन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, जिससे सतत आर्थिक विकास के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण होता है।
विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institutions – DFI):-
विकास वित्तीय संस्थान (DFIs) विशेष रूप से कम आय वाले क्षेत्रों या देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित विशेष संस्थाएँ हैं। वे आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, गरीबी को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- पूंजी प्रावधान (Capital Provision):-
- 💰 DFIs विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि बुनियादी ढाँचे, कृषि, और लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) को पूंजी प्रदान करते हैं, जिन्हें पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कथित जोखिमों के कारण अनदेखा किया जा सकता है।
- जोखिम न्यूनीकरण (Risk Mitigation):-
- 🛡️ वे चुनौतीपूर्ण बाजारों या क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए जोखिम न्यूनीकरण उपकरण प्रदान करते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
- अतिरिक्त संसाधनों का लाभ उठाना (Leveraging Additional Resources):-
- 🔄 DFIs में निजी क्षेत्र के निवेशकों, अन्य वित्तीय संस्थानों और सरकारों के साथ सहयोग करके अपने निवेश के प्रभाव को कई गुना बढ़ाने की क्षमता होती है।
- तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण (Technical Assistance and Capacity Building):-
- 🎓 वे उद्यमों को बढ़ने में मदद करने और व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहायता, सलाहकार सेवाएँ, और क्षमता निर्माण प्रदान करते हैं।
- नीति संवाद और सुधार (Policy Dialogue and Reform):-
- 📜 व्यापार वातावरण और निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए नीति संवाद और सुधारों की वकालत करना।
- सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना (Promoting Sustainable Practices):-
- 🌿 DFIs पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी परियोजनाओं और सामाजिक रूप से जिम्मेदार उद्यमों में निवेश को प्राथमिकता देते हैं, वित्तीय उद्देश्यों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हैं।
- वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion):-
- 🌐 वे कम सेवा वाली आबादी तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने का प्रयास करते हैं, जिससे वित्तीय समावेशन और गरीबी कम होती है।
- वित्तीय बाजारों का नवाचार और विकास (Innovation and Development of Financial Markets):-
- 💡 DFIs अक्सर अभिनव वित्तपोषण मॉडल और उपकरणों का बीड़ा उठाते हैं, जिससे स्थानीय वित्तीय बाजारों के विकास और गहरा होने में योगदान मिलता है।
- दीर्घकालिक निवेश (Long-term Investment):-
- 🕰️ वे अक्सर दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करते हैं जो लंबी गर्भावधि वाली परियोजनाओं (long gestation periods) के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ।
- निगरानी और मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation):-
- 🔍 DFIs यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर निगरानी और मूल्यांकन पर जोर देते हैं कि निवेश वांछित विकासात्मक प्रभाव प्राप्त करें।
- ज्ञान साझा करना (Knowledge Sharing):-
- 🔄 वे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं, जिससे व्यापक विकास परिणामों में योगदान होता है।
- उदाहरण: भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
- 🔄 वे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं, जिससे व्यापक विकास परिणामों में योगदान होता है।
NABARD, भारत में एक DFI, DFIs की समग्र भूमिका का उदाहरण है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करता है, विभिन्न ग्रामीण बुनियादी ढाँचे परियोजनाओं का समर्थन करता है, और स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। अपनी कई पहलों के माध्यम से, NABARD दर्शाता है कि DFIs आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और वित्तीय समावेशन में कैसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, उभरते और पिछड़े क्षेत्रों में वित्तपोषण के अंतराल को पाटने और सतत विकास उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- भारत में, विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs) ने उन क्षेत्रों की वित्तपोषण जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक वाणिज्यिक बैंक कथित जोखिमों के कारण उद्यम नहीं कर सकते हैं। पिछले पाँच वर्षों में भारत में कुछ उल्लेखनीय DFIs और उनके प्रभाव में शामिल हैं:
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB):-
भारत का इन दो हाल ही में स्थापित वैश्विक DFIs में एक बड़ा हिस्सा है। वे अन्य सदस्य देशों के अलावा, भारत में बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं के लिए धन प्रदान करते हैं।
- नव स्थापित DFI:-
- भारत सरकार ने DFIs की प्रासंगिकता को मान्यता दी है और अगले तीन वर्षों में ₹5 ट्रिलियन के अपेक्षित पोर्टफोलियो के साथ एक नया DFI स्थापित करने की पहल की है। इस DFI का उद्देश्य दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के लिए है, जो भारत के सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- पारंपरिक DFIs:-
- इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (IFCI), इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ICICI), इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI), स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI), और इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक (IIBI) जैसी संस्थाएँ औद्योगिक और लघु-उद्योग क्षेत्रों के लिए संसाधनों को जुटाने और ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण रही हैं।
भारत में DFIs का पुनरुद्धार और स्थापना बुनियादी ढाँचे के विकास, औद्योगिक विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक दीर्घकालिक वित्तपोषण जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम का संकेत देती है। इन संस्थानों में निजी क्षेत्र के निवेशों को आकर्षित करने, पूंजी निर्माण को बढ़ाने, और देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता है। अपने संचालन के माध्यम से, DFIs वित्तपोषण के अंतराल को पाटने, स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने, और भारत के व्यापक विकासात्मक उद्देश्यों का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्थित हैं।
DFI – IFCI (इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया – IFCI):-
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (IFCI) भारत में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान है। यहाँ इसकी स्थापना, जनादेश, संचालन और प्रभाव के बारे में एक विस्तृत जानकारी दी गई है:
- स्थापना (Establishment):-
- IFCI को 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत एक वैधानिक निगम (Statutory Corporation) के रूप में स्थापित किया गया था, जिससे यह स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला विकास वित्त संस्थान बन गया।
- 1993 में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के निरसन के बाद, IFCI को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है।
- जनादेश (Mandate):-
- IFCI का मुख्य जनादेश औद्योगिक क्षेत्र को मध्यम से दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना है, जिसमें बुनियादी ढाँचा (हवाई अड्डे, सड़कें, दूरसंचार, बिजली), रियल एस्टेट, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और अन्य संबद्ध उद्योगों सहित परियोजनाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है।
- संचालन (Operations):-
- इन वर्षों में, IFCI ने औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय उत्पादों की एक विविध श्रृंखला की पेशकश करने के लिए विकसित किया है।
- यह दीर्घकालिक वित्त अंतर को भरने में सहायक रहा है, खासकर ऐसे समय में जब स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों के दौरान पूंजी बाजार का परिदृश्य काफी चुनौतीपूर्ण था।
- IFCI बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में भी सूचीबद्ध है, जो इसके परिचालन पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है।
- प्रभाव (Impact):-
- विभिन्न क्षेत्रों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके, IFCI ने उद्योगों के विकास और विकास की सुविधा प्रदान की है, जो बदले में, रोजगार सृजन, तकनीकी प्रगति और समग्र आर्थिक विकास में योगदान देता है।
- इसके प्रयास दीर्घकालिक वित्त की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण रहे हैं, जिससे देश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सहायक कंपनियाँ और सहयोगी (Subsidiaries and Associates):-
- IFCI की सात सहायक कंपनियाँ और एक सहयोगी है, जो औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं में इसके विस्तारित नेटवर्क और प्रभाव को दर्शाता है।
- IFCI की स्थापना और संचालन भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहे हैं, खासकर देश के विकास के प्रारंभिक चरणों के दौरान।
- अपनी वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के माध्यम से, IFCI भारत में औद्योगिक और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ICICI):-
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ICICI) ने भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र की सेवा की है। यहाँ ICICI का एक विस्तृत अवलोकन है, जिसमें इसकी स्थापना, उद्देश्य, संचालन और विकास शामिल है:
- स्थापना (Establishment):-
- ICICI को 5 जनवरी, 1955 को सर अरकोट रामासामी मुदलियार के पहले अध्यक्ष के रूप में एक सरकारी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। इसे विश्व बैंक, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त उद्यम के रूप में संरचित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग को परियोजना वित्तपोषण प्रदान करना था।
- ICICI बैंक, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, 1994 में वडोदरा में स्थापित की गई थी, और अक्टूबर 2001 में, ICICI का ICICI बैंक के साथ विलय हो गया, जिससे निजीकरण हुआ।
- उद्देश्य (Objectives):-
- ICICI के प्राथमिक उद्देश्यों में निजी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं को ऋण प्रदान करना, नए उद्योगों के संवर्धन को प्रोत्साहित करना, मौजूदा उद्योगों के विस्तार और आधुनिकीकरण में सहायता करना, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करना शामिल था।
- संचालन (Operations):-
- ICICI का उद्देश्य विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था, जिससे उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके। यह सहायता पैसे, शेयरों, डिबेंचर, या उपकरण की आपूर्ति के लिए गारंटी, और मशीनरी, उपकरण, या अन्य प्रारंभिक खर्चों को कवर करने के लिए रुपये के ऋण के संदर्भ में बढ़ाई गई थी।
- विकास (Evolution):-
- ICICI ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, एक सरकारी संस्था से एक निजी क्षेत्र की इकाई के रूप में विकसित हुआ। इस संक्रमण ने 1994 में ICICI बैंक को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया। समय के साथ, ICICI बैंक एक अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में विकसित हुआ, जो न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करता है।
- यह परिवर्तन भारत के वित्तीय क्षेत्र पर ICICI के स्थायी प्रभाव को रेखांकित करता है, पूंजी के एकत्रीकरण, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास की सुविधा में योगदान देता है।
ICICI की कहानी भारत में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। अपनी वित्तीय सेवाओं और रणनीतिक विकास के माध्यम से, ICICI, और बाद में ICICI बैंक, भारतीय वित्तीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान करना जारी रखे हुए हैं।
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI):-
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) की भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष रूप से माइक्रो, स्मॉल, और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के विकास को बढ़ावा देने में। यहाँ इसकी स्थापना, कार्यों और प्रभाव का एक विवरण दिया गया है:
- स्थापना और जनादेश (Establishment and Mandate):-
- SIDBI को 2 अप्रैल, 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य MSMEs को क्रेडिट के प्रवाह को सुविधाजनक और मजबूत करने के लिए, इस क्षेत्र में वित्तीय और विकासात्मक अंतरालों को संबोधित करते हुए, प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में सेवा करना है।
- संचालन और सेवाएँ (Operations and Services):-
- पुनर्वित्त और उधार (Refinancing and Lending): SIDBI बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सुविधाएँ प्रदान करता है, उद्योगों को टर्म लेंडिंग और कार्यशील पूंजी वित्त में संलग्न करता है। यह MSME क्षेत्र को धन की आपूर्ति को बढ़ाने और समर्थन करने में मदद करता है। SIDBI बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को टर्म लोन सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, यह सीधे MSMEs को भी उधार देता है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि छोटे उद्यमों के पास संचालन और विस्तार के लिए आवश्यक धन हो।
- सूक्ष्म वित्त विकास (Micro Finance Development): SIDBI सूक्ष्म ऋण के लिए SIDBI फाउंडेशन के माध्यम से सूक्ष्म वित्त संस्थानों को विकसित करने में सक्रिय रहा है। यह पहल सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI) मार्ग के माध्यम से सूक्ष्म वित्त का विस्तार करने में सहायता करती है, यह सुनिश्चित करती है कि छोटे उद्यमों के पास ऋण तक पहुंच हो।
- ग्रामीण उद्यम संवर्धन (Rural Enterprises Promotion): SIDBI के संवर्धन और विकास कार्यक्रम में ग्रामीण उद्यम संवर्धन और उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित है। यह पहल यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों के पास बढ़ने और अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए आवश्यक समर्थन हो।
- गैर-वित्तीय हस्तक्षेप और नवाचार (Non-Financial Interventions and Innovations):-
- SIDBI MSME क्षेत्र में गैर-वित्तीय हस्तक्षेपों में भी शामिल रहा है। उदाहरण के लिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRISIL और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी TransUnion CIBIL के सहयोग से, SIDBI ने “CriSidEx” और “MSME Pulse” पेश किया। CriSidEx सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए भारत का पहला भावना सूचकांक है, जो संभावित चुनौतियों और उत्पादन चक्रों में बदलाव को इंगित करके बाजार की दक्षता में सुधार करने में मदद करता है। ये हस्तक्षेप विदेशी व्यापार और MSME क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अन्य पहलुओं पर कार्रवाई योग्य संकेतक प्रदान करते हैं।
- समग्र प्रभाव (Holistic Impact):-
- SIDBI के काम का एक समग्र प्रभाव है क्योंकि यह न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करता है बल्कि क्षेत्र के विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देने, ऋण तक पहुंच में सुधार, और बेहतर बाजार दक्षता के लिए नवाचारों को पेश करने में भी संलग्न है। इन प्रयासों के माध्यम से, SIDBI उत्पादन, रोजगार, और निर्यात के मामले में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, भारत में MSMEs के विकास और विकास में सहायता करने के अपने जनादेश को पूरा करता है।
इन बहु-आयामी प्रयासों के माध्यम से, SIDBI MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है।
इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IIBI):-
इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IIBI) ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व के तहत एक विकास वित्त संस्थान के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ इसके संचालन, परिवर्तन, और भारतीय उद्योगों पर प्रभाव का एक विवरण दिया गया है:
- स्थापना और संचालन (Establishment and Operations):-
- IIBI को 1971 में, शुरुआत में इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (IRCI) के रूप में बीमार औद्योगिक कंपनियों के पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया था।
- यह बाद में 1985 में इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया (IRBI) में बदल गया, और अंततः, मार्च 1997 में, इसे एक पूर्ण-विकसित विकास वित्तीय संस्थान के रूप में सेवा करने के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (IIBI) के रूप में पुनर्गठित किया गया।
- बैंक ने विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएँ प्रदान कीं, जिसमें परियोजना वित्त के लिए टर्म लोन सहायता, अल्पकालिक गैर-परियोजना परिसंपत्ति-समर्थित वित्तपोषण, कंपनियों को कार्यशील पूंजी/अन्य अल्पकालिक ऋण, इक्विटी सदस्यता, परिसंपत्ति ऋण, उपकरण वित्त, और पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार उपकरणों में निवेश शामिल थे।
- उद्देश्य और परिवर्तन (Objective and Transformation):-
- IIBI का प्राथमिक उद्देश्य भारत में बीमार औद्योगिक कंपनियों का पुनर्वास करना था। इसका उद्देश्य वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनियों का पुनर्वास करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारतीय उद्योग को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना था।
- समापन और प्रभाव (Closure and Impact):-
- IIBI का एक पर्याप्त ग्राहक आधार था, जिसमें वीडियोकॉन, डॉ. मोरेपेन, परफेक्ट थ्रेड्स, क्लच ऑटो लिमिटेड, JSW इस्पात, और LML मोटर्स जैसी प्रमुख फर्में शामिल थीं।
- हालांकि, 2000 के दशक के मध्य में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक विलय पर विचार किया गया था, जिसे IIBI ने मना कर दिया था। इसके बाद, भारत सरकार ने 2006-2007 में बैंक को बंद करने का फैसला किया। 2012 के बजट में आधिकारिक समापन की घोषणा की गई थी, जो इसके संचालन के अंत को दर्शाता है।
- विरासत (Legacy):-
- IIBI के बंद होने से संकटग्रस्त कंपनियों को पुनर्वास वित्त प्रदान करने में एक अंतर रह गया, जो इसका प्राथमिक ध्यान था। इसके ग्राहकों और जिन क्षेत्रों में इसने सेवा की, उन्हें वित्तीय संकट से उबरने के लिए वैकल्पिक वित्तीय संस्थानों या तंत्रों की तलाश करनी पड़ी, इस प्रकार एक ऐसे विशेष संस्थान द्वारा छोड़े गए महत्व और शून्यता को उजागर किया गया।
- IIBI की यात्रा भारत में वित्तीय संस्थानों के विकास को दर्शाती है जो औद्योगिक क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, और इसके बंद होने ने औद्योगिक संकट को संबोधित करने और क्षेत्र के भीतर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित वित्तीय तंत्रों के महत्व को रेखांकित किया।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI):-
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI) को 1964 में संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में, जिसका प्राथमिक उद्देश्य नवजात भारतीय उद्योग के विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएँ प्रदान करना था। प्रारंभ में, इसने 1976 तक उद्योगों के विकास और विकास में लगे संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में काम किया, जब इसका स्वामित्व केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया, जिससे यह भारत में उद्योग के वित्तपोषण, संवर्धन और विकास में लगे संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान बन गया।
IDBI के उद्देश्यों में वित्तीय सेवाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल था, जिसमें शामिल हैं:-
- ICICI, LIC, आदि जैसे वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना।
- अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन एकत्र करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रमुख उद्योगों की योजना बनाना और बढ़ावा देना।
IDBI ने मध्यम और दीर्घकालिक वित्त की आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर को पाटने के लिए औद्योगिक इकाइयों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की। IDBI अधिनियम को 1994 में संशोधित किया गया था, जिससे 49 प्रतिशत तक सार्वजनिक स्वामित्व की अनुमति दी गई। 1995 में, इसने अपने पहले आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के माध्यम से 20 अरब रुपये से अधिक जुटाए।
- 2004 में, IDBI एक विकास वित्तीय संस्थान (DFI) से एक पूर्ण-विकसित वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित हो गया, जिसने अपनी सेवाओं के दायरे को व्यापक बनाया लेकिन अपने विकासात्मक एजेंडे को बनाए रखा, जिसे अब ‘विकास बैंकिंग’ कहा जाता है। इस परिवर्तन का उद्देश्य थोक और खुदरा बैंकिंग सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करना था, साथ ही विकास वित्तपोषण के अपने पहले के जनादेश को जारी रखना था। IDBI बैंक लिमिटेड, जिसे हम आज जानते हैं, ने अपने पूर्ववर्ती संस्था से इस समृद्ध विरासत को विरासत में मिला है, और इसके संचालन में अब निवेश, वाणिज्यिक, खुदरा बैंकिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन, पेंशन, गिरवी, और क्रेडिट कार्ड सहित अन्य बैंकिंग सेवाओं की एक श्रृंखला शामिल है।
- इन वर्षों में IDBI का विकास भारतीय वित्तीय परिदृश्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। यह स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), और नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) जैसी कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना में सहायक था। IDBI बैंक की यात्रा भारत के औद्योगिक और वित्तीय विकास के व्यापक आख्यान को दर्शाती है, जो भारत में आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs) की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है।
अपने वाणिज्यिक प्रभाग के साथ विलय करके और एक पूर्ण-विकसित वाणिज्यिक बैंक बनकर, IDBI ने देश के बदलते वित्तीय परिदृश्य के अनुकूल होते हुए अपने मूल जनादेश को पूरा करने का प्रयास किया है।