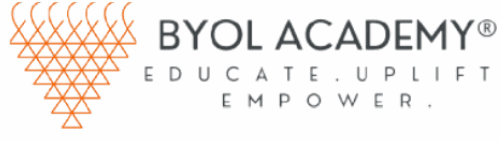b. भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ: संवैधानिक विकास का प्रतिबिंब
छात्रों के लिए नोट्स
लेख का संदर्भ:-
26 नवम्बर 2024 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया गया। इसे ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाया गया, जिसका केंद्रीय नारा था— “हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान”। इसका नेतृत्व संवैधानिक पदाधिकारियों ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष (संविधान सदन) से किया।
UPSC पेपर से संबंध:-
- GS पेपर II: भारतीय संविधान, शासन-प्रशासन, संवैधानिक मूल्य
- GS पेपर IV: लोक प्रशासन में नैतिकता, संस्थागत अखंडता
- निबंध पत्र: संवैधानिक नैतिकता और राष्ट्र-निर्माण
लेख के आयाम:-
- संवैधानिक प्रतीकवाद और संस्थागत अखंडता
- संवैधानिक पदाधिकारियों की नैतिकता
- संवैधानिक मूल्यों के प्रति जन-भागीदारी और जागरूकता
- संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ के रूप में
- संवैधानिक राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक वैधता
चर्चा में क्यों ?:-
भारत ने 26 नवम्बर 2024 को एक ऐतिहासिक क्षण मनाया—संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष (1949–2024)। इस वर्ष भर चलने वाले आयोजन का उद्देश्य नागरिकों की संवैधानिक मूल्यों में गहरी भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके चार स्तंभ हैं:
- 1. संविधान की प्रस्तावना
- 2. अपना संविधान जानो
- 3. संविधान निर्माण
- 4. संविधान की महिमा का उत्सव
इस समारोह का शुभारंभ संसद भवन के केंद्रीय कक्ष (संविधान सदन) में हुआ, जहाँ भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित थे। इस अवसर पर:
- स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए गए
- संस्कृत और मैथिली में भारतीय संविधान प्रकाशित हुआ
देशभर के नागरिकों ने एक साथ प्रस्तावना का वाचन किया, जो संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति सामूहिक नैतिक निष्ठा का प्रतीक था।
आयोजन की प्रमुख विशेषताएँ और नैतिक आयाम:-
1. नैतिक नेतृत्व और संस्थागत उत्तरदायित्व:-
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि संस्थागत नैतिकता केवल कानूनी आचरण का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह नैतिक दिशा-निर्देश है। सार्वजनिक संस्थानों को राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप कार्य करना चाहिए।
2. प्रतीकात्मक भागीदारी से राष्ट्रीय एकता:-
- सामूहिक रूप से प्रस्तावना का वाचन करना संवैधानिक राष्ट्रवाद का एक सशक्त प्रतीक था, जिसने भाषाई, क्षेत्रीय और सामाजिक सीमाओं से परे एकता का संदेश दिया।
3. लोकतांत्रिक विरासत और संवैधानिक लचीलापन:-
- एक लघु चलचित्र में संविधान की यात्रा—निर्माण से लेकर संशोधनों तक—को दिखाया गया, जिससे यह विचार सुदृढ़ हुआ कि संविधान स्थिर नहीं है बल्कि जीवंत है, जो समयानुकूल न्याय और समावेशी शासन की चुनौतियों के अनुसार स्वयं को ढालता है।
4. अधिकारों और कर्तव्यों के सामंजस्य का आह्वान:-
- उपराष्ट्रपति ने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन पर जोर दिया और कहा कि लोकतंत्र में नागरिकता का अर्थ केवल अधिकारों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों से भी है, विशेषकर वैचारिक ध्रुवीकरण के दौर में।
विश्लेषण:-
1. संवैधानिक प्रतीकवाद क्या है?
संवैधानिक प्रतीकवाद उन संस्थागत प्रथाओं, अनुष्ठानों, प्रतीकों और भाषा को संदर्भित करता है, जो संविधान की भावना और मूल्यों को दृष्टिगत और औपचारिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। इसमें गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस समारोह, संविधान दिवस (संविधान दिवस) का आयोजन, प्रस्तावना वाचन, न्यायपालिका और संसद में संविधान पर शपथ लेना आदि शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य मात्र संविधान का स्मरण करना नहीं, बल्कि इसके मूल्यों—स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व—को सार्वजनिक चेतना में आत्मसात करना है। जब नागरिक एक साथ प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो यह विविधता में एकता और लोकतांत्रिक परियोजना के सामूहिक स्वामित्व का प्रतीक बन जाता है।
- संवैधानिक प्रतीकवाद नागरिक शिक्षा को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे संस्थानों के प्रति आदर और लोकतांत्रिक भावनात्मक लगाव बढ़ता है। राष्ट्रीय ध्वज, अशोक चक्र, या “सत्यमेव जयते” जैसे प्रतीक केवल चिह्न नहीं हैं, बल्कि भारत की संवैधानिक विचारधारा का आधार हैं।
- संक्षेप में, संवैधानिक प्रतीकवाद नैतिकता और भावना के संगम पर कार्य करता है, जो नागरिकों को समय-समय पर संविधान की याद दिलाता है, उन्हें शिक्षित करता है और एकजुट रखता है।
2. संविधान को “जीवंत दस्तावेज़” क्यों कहा जाता है?
भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज़ कहा जाता है क्योंकि यह गतिशील, उत्तरदायी और सतत विकसित होता रहता है। यह तीन माध्यमों से संभव हुआ है:
- न्यायिक व्याख्या:–
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में मूल संरचना सिद्धांत सामने आया, जिसमें संसद को संविधान संशोधन का अधिकार तो मिला, लेकिन मूल सिद्धांतों में बदलाव करने पर रोक लगाई गई।
- बाद के निर्णयों में गोपनीयता का अधिकार (पुट्टस्वामी मामला, 2017) और संवैधानिक नैतिकता जैसे नए आयाम जुड़े।
- संशोधन:-
- संविधान में 100 से अधिक संशोधन किए गए हैं, जो बदलती सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। जैसे 73वाँ और 74वाँ संशोधन—पंचायती राज और नगरीय निकायों के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना।
- जन-संलग्नता:-
- नागरिक, सिविल सोसाइटी, मीडिया और अकादमिक जगत सक्रिय रूप से संविधान के साथ जुड़ते रहे हैं। अन्ना हज़ारे आंदोलन, सूचना का अधिकार (RTI) आंदोलन और लैंगिक न्याय अभियानों जैसे उदाहरण इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
इस प्रकार संविधान केवल कानूनी पाठ नहीं, बल्कि एक नैतिक मार्गदर्शक है, जो समय के साथ व्यापक होता गया है और भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक है।
3. संविधान दिवस (संविधान दिवस) मनाने का नैतिक महत्व:-
संविधान दिवस केवल औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि एक नैतिक कृत्य है—स्मरण, पुनर्पुष्टि और पुनर्निर्देशन का।
- यह सामूहिक नैतिक लेखा-जोखा है, जहाँ नागरिक और संस्थाएँ यह मूल्यांकन करते हैं कि न्याय, समानता, गरिमा और बंधुत्व के संवैधानिक आदर्शों का पालन कितना हो रहा है।
- यह सार्वजनिक पदाधिकारियों को उनकी नैतिक जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। जब राजनीति में जनप्रियता और ध्रुवीकरण बढ़ता है, तब संविधान दिवस शासन को संवैधानिक नैतिकता के ढांचे में पुनः स्थापित करने का अवसर बनता है।
- यह एक शैक्षिक अवसर है, विशेषकर युवाओं के लिए—जिससे उनमें अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित हो।
इस प्रकार संविधान दिवस संविधान को केवल एक शासन दस्तावेज़ नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण के साझा नैतिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत करता है।
निष्कर्ष:-
भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ केवल स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मचिंतन का भी समय है। भारत यदि एक विकसित लोकतंत्र बनना चाहता है तो संवैधानिक मूल्यों की पुनर्पुष्टि को इन रूपों में मूर्त रूप देना होगा:
- सार्वजनिक पदाधिकारियों का नैतिक आचरण
- सक्रिय नागरिक भागीदारी
- अधिकारों की सुदृढ़ रक्षा के साथ कर्तव्यों की जवाबदेही
- सभी भाषाओं और क्षेत्रों में संवैधानिक साक्षरता का प्रसार
1949 के “हम भारत के लोग” से लेकर 2024 के “विश्व-बंधु” तक की यात्रा तभी सार्थक होगी जब संस्थागत अखंडता और संवैधानिक प्रतीकवाद पर आधारित नैतिक शासन-व्यवस्था कायम की जाए।