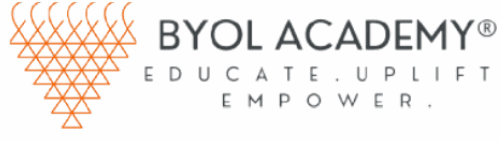e. समान नागरिक संहिता: संवैधानिक दृष्टि बनाम सामाजिक वास्तविकताएँ
छात्रों के लिए नोट्स
लेख का संदर्भ:-
फरवरी 2024 में उत्तराखंड विधान सभा द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद इसके संवैधानिक वैधता, सामाजिक स्वीकार्यता और समय-चयन को लेकर पूरे देश में बहस फिर से तेज हो गई है, खासकर लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व। इसी समय, निर्वाचन सुधारों—विशेष रूप से राजनीति के अपराधीकरण, धनबल के दुरुपयोग और एक साथ चुनाव कराने—को लेकर चर्चाएँ भी जोर पकड़ रही हैं। ये सभी मुद्दे भारत के लोकतांत्रिक परिपक्वता के केंद्र में हैं।
UPSC पाठ्यक्रम से संबंध:-
- सामान्य अध्ययन पत्र–II: राजनीति – भारतीय संविधान; विशेषताएँ और संशोधन; निर्वाचन सुधार; न्यायपालिका; संघवाद
- सामान्य अध्ययन पत्र–II: सुशासन – सिविल सेवाओं की भूमिका, दबाव समूह, एवं चुनाव आयोग
- सामान्य अध्ययन पत्र–I: समाज – सामाजिक सशक्तिकरण; धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद
- सामान्य अध्ययन पत्र–IV: नैतिकता – संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक न्याय
लेख के आयाम:-
- 1. हाल के निर्वाचन सुधार और लंबित चुनौतियाँ
- 2. UCC और उसका संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 44 बनाम अनुच्छेद 25)
- 3. सामाजिक वास्तविकताएँ और अल्पसंख्यक समुदाय की चिंताएँ
- 4. संघवाद और केंद्र–राज्य संबंध
- 5. न्यायपालिका और चुनाव आयोग की भूमिका
- 6. राजनीतिक इच्छाशक्ति बनाम लोकतांत्रिक सहमति
वर्तमान संदर्भ:-
2024 की शुरुआत में, उत्तराखंड विधानसभा ने देश का पहला राज्य-स्तरीय समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित किया, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित एक समान कानूनी ढाँचा प्रस्तावित किया गया है, जो सभी नागरिकों पर, उनके धर्म की परवाह किए बिना, लागू होगा। इसी बीच, भारत के विधि आयोग (22वाँ) ने राष्ट्रीय स्तर पर UCC लागू करने के लिए जनमत आमंत्रित किया है। साथ ही, भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता के कठोर प्रावधान और एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections) की व्यवहार्यता पर चर्चा की है, जबकि चुनावी मुफ्तखोरी और मतदाता प्रलोभन को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं। ये दोनों मुद्दे भारत के संवैधानिक आदर्शों को राजनीतिक व्यवहारिकता और सामाजिक बहुलवाद के साथ सामंजस्य बिठाने की चुनौती प्रस्तुत करते हैं।
विशेषताएँ:-
1. UCC – संवैधानिक निर्देश बनाम सामाजिक बहुलवाद:-
- संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अंतर्गत अनुच्छेद 44 राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का आह्वान करता है।
- हालाँकि, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए।
- उत्तराखंड विधेयक में अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है, लेकिन इसमें लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, पुत्र-पुत्री को समान संपत्ति अधिकार दिए गए हैं और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है।
2. सामाजिक प्रतिक्रियाएँ और अल्पसंख्यक चिंताएँ:-
- मुस्लिम, ईसाई और आदिवासी समुदायों ने सांस्कृतिक क्षरण और धार्मिक पहचान खोने की चिंता व्यक्त की है।
- आलोचकों का कहना है कि पर्याप्त जनपरामर्श नहीं हुआ और विचार-विमर्श के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
- समर्थकों का तर्क है कि यह लैंगिक न्याय सुनिश्चित करता है और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को मजबूत बनाता है।
3. न्यायिक दृष्टिकोण और पूर्व उदाहरण:-
- शाह बानो मामला (1985) में, सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक समानता बनाए रखने के लिए UCC लागू करने का आग्रह किया।
- सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) मामले में, न्यायालय ने व्यक्तिगत लाभ के लिए धार्मिक कानूनों के दुरुपयोग की आलोचना की और UCC की आवश्यकता पर बल दिया।
- हालाँकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि UCC का क्रियान्वयन क्रमिक और सर्वसम्मति से होना चाहिए, ताकि सामाजिक अशांति से बचा जा सके।
4. चुनावी सुधार – मुख्य बातें और कमियाँ:-
- राजनीति का आपराधिकरण जारी है, 2024 की ADR रिपोर्ट के अनुसार 40% सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं।
- धन बल और निर्वाचन बांड को सुप्रीम कोर्ट ने “एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ” (2024) मामले में असंवैधानिक घोषित किया है।
- एक साथ चुनाव (वन नेशन, वन इलेक्शन) के प्रस्ताव की जाँच पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने की है, लेकिन संघीय ढाँचे और लॉजिस्टिक्स को लेकर चिंताएँ अब भी अनसुलझी हैं।
5. निर्वाचन आयोग और नागरिक समाज की भूमिका:-
- निर्वाचन आयोग ने दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए चुनावों के राज्य-निधिकरण (State Funding) की सिफारिश की है।
- नागरिक समाज संगठन राजनीतिक दलों की फंडिंग में आरटीआई लागू करने, उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता लाने और चुनाव प्रचार के दौरान घृणा भाषण पर रोक लगाने की माँग करते रहे हैं।
व्याख्या:-
1. क्या समान नागरिक संहिता (UCC) असंवैधानिक है?
नहीं, UCC असंवैधानिक नहीं है। इसका संवैधानिक आधार नीति-निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 44 से मिलता है, जो राज्य को पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। हालाँकि, इसका क्रियान्वयन इस प्रकार होना चाहिए कि यह अनुच्छेद 25 से 28 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे, जो धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार सुनिश्चित करते हैं।
- संविधान सभा की बहसों में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि UCC प्रारंभिक चरण में स्वैच्छिक होनी चाहिए और समाज के तैयार होने पर धीरे-धीरे लागू की जानी चाहिए। अतः, संविधान विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेना और तलाक जैसे नागरिक मामलों में कानूनी एकरूपता का दृष्टिकोण रखता है, लेकिन धार्मिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का संरक्षण भी आवश्यक है।
- सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो (1985) और सरला मुद्गल (1995) मामलों में संवैधानिक समानता बनाए रखने के लिए UCC की वकालत की, परंतु सामाजिक जटिलताओं को भी स्वीकार किया। इसलिए, UCC अपने आप में असंवैधानिक नहीं है, लेकिन इसका क्रियान्वयन धर्मनिरपेक्ष कानून और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखते हुए, समावेशी, क्रमिक और सर्वसम्मति से होना चाहिए।
2. क्या UCC लैंगिक न्याय सुनिश्चित करता है?
हाँ, UCC विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद लैंगिक असमानताओं को समाप्त करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए:
- मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पहले तीन तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाओं की अनुमति देता था, जो महिलाओं के साथ असमान व्यवहार करता था।
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (2005 संशोधन से पहले) बेटियों को समान उत्तराधिकार अधिकार नहीं देता था।
- ईसाई तलाक कानून ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के लिए तलाक के कठोर आधार तय करते थे।
समान नागरिक संहिता नागरिक मामलों में सभी धर्मों और लिंगों के लिए एक समान कानूनी ढाँचा प्रदान कर समान अधिकार सुनिश्चित करने का वादा करती है। इसका उद्देश्य अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध) को लागू करना है।
हालाँकि, UCC को वास्तव में लैंगिक न्याय का साधन बनाने के लिए यह जरूरी है कि यह बहुसंख्यकवादी थोपने का औजार न बन जाए। इसके प्रारूपण और क्रियान्वयन में अल्पसंख्यक, आदिवासी और महिला समूहों की राय शामिल होनी चाहिए, ताकि इसे कानूनी समानता का प्रकल्प माना जाए, न कि सांस्कृतिक एकरूपता का। यदि ऐसी संवेदनशीलता नहीं बरती गई तो यह अलगाव और विरोध को जन्म दे सकती है, जिससे इसका उद्देश्य विफल हो जाएगा।
3. चुनावी सुधार क्यों जरूरी हैं?
भारतीय लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनावी सुधार अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि यह कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे:
- राजनीति का आपराधिकरण: ADR रिपोर्ट (2024) के अनुसार 40% से अधिक सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित हैं, जिससे जन-विश्वास कमजोर होता है और क़ानून के शासन पर खतरा बढ़ता है।
- चुनावों में धनबल: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ADR बनाम भारत संघ (2024) मामले में निर्वाचन बांड योजना को असंवैधानिक ठहराया, क्योंकि यह राजनीतिक वित्त पोषण में अपारदर्शिता और कॉर्पोरेट प्रभाव बढ़ाती थी।
- वोट खरीदना और लोकलुभावनवाद: मुफ्तखोरी की राजनीति और पहचान-आधारित लामबंदी ने मुद्दा-आधारित लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर किया है।
- जन-विश्वास में गिरावट: कम मतदान प्रतिशत और राजनीतिक निंदकता चुनावी परिणामों की वैधता पर संकट पैदा कर रही है।
इसलिए, अपराधी नेताओं की अयोग्यता पर शीघ्र निर्णय के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें, चुनावों का राज्य-निधिकरण, आंतरिक पार्टी लोकतंत्र और राजनीतिक वित्त में अधिक पारदर्शिता जैसे सुधार आवश्यक हैं। ये कदम स्वच्छ राजनीति, जन-जवाबदेही और संविधानसम्मत नैतिक शासन स्थापित करने में मदद करेंगे।
4. एक साथ चुनाव में क्या चुनौतियाँ हैं?
वन नेशन, वन इलेक्शन का उद्देश्य चुनावी थकान, नीतिगत ठहराव और सार्वजनिक व्यय को कम करना है। लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई संवैधानिक, संघीय और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ हैं, जैसे:
- असमान संघवाद: विभिन्न राज्यों के चुनाव चक्र अलग-अलग हैं, जो समयपूर्व विघटन, न्यायिक हस्तक्षेप या स्थानीय जनादेश के कारण बदल सकते हैं।
- संवैधानिक कठोरता: कार्यकाल का समन्वय करने के लिए अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 में संशोधन करने होंगे, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।
- प्रशासनिक व्यवहार्यता: लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए भारी मानव एवं वित्तीय संसाधन, सुरक्षा बल और चुनावी कर्मियों की आवश्यकता होगी।
- राज्य-विशिष्ट मुद्दों का ह्रास: एक साथ चुनाव से राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, जिससे स्थानीय शासन संबंधी मुद्दे हाशिए पर चले जाएँगे और सहयोगात्मक संघवाद की भावना कमजोर हो सकती है।
हालाँकि, उच्च-स्तरीय समिति (2024) ने चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने की सिफारिश की है, लेकिन किसी भी कदम को संवैधानिक रूप से ठोस, लॉजिस्टिक रूप से सक्षम और लोकतांत्रिक रूप से समावेशी होना चाहिए।
निष्कर्ष:-
समान नागरिक संहिता (UCC) और निर्वाचन सुधारों पर समानांतर रूप से बढ़ती बहस भारत के लोकतांत्रिक विकास में एक अहम मोड़ का संकेत है। यद्यपि दोनों ही समानता और एकरूपता के संवैधानिक आदर्शों में निहित हैं, परंतु इनके क्रियान्वयन में सतर्क व्यवहारिकता, समावेशी संवाद और पारदर्शी तंत्र आवश्यक हैं।
- संवैधानिक दृष्टि और सामाजिक यथार्थ के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदम अनिवार्य हैं:
- अल्पसंख्यक और आदिवासी समूहों सहित सभी हितधारकों के साथ UCC पर राष्ट्रव्यापी जनपरामर्श को बढ़ावा देना।
- मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSPs) में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए UCC कानूनों की न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करना।
- समयबद्ध निर्वाचन सुधार लागू करना, जिसमें प्रत्याशी अयोग्यता, राजनीतिक दलों की पारदर्शिता और डिजिटल चुनाव निगरानी शामिल हो।
- UCC या निर्वाचन सुधारों को चुनावी मौसम में राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने से बचना; इन्हें राष्ट्रीय संकल्प के रूप में बनाए रखना।
- चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और प्रवर्तन शक्तियों को सुदृढ़ करना।
सच्चे निर्वाचन और कानूनी सुधार शीर्ष-से-नीचे थोपे गए आदेश नहीं होने चाहिए, बल्कि भारत की बहुलतावादी परंपरा और संवैधानिक नैतिकता में निहित सहमति-आधारित लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ होने चाहिए।