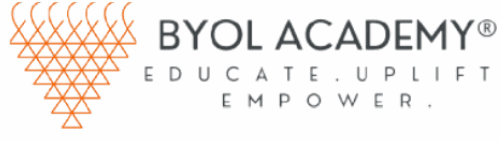ख. गृह-मतदान तंत्र: समावेशन बनाम अखंडता
छात्रों के लिए नोट्स:-
संदर्भ:-
अप्रैल 2024 में, भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने आगामी राज्य चुनावों के लिए चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांगजन (PwDs) के लिए गृह-मतदान तंत्र का पायलट चरण शुरू करने की घोषणा की। इसे समावेशन के लिहाज़ से लोकतांत्रिक प्रगति के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन नागरिक समाज और राजनीतिक हितधारकों द्वारा मतदाता की गोपनीयता, हेरफेर और चुनावी अखंडता को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं।
UPSC प्रश्न पत्र में सम्बद्ध विषय
सामान्य अध्ययन पत्र-II: राजनीति – निर्वाचन सुधार, निर्वाचन आयोग की भूमिका ।
सामान्य अध्ययन पत्र-II: शासन – समावेशी शासन, संवेदनशील वर्ग ।
सामान्य अध्ययन पत्र-II: अधिकार संबंधी मुद्दे – दिव्यांग एवं बुजुर्ग मताधिकार ।
सामान्य अध्ययन पत्र-IV: नैतिकता – लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अखंडता ।
लेख के आयाम:-
- गृह-मतदान का कानूनी एवं संस्थागत आधार।
- कार्यान्वयन तंत्र और उसकी सुरक्षा व्यवस्था।
- हाशिये पर स्थित मतदाताओं का समावेशन बनाम हेरफेर का जोखिम।
- चुनावी अखंडता और मतदान प्रक्रिया में विश्वास।
- अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं और भारतीय संदर्भ।
चर्चा में क्यों ?:-
अप्रैल 2024 में भारत के निर्वाचन आयोग ने, विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श और विधि एवं न्याय पर स्थायी समिति (2024) की सिफ़ारिशों के आधार पर, शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गृह-मतदान परियोजना के पायलट चरण की घोषणा की।
- इस योजना का उद्देश्य 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं और 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों को, चुनाव अधिकारियों की देखरेख में, डाक मतपत्र और वीडियो सत्यापन के माध्यम से घर से सुरक्षित मतदान की सुविधा देना है।
- यह पहल मतदाता समावेशन और निर्वाचन सुगमता की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही मतदान की गोपनीयता में संभावित कमी, तथा विशेष रूप से सामाजिक रूप से आश्रित वातावरण में मतदाता पर दबाव पड़ने के खतरे को लेकर गंभीर बहस शुरू हो गई है।
सुधार की विशेषताएँ:-
1. कानूनी आधार और निर्वाचन समावेशन:-
- 1. गृह-मतदान प्रक्रिया निर्वाचन आचरण नियम, 1961 के नियम 27A (2019 में संशोधित) के अंतर्गत अनुमत है।
- 2. यह 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को, अग्रिम आवेदन करने पर, डाक मतपत्र की सुविधा देता है।
- 3. एक समर्पित टीम मतदाता के घर जाकर मोबाइल कैमरा और मतपत्र के साथ सुरक्षित और सत्यापन योग्य मतदान सुनिश्चित करती है।
2. कार्यान्वयन तंत्र:-
- 1. मतदाता की पहचान फॉर्म 12D के माध्यम से सत्यापित की जाती है।
- 2. दो अधिकारियों की टीम और एक वीडियोग्राफर मतदान की देखरेख करते हैं।
- 3. पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की जाती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है, लेकिन इससे मतदाता की गोपनीयता और स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं।
3. लाभ: निर्वाचन तक पहुँच का विस्तार:-
- 1. अचल या संवेदनशील मतदाताओं को स्वास्थ्य या गरिमा के साथ समझौता किए बिना भाग लेने में सक्षम बनाता है।
- 2. मतदाता उपस्थिति बढ़ाता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) के संवैधानिक आदेश के अनुरूप है।
- 3. भारत की संयुक्त राष्ट्र विकलांग अधिकार संधि (UNCRPD) के प्रति प्रतिबद्धता पूरी करता है।
4. चिंताएँ: गोपनीयता और अखंडता पर खतरा:-
- 1. परिवार के सदस्यों या स्थानीय प्रभावशाली लोगों द्वारा मतदान के समय मतदाता पर प्रभाव डाला जा सकता है।
- 2. मतदान के दौरान सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति चुनाव की “स्वतंत्र और निष्पक्ष” प्रकृति को कमजोर कर सकती है।
- 3. राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा, खासकर करीबी मुकाबलों या ध्रुवीकृत क्षेत्रों में।
व्याख्या:-
1. गृह-मतदान विवादास्पद क्यों है?
गृह-मतदान, भले ही निर्वाचन आधार को व्यापक बनाने का एक सराहनीय प्रयास हो, लेकिन इसमें मतदान की गोपनीयता, स्वतन्त्रता और अनुचित प्रभाव के गंभीर खतरे निहित हैं।
- मतपत्र की गोपनीयता पर खतरा:-
- गोपनीयता लोकतांत्रिक चुनावों का आधार है, जिसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 में संरक्षित किया गया है। नियंत्रित मतदान केंद्र में यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी—न परिवार, न राजनीतिक एजेंट, न ही मतदान कर्मी—मतदाता की पसंद न जान सके। यह स्थिति घर के माहौल में दोहराना कठिन है, खासकर संयुक्त परिवारों या आश्रित सामाजिक परिस्थितियों में।
- दबाव या प्रभाव का जोखिम:-
- बुजुर्ग या दिव्यांग मतदाता पर परिवार या देखभाल करने वालों का सूक्ष्म या प्रत्यक्ष दबाव पड़ सकता है। पितृसत्तात्मक या राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत परिवारों में स्वतंत्र निर्णय लेना कठिन हो सकता है।
- राज्य की निगरानी की धारणा:-
- वीडियो रिकॉर्डिंग और सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति, भले ही सुरक्षा उपाय हों, परोक्ष रूप से निगरानी का माहौल बना सकती है। इससे विशेषकर हाशिये के समुदायों के मतदाता भयभीत होकर मतदान से वंचित हो सकते हैं या दबाव में मतदान कर सकते हैं।
- प्रशासनिक विवेक और हेरफेर:-
- पात्र गृह-मतदाताओं की सूची के चयन और सत्यापन को लेकर चिंताएँ हैं। कड़े सुरक्षा उपायों के बिना यह प्रक्रिया वोट बैंक साधने या करीबी चुनाव परिणामों में हेरफेर के लिए इस्तेमाल हो सकती है।
इसलिए, जब तक मजबूत संस्थागत नियंत्रण न हों, गृह-मतदान “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव” के सिद्धांतों के लिए चुनौती बन सकता है।
2. संविधान मतदान अधिकार के बारे में क्या कहता है?
- मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि वैधानिक अधिकार है, लेकिन इसका प्रयोग संवैधानिक सिद्धांतों के अंतर्गत होता है।
- अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने का प्रावधान करता है—अर्थात् 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर नागरिक को मतदान का अधिकार है।
- जबकि संविधान सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करता है, चुनावों का संचालन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 व 1951 और निर्वाचन आचरण नियम, 1961 द्वारा नियंत्रित होता है।
- सुलभता और अखंडता के बीच संतुलन बनाए रखना राज्य का दायित्व है। गृह-मतदान जैसी पहल में समावेशन को चुनावी शुचिता से समझौता नहीं करने देना चाहिए।
- PUCL बनाम भारत संघ (2003) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों की जानकारी का अधिकार, मतदाता के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है, जिससे मतदान अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकारों से जुड़ता है। इसी तरह, मतदान की गोपनीयता स्वतंत्र चुनावी अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य है।
3. अंतरराष्ट्रीय अनुभव:-
- ऑस्ट्रेलिया:–
- अचल मतदाताओं के लिए मोबाइल मतदान केंद्र और डाक मतदान की सुविधा; डाक मतपत्र सख्त चेन-ऑफ़-कस्टडी प्रोटोकॉल के तहत गिने जाते हैं।
- जर्मनी:-
- 1. बीमारी या दिव्यांगता के लिए चिकित्सीय प्रमाण पत्र आवश्यक।
- 2. यादृच्छिक ऑडिट और निजी माहौल में मतदान की अनिवार्यता।
- 3. जर्मन संघीय संवैधानिक न्यायालय ने कहा कि मतदान की सुगमता, गोपनीयता और प्रामाणिकता से ऊपर नहीं हो सकती।
- कनाडा:-
- विशेष मतपत्र किट, सीलबंद लिफाफे और सत्यापन कोड के साथ; संवेदनशील क्षेत्रों में चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं।
ये उदाहरण बताते हैं कि सुगमता और अखंडता को संतुलित करने के लिए बहु-स्तरीय सुरक्षा आवश्यक है।
4. चिंताओं का समाधान कैसे हो?
- स्वतंत्र पर्यवेक्षक की तैनाती:-
- सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी या स्वतंत्र निगरानी निकाय के सदस्य प्रक्रिया की देखरेख करें।
- छेड़छाड़-रोधी वीडियो निगरानी:-
- टाइमस्टैम्प और एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित फुटेज, तृतीय-पक्ष सत्यापन से ऑडिट।
- सख्त पात्रता जाँच:-
- 1. चिकित्सीय प्रमाणपत्र या सामाजिक कार्यकर्ता की सिफारिश के आधार पर ही पात्रता।
- 2. स्वतंत्र गृह-मतदान पैनल को सूची सत्यापित करने का अधिकार।
- गैर-परिवार गवाह प्रणाली:-
- 1. निष्पक्ष गवाह (जैसे शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) की उपस्थिति।
- 2. मतदान निर्देश निजी रूप से पढ़कर सुनाए जाएँ।
- मजबूत शिकायत निवारण तंत्र:
- 1. त्वरित शिकायत निपटान और हेल्पलाइन।
- 2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58A के तहत पुनर्मतदान की व्यवस्था।
निष्कर्ष:-
गृह-मतदान तंत्र भारत की वृद्ध होती जनसंख्या और दिव्यांग नागरिकों के लिए निर्वाचन समावेशन का एक प्रगतिशील प्रयास है, जो सहभागितापूर्ण लोकतंत्र की ओर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- फिर भी, यह आवश्यक है कि समावेशन के नाम पर चुनावी अखंडता, गोपनीयता और स्वतंत्रता से समझौता न किया जाए। सुलभता और अखंडता, तथा समावेशन और निष्पक्षता के बीच संतुलन का सूक्ष्म मूल्यांकन अनिवार्य है।
आगे की राह:-
- पायलट परियोजनाओं के परिणामों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर का स्पष्ट एवं कठोर ढाँचा तैयार किया जाए।
- बहु-पक्षीय परामर्श के तहत नागरिक समाज, दिव्यांग संगठनों, राजनीतिक दलों और निर्वाचन अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- संवैधानिक मूल्यों को आधार बनाते हुए, “स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर मतदान” का अधिकार मतदाता के घर की चारदीवारी के भीतर भी सुरक्षित रखा जाए।