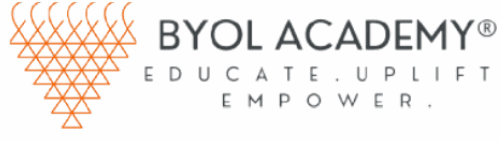क. एक राष्ट्र, एक चुनाव: व्यवहार्यता और संघीय प्रभाव
छात्रों के लिए
लेख का संदर्भ:-
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (ONOE) पर उच्चस्तरीय समिति (HLC) — जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने की — ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का तर्क है कि इससे चुनावी थकान, चुनावी व्यय और प्रशासनिक व्यवधान कम होंगे। यह रिपोर्ट चुनावी दक्षता और संविधान की संघीय संरचना के बीच संतुलन को लेकर चल रही पुरानी बहस को एक बार फिर तेज कर देती है।
UPSC पेपर विषय:-
GS पेपर-II – राजनीति एवं प्रशासन (निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सुधार, संघवाद) ।
GS पेपर-II – संविधान (संघीय संरचना, शक्तियों का पृथक्करण) ।
GS पेपर-II – भारतीय लोकतंत्र (सहभागी शासन, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ) ।
GS पेपर-II – सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप (HLC की सिफारिशें) ।
लेख के आयाम:-
- एक राष्ट्र, एक चुनाव की पृष्ठभूमि और तर्क ।
- HLC 2024 की प्रमुख सिफारिशें ।
- आवश्यक कानूनी और संवैधानिक संशोधन ।
- संघीय और लोकतांत्रिक चुनौतियाँ ।
- अंतरराष्ट्रीय अनुभवों की तुलना ।
- भारत में निर्वाचन सुधार की आगे की राह।
चर्चा में क्यों ?:-
मार्च 2024 में, उच्चस्तरीय समिति (HLC) ने 18,626 पृष्ठों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 2029 से लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की चरणबद्ध योजना का प्रस्ताव दिया गया। यह रिपोर्ट राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, विधि आयोग और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों से परामर्श के बाद तैयार की गई थी। इस प्रस्ताव ने लोकतांत्रिक अखंडता, संघीय संतुलन, व्यावहारिकता और संवैधानिक वैधता को लेकर बहस को तेज कर दिया है।
मुख्य विशेषताएँ:-
1. HLC की ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (ONOE) पर सिफारिशें:-
- 1. 2029 तक दो चरणों में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना।
- 2. चुनावी चक्र को समन्वित करने के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव।
- 3. लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एकीकृत मतदाता सूची और समान मतदाता सूची बनाने का सुझाव।
- 4. अनुच्छेद 83, 172, 356 और दसवीं अनुसूची में संशोधन की अनुशंसा, ताकि कार्यकाल एकसमान हो सके।
- 5. एक स्थायी संस्था – राष्ट्रीय निर्वाचन परिषद (National Electoral Council) का गठन, जो भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के साथ समन्वय करेगी।
2. समिति द्वारा दिए गए तर्क:-
- 1. बार-बार चुनाव से शासन और विकास कार्यों में व्यवधान।
- 2. उच्च वित्तीय लागत – केवल 2019 के आम चुनाव में लगभग ₹10,000 करोड़ का व्यय।
- 3. मानव संसाधनों (विशेषकर सुरक्षा बल और शिक्षक) पर दबाव।
- 4. आदर्श आचार संहिता (MCC) से नीतिगत निर्णयों में देरी।
- 5. निरंतर चुनावी माहौल से राजनीतिक ध्रुवीकरण और लोकलुभावन राजनीति।
3. संवैधानिक और कानूनी अड़चनें:-
- 1. कई संवैधानिक अनुच्छेदों में संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 368(2) के तहत आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक।
- 2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन की आवश्यकता।
- 3. कार्यकाल पूरा होने से पहले विधानसभाओं का विघटन, राज्यों की संघीय स्वायत्तता को चुनौती।
- 4. अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की आशंका – चुनाव समन्वय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की संभावना।
4. संघवाद और लोकतांत्रिक चिंताएँ:-
- 1. संविधान राज्यों के स्वायत्त कार्य और स्वतंत्र चुनावी चक्र को मान्यता देता है।
- 2. राज्यों के लोकतांत्रिक अधिकार और चुनावी समय-निर्धारण पर नियंत्रण कम हो सकता है।
- 3. छोटे दल और क्षेत्रीय आवाज़ें राष्ट्रीय मुद्दों के साये में दब सकती हैं।
- 4. दलबदल विरोधी कानून और मध्यावधि अस्थिरता, स्थिर कार्यकाल की अवधारणा को कमजोर कर सकती है।
5. तुलनात्मक अनुभव और वैश्विक परिप्रेक्ष्य:-
- 1. दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और इंडोनेशिया में एक साथ चुनाव होते हैं।
- 2. लेकिन वहां का संघीय ढांचा कमजोर या अस्तित्वहीन है।
- 3. भारत की विविधता और राज्यों की मजबूत स्थिति इसे लागू करना कठिन बनाती है।
व्याख्या:-
1. क्या भारत में एक साथ चुनाव की अवधारणा नई है?
नहीं, यह नई अवधारणा नहीं है। भारत में 1951 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। यह इसलिए संभव था क्योंकि केंद्र और राज्यों की सरकारों का कार्यकाल एक साथ समाप्त होता था और हर पांच साल में चुनाव एक साथ कराए जाते थे।लेकिन यह प्रणाली तब टूटी जब 1970 में चौथी लोकसभा का कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो गया। इसके बाद कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण चुनावी चक्र अलग-अलग हो गए।
यह विचार कई बार सामने आया:-
- विधि आयोग (1999 व 2018):- ने आवश्यक संवैधानिक संशोधनों के साथ इसकी सिफारिश की।
- नीति आयोग (2017):-ने प्रशासनिक दक्षता, चुनावी व्यय में कमी और सुचारू शासन को इसके प्रमुख लाभ बताया।
इस प्रकार, यह प्रस्ताव नया नहीं है बल्कि चुनावी थकान कम करने और नीतिगत निरंतरता लाने का एक पुनःस्थापना प्रयास है।
2. अभी इसे पुनर्जीवित क्यों किया जा रहा है?
2014 के बाद यह प्रस्ताव निम्न कारणों से प्रमुखता में आया:-
- चुनावी थकान – भारत में हर साल अलग-अलग स्तरों पर कई चुनाव होते हैं, जिससे शासन बाधित होता है।
- आदर्श आचार संहिता (MCC) से विकास योजनाओं और घोषणाओं में देरी।
- चुनावी खर्च में वृद्धि – जैसे, 2019 के लोकसभा चुनाव में ₹10,000 करोड़ से अधिक खर्च हुआ।
सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया, जिसने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 2029 तक चरणबद्ध तरीके से ONOE लागू करने की सिफारिश की।
3. निर्वाचन आयोग (ECI) का रुख क्या है?
1983 से ही निर्वाचन आयोग इस विचार के प्रति सावधानीपूर्वक समर्थन देता रहा है। सिद्धांततः ECI ONOE के पक्ष में है क्योंकि:-
- प्रशासनिक और सुरक्षा मशीनरी पर भार कम होगा।
- मतदाताओं की भागीदारी अधिक प्रभावी होगी।
- चुनावी व्यय में कमी आएगी।
लेकिन ECI ने ज़ोर दिया कि:-
- लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को समन्वित करने के लिए स्पष्ट रोडमैप बने।
- EVMs, VVPATs और मानव संसाधन में बड़े पैमाने पर वृद्धि हो।
- मध्यावधि विघटन, उपचुनाव और संवैधानिक चुनौतियों से निपटने के लिए राजनीतिक सहमति हो।
4. क्या मध्यावधि विघटन से समन्वय बिगड़ सकता है?
हाँ। भारत की संसदीय व्यवस्था लचीली है:-
- अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर सकती है।
- विधानसभाओं का समय से पहले विघटन संभव है।
- त्रिशंकु सदन, इस्तीफे या बहुमत खोने से भी समयपूर्व चुनाव हो सकते हैं।
इन स्थितियों से चुनावी समन्वय टूट सकता है।
HLC (2024) द्वारा सुझाव :-
Constructive Vote of No Confidence (जर्मनी की तरह) लागू हो, यानी पुरानी सरकार हटाने से पहले नई सरकार तय हो।यदि मध्यावधि चुनाव हों, तो नई सरकार केवल शेष कार्यकाल के लिए चले, ताकि चक्र बना रहे।
5. राजनीतिक सहमति कैसे बनेगी?
यह ONOE लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती है:-
- क्षेत्रीय दल और विपक्ष मानते हैं कि यह संघवाद को कमजोर कर सकता है, क्योंकि राज्यों का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
- छोटे दलों को डर है कि राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय चुनावों में हावी हो जाएंगे।
- सत्ता का केन्द्रीकरण, भारत की बहुलतावादी लोकतांत्रिक संरचना को कमजोर कर सकता है।
समाधान के तर्क:-
- केंद्र सरकार को राज्यों और राजनीतिक हितधारकों से सार्थक संवाद करना होगा।
- कानून में ऐसे प्रावधान हों जो राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा करें।
- अंतर-राज्य परिषद, विधि आयोग और संसदीय समितियों के साथ मिलकर सहमति-आधारित रोडमैप तैयार किया जाए।
निष्कर्ष:-
“एक राष्ट्र, एक चुनाव” प्रस्ताव का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता, व्यय में कमी और नीतिगत निरंतरता है। लेकिन इसके क्रियान्वयन में संवैधानिक गरिमा, संघीय विविधता और चुनावी न्याय का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
- समान चुनावी चक्र लागू करने के बजाय, भारत को चरणबद्ध समन्वय मॉडल अपनाना चाहिए, जैसा कि HLC ने सुझाव दिया है, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट और स्पष्ट कानूनी ढांचा हो।
- चुनावी सुधार केवल लागत घटाने के लिए नहीं, बल्कि हर स्तर पर नागरिक सशक्तिकरण के लिए होने चाहिए। एक सुदृढ़ चुनावी व्यवस्था को शासन की स्थिरता और प्रतिनिधित्व की समावेशिता – भारतीय संघीय लोकतंत्र के इन दो स्तंभों – को समान महत्व देना होगा।