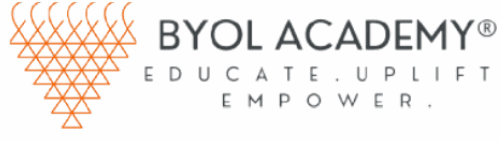d. प्रास्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ की वैधता
छात्रों के लिए नोट्स
लेख की पृष्ठभूमि:-
डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2024) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रास्तावना में “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, जिनमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इन शब्दों को जोड़ने को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति की पुष्टि की और यह भी कहा कि भारतीय संविधान मूल्यों की एक निरंतर विकसित होती धारा है।
UPSC पेपर विषय से संबंध:-
- GS Paper II – भारतीय संविधान: प्रास्तावना, संशोधन, बुनियादी ढांचा सिद्धांत
- GS Paper IV – शासन में नैतिकता: संवैधानिक नैतिकता, लोकतांत्रिक मूल्य
- निबंध – संवैधानिकता, न्याय, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक विकास
लेख के आयाम:-
- 1. प्रास्तावना की भूमिका: प्रतीकात्मक और मानक दस्तावेज़ के रूप में
- 2. अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति और मूल संरचना सिद्धांत
- 3. भारतीय राजनीतिक-नैतिक विमर्श में “धर्मनिरपेक्ष” और “समाजवादी” का विकास
- 4. न्यायिक व्याख्या और संवैधानिक नैतिकता
- 5. जन-विश्वास, संस्थागत नैतिकता और शासन में प्रतीकात्मक निरंतरता
चर्चा में क्यों ?:-
दिसंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें प्रास्तावना में “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों की वैधता को चुनौती दी गई थी। ये शब्द आपातकाल (1976) के दौरान 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये जोड़ संविधान सभा की मूल दृष्टि का हिस्सा नहीं थे और इन पर जनता की सहमति नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को प्रास्तावना में संशोधन का अधिकार है, बशर्ते यह मूल संरचना को प्रभावित न करे।
मुख्य बातें:-
1. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम (1976):-
- “मिनी संविधान” कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यापक बदलाव किए गए।
- प्रास्तावना में “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” और “अखंडता” शब्द जोड़े।
- शिक्षा, वन, न्याय जैसे विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया।
- भाग IV-A (मौलिक कर्तव्य) और भाग XIV-A (प्रशासनिक न्यायाधिकरण) जोड़े।
- डीपीएसपी (राज्य के नीति निदेशक तत्व) में समाज कल्याण व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संशोधन किए।
2. याचिकाकर्ताओं का तर्क:-
- प्रास्तावना की अंगीकरण तिथि (26 नवम्बर 1949) के बाद इसकी सामग्री स्थायी हो गई थी।
- “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” जोड़ राजनीतिक अवसरवादिता के प्रतीक हैं, न कि संवैधानिक सर्वसम्मति के।
3. सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन:-
- अनुच्छेद 368 संसद को किसी भी प्रावधान को “जोड़ने, बदलने या हटाने” का अधिकार देता है।
- संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है, जो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होता है।
- “धर्मनिरपेक्ष” और “समाजवादी” जोड़ने से मूल संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि उसे और पुष्ट किया गया।
4. न्यायिक परिभाषाएँ पुनः स्थापित:-
- धर्मनिरपेक्षता: सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और राज्य की निष्पक्षता।
- केशवानंद भारती (1973) और एस.आर. बोम्मई (1994) में इसे संविधान की मूल संरचना माना गया।
- समाजवाद: समान विकास, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य के प्रति प्रतिबद्धता।
5. संवैधानिक प्रतीकवाद और संस्थागत नैतिकता:-
- इन शब्दों का समावेश शासन नीति को नैतिक दृष्टि से मार्गदर्शन देता है।
- प्रतीकात्मक रूप से यह भारत की पहचान को एक बहुलतावादी, कल्याणकारी लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में मजबूत करता है।
व्याख्या:-
1. प्रास्तावना केवल प्रतीकात्मक क्यों नहीं है?
प्रास्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में लागू नहीं होती, पर यह एक दार्शनिक दिशा-दर्शक है।
- “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्द संविधान की मौजूदा भावना से मेल खाते हैं।
- उदाहरण:-
- अनुच्छेद 14 (समानता),
- अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार व गरिमा),
- अनुच्छेद 38, 39, 39A (सामाजिक-आर्थिक न्याय)।
न्यायालय ने कई बार प्रास्तावना का सहारा लेकर अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या की है (बेहरुबारी मामला 1960, केशवानंद भारती 1973)।
2. क्या अनुच्छेद 368 प्रास्तावना में संशोधन की अनुमति देता है?
हाँ। केशवानंद भारती मामला (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया:
- संसद को अनुच्छेद 368 के तहत प्रास्तावना में संशोधन का अधिकार है।
- परंतु कोई भी संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकता।
- 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” मूल संरचना को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करते हैं।
3. संवैधानिक मूल्य समय के साथ क्यों बदलते हैं?
एक कठोर संविधान बदलते समाज में अप्रासंगिक हो सकता है। भारतीय संविधान को जान-बूझकर एक जीवंत दस्तावेज़ बनाया गया है।
- मूल्य बदलते हैं न्यायिक व्याख्या, विधायी सुधार और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से।
- उदाहरण:-
- नवतेज सिंह जोहर (2018) – LGBTQ+ अधिकार मान्यता,
- जोसफ शाइन (2018) – व्यभिचार अपराध का निरस्तीकरण,
- शायरा बानो (2017) – तीन तलाक अमान्य।
इनसे साबित होता है कि संवैधानिक नैतिकता समय के साथ समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होती है।
4. इस निर्णय का संस्थागत नैतिकता से क्या संबंध है?
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस बात का उदाहरण है कि संस्थान संवैधानिक मूल्यों के प्रति ईमानदार बने रहें।
- “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” को मान्यता देकर न्यायालय ने:
- संवैधानिक व्याख्या की नैतिक निरंतरता को बनाए रखा।
- राजनीतिक संशोधनवाद का प्रतिरोध किया।
- संविधान की नैतिक आत्मा की रक्षा की।
इससे यह सिद्ध हुआ कि संस्थाएँ लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षक होनी चाहिए, न कि दलगत राजनीति की साधन।
निष्कर्ष:-
डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2024) का निर्णय भारतीय संविधान की आत्मा को पुनः पुष्ट करता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद की प्रतिस्पर्धी कथाओं के दौर में यह फैसला कानूनी स्पष्टता और नैतिक दृढ़ता दोनों का उदाहरण है।
- प्रास्तावना में “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” का समावेश किसी असंगति का नहीं, बल्कि भारत की बहुलतावादी और कल्याणकारी लोकतांत्रिक पहचान का सुदृढ़ीकरण है।
- संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर यह निर्णय भीम राव अंबेडकर की उस दृष्टि को प्रतिध्वनित करता है कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सार्थक है जब वह सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित हो।