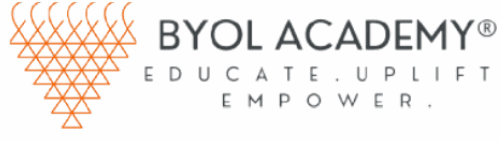विद्यार्थियों के लिए नोट्स
लेख की पृष्ठभूमि:-
यह लेख अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर आयोग (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) के 33वें सत्र में भारत की सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है। इसमें यह दर्शाया गया है कि भारत किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय मानकों का केवल अनुयायी नहीं रहा, बल्कि आज वह एक प्रमुख योगदानकर्ता और अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। लेख में भारत के प्रमुख योगदानों का उल्लेख है – जैसे घरेलू आपराधिक कानूनों का आधुनिकीकरण, साइबर अपराध से मुकाबला, और आतंकवाद विरोधी वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन – जो यह दर्शाता है कि भारत किस प्रकार एक अधिक प्रभावी और न्यायसंगत वैश्विक आपराधिक न्याय ढाँचे को आकार देने में भूमिका निभा रहा है।
UPSC GS पेपर विषय:-
- यह विषय UPSC GS पेपर-II : शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से इसमें –
- अंतरराष्ट्रीय संबंध : प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, एजेंसियाँ, और मंच, उनकी संरचना और दायित्व।
- शासन और राजनीति : सरकारी नीतियाँ एवं विकास हेतु हस्तक्षेप तथा उनसे उत्पन्न समस्याएँ।
- आंतरिक सुरक्षा : संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच कड़ियाँ।
लेख के आयाम:-
- भारत के घरेलू सुधार : हाल ही में भारत ने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलकर भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) लागू किए हैं।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग : आतंकवाद और साइबर अपराध जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने हेतु वैश्विक तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में भारत का योगदान।
- तकनीकी एकीकरण : आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने हेतु तकनीक का उपयोग – जैसे Inter-operable Criminal Justice System (ICJS) और Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)।
- नीति पक्षधरता : भारत का यह प्रयास कि वैश्विक आपराधिक न्याय प्रणाली संतुलित हो, जहाँ कानून प्रवर्तन की ज़रूरतें और मानवाधिकार दोनों संरक्षित रहें।
वर्तमान संदर्भ:-
वियना (ऑस्ट्रिया) में आयोजित CCPCJ के 33वें सत्र ने सदस्य देशों को समकालीन आपराधिक न्याय चुनौतियों पर विचार-विमर्श का अवसर दिया। भारत की भागीदारी विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसने हाल के कानूनी सुधारों को प्रस्तुत किया, जो शीघ्र प्रभाव में आने वाले हैं। साइबर खतरों से लेकर अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध तक से जूझ रही दुनिया के लिए भारत का योगदान इस बात का प्रमाण है कि वह घरेलू आधुनिकीकरण और वैश्विक सहयोग – दोनों को लेकर गंभीर है। भारत ने मंच से आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति और साइबर अपराध पर व्यापक दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिससे वह वैश्विक प्रयासों का एक विश्वसनीय साझेदार बनकर उभरा।
समाचार की मुख्य विशेषताएँ:-
- विधायी सुधारों का प्रदर्शन :-
- भारत ने अपने नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) को आधुनिक एवं प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में एक प्रगतिशील कदम बताया।
- तकनीक पर जोर :–
- भारत ने ICJS जैसी डिजिटल पहलें प्रस्तुत कीं जो पुलिस, अदालत और कारागार जैसी संस्थाओं को जोड़ती हैं। साथ ही I4C की भूमिका को भी रेखांकित किया गया जो साइबर अपराध से समन्वित ढंग से निपटता है।
- वैश्विक सहयोग की वकालत :–
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के भीतर अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचे को मजबूत करने, खासकर आतंकवाद और उसके वित्तपोषण के विरुद्ध, की आवश्यकता दोहराई।
- अनुभव साझा करना :–
- अपने विशाल आकार और विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत ने अन्य देशों के साथ पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन से जुड़े अनुभव साझा करने का प्रस्ताव दिया – चाहे वह सामान्य अपराध हो या डार्क नेट जैसी जटिल चुनौतियाँ।
स्पष्टीकरण:-
1. अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर आयोग (CCPCJ) क्या है?
- CCPCJ, अपराध निवारण और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति-निर्माण निकाय है। इसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) ने स्थापित किया था।
- यह सदस्य देशों को विशेषज्ञता साझा करने, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रणनीतियाँ बनाने और अपराध से निपटने की प्राथमिकताएँ तय करने का मंच प्रदान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और आपराधिक न्याय कांग्रेस की तैयारी भी करता है और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) का शासी निकाय है। इसका कार्य कानून के शासन को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करना है।
2. भारत के नए आपराधिक कानून CCPCJ के उद्देश्यों से कैसे मेल खाते हैं?
- भारत द्वारा हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम औपनिवेशिक युगीन कानूनों को बदलते हुए एक आधुनिक कानूनी ढाँचा प्रस्तुत करते हैं। इन कानूनों का उद्देश्य प्रक्रिया में देरी को कम करना, न्यायिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करना और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल करना है। ये CCPCJ के उद्देश्यों – प्रभावी और न्यायसंगत आपराधिक न्याय प्रशासन – के अनुरूप हैं। साथ ही, साइबर अपराध जैसे नए युगीन अपराधों को विधिक रूप से परिभाषित कर इन कानूनों ने वैश्विक प्रयासों को भी मजबूती दी है।
3. 33वें CCPCJ सत्र में साइबर अपराध पर भारत की भूमिका क्या रही?
- भारत ने साइबर अपराध से निपटने के अपने व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। इसमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल जैसी नागरिक-केन्द्रित पहलें शामिल हैं। भारत ने यह भी रेखांकित किया कि साइबर खतरों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है और इनके लिए तकनीकी सहयोग एवं अनुभव साझा करना अनिवार्य है।
4. संयुक्त राष्ट्र मंच पर आतंकवाद के प्रति ‘शून्य सहिष्णुता’ नीति पर भारत का जोर क्यों महत्वपूर्ण है?
- आतंकवाद, विशेषकर संगठित अपराध से जुड़ा हुआ, वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। भारत का यह आग्रह कि किसी भी रूप या उद्देश्य का आतंकवाद स्वीकार्य नहीं हो सकता, वैश्विक सहमति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। भारत के दशकों लंबे आतंकवाद-विरोधी अनुभव ने उसकी स्थिति को और अधिक सशक्त बनाया है। CCPCJ जैसे मंच पर भारत का यह संदेश अंतरराष्ट्रीय खुफिया सहयोग और आतंकवादियों के अभियोजन हेतु कानूनी ढाँचे को मजबूती प्रदान करता है।
5. CCPCJ में भारत की भागीदारी उसके वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरते स्थान को कैसे दर्शाती है?
- भारत की भूमिका अब केवल अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुसरण करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सर्वोत्तम प्रथाओं का योगदानकर्ता बन चुका है। घरेलू सुधारों और तकनीकी प्रगति को प्रस्तुत कर भारत विकासशील देशों के लिए प्रेरणास्रोत बन रहा है। साथ ही, संतुलित और न्यायपूर्ण वैश्विक ढाँचे की पैरवी करते हुए भारत यह दर्शाता है कि वह नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व करने को तैयार है।
निष्कर्ष:-
33वें CCPCJ सत्र में भारत की सक्रिय भागीदारी वैश्विक आपराधिक न्याय सुधारों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। घरेलू कानूनों के आधुनिकीकरण और तकनीक के उपयोग से भारत अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है।
- आगे की राह यह है कि भारत आतंकवाद, साइबर अपराध और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के अभियोजन जैसे मुद्दों पर मजबूत वैश्विक कानूनी ढाँचे की पैरवी करता रहे। साथ ही, तकनीकी निवेश और क्षमता निर्माण में निरंतर सुधार करे तथा अपने अनुभव साझेदार देशों से साझा करे।
- एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर – जिसमें कठोर कानून प्रवर्तन और मानवाधिकार दोनों सुरक्षित हों – भारत विश्व को अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित बनाने में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है।