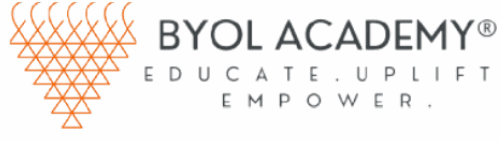छात्रों के लिए नोट्स
आलेख का संदर्भ:-
यह लेख इस पर चर्चा करता है कि किस प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, जो मूल रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे, अब तेजी से दुष्प्रचार फैलाने, हिंसा भड़काने, समुदायों को ध्रुवीकृत करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए दुरुपयोग किए जा रहे हैं। यह इस बात का मूल्यांकन करता है कि किस हद तक सीमित डिजिटल स्पेस आंतरिक अशांति और सामाजिक कलह में योगदान कर सकते हैं।
UPSC GS पेपर विषय संबंध:-
सामान्य अध्ययन पत्र-II:-
- सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही
- आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका
- आंतरिक सुरक्षा के संरक्षण हेतु तंत्र, कानून, संस्थान
सामान्य अध्ययन पत्र-III:-
- आंतरिक सुरक्षा
- गैर-राज्य कर्ताओं की भूमिका
- साइबर सुरक्षा
आलेख के आयाम:-
- सोशल मीडिया और दुष्प्रचार का उभार
- लोकतांत्रिक विमर्श और विकल्पों पर प्रभाव
- नफरत, हिंसा और अफवाहों का प्रसार
- नियामकीय और कानूनी चुनौतियाँ
- राज्य और नागरिक समाज की भूमिका
- वैश्विक तुलना और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का शासन
वर्तमान संदर्भ:-
- हाल ही में मणिपुर, नूंह (हरियाणा) और दिल्ली में हुई हिंसा ने यह दिखाया कि किस प्रकार फ़ेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर झूठे वीडियो, नफ़रत फैलाने वाले भाषण और भड़काऊ पोस्ट का उपयोग किया गया।
- भारत के विधि आयोग ने इस मुद्दे को रेखांकित किया है कि सीमित डिजिटल स्पेस सामूहिक और जातीय तनाव को बढ़ा रहे हैं।
भारतीय सरकार द्वारा सोशल मीडिया कंपनियों को अवैध सामग्री हटाने का निर्देश और कड़े आईटी नियमों के प्रस्ताव, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के प्रति बढ़ती चिंता को दर्शाते हैं।
समाचार की विशेषताएँ:-
- अप्रमाणित व हेरफेर की गई सामग्री का व्यापक प्रसार भय और सामुदायिक कलह पैदा करता है।
- इको चेंबर और एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह विचारधारात्मक ध्रुवीकरण को बढ़ाते हैं।
- टेक कंपनियों की जवाबदेही की कमी और उपयोगकर्ताओं की गुमनामी नियमन को जटिल बनाती है।
- आईपीसी की धारा 153ए और 505 जैसे कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन।
- तेज़ वायरलिटी सरकार और क़ानून प्रवर्तन की प्रतिक्रिया से कहीं आगे निकल जाती है।
व्याख्या:-
प्रश्न 1. भारत में सोशल मीडिया किस प्रकार आंतरिक अशांति में योगदान देता है?
- सोशल मीडिया फेक न्यूज़, नफ़रत फैलाने वाले भाषण और बड़े पैमाने पर प्रचार का साधन बनता जा रहा है। हाल के साम्प्रदायिक दंगों में भड़काऊ झूठे वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित हुए, जिनसे हिंसा भड़की और समुदायों के बीच विभाजन गहरा हुआ।
- व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर गुमनामी और तथ्य-जाँच की कमी के कारण ऐसा कंटेंट अनियंत्रित रूप से फैल जाता है, जिससे दंगे, लिंचिंग और व्यापक असुरक्षा उत्पन्न होती है।
प्रश्न 2. सोशल मीडिया को लोकतांत्रिक विमर्श के लिए खतरा क्यों माना जाता है?
- लोकतांत्रिक विमर्श एक सूचित जनसमूह और सम्मानजनक बहस पर आधारित होता है। लेकिन सोशल मीडिया अक्सर सनसनी और आक्रोश को बढ़ावा देता है।
- एल्गोरिद्म उग्र विचारों को amplify करते हैं, संयमित आवाज़ों को हतोत्साहित करते हैं और डिजिटल इको चेंबर पैदा करते हैं। इससे जनमत विकृत होता है, सहमति-निर्माण कमजोर होता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा घटता है।
प्रश्न 3. सोशल मीडिया को नियंत्रित करने में भारतीय प्राधिकारियों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
- आईटी नियम 2021 के बावजूद, प्रवर्तन कठिन है क्योंकि टेक कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होती हैं, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मौजूद है और नागरिक स्वतंत्रता समूह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर विरोध करते हैं।
- साथ ही, वायरल दुष्प्रचार की गति तथ्य-जाँच तंत्र या कानूनी प्रतिक्रियाओं से कहीं तेज़ होती है।
प्रश्न 4. ऑनलाइन उकसावे और दुष्प्रचार को रोकने के लिए कौन-से कानूनी तंत्र उपलब्ध हैं?
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 153ए, 295ए, 505 और गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA) का उपयोग हिंसा भड़काने वालों पर मुकदमा चलाने में होता है।
- 2021 के केंद्रीय दिशानिर्देश प्लेटफ़ॉर्म्स पर अवैध सामग्री शीघ्र हटाने की ज़िम्मेदारी डालते हैं। फिर भी, इनका कार्यान्वयन असंगत और विवादास्पद है।
प्रश्न 5. इस क्षेत्र में भारत किन अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं से सीख सकता है?
- जर्मनी का NetzDG क़ानून प्लेटफ़ॉर्म्स पर कड़े समय-सीमा और जुर्माने लागू करता है। यूरोपीय संघ का डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट एल्गोरिद्म और सामग्री मॉडरेशन में पारदर्शिता को अनिवार्य बनाता है।
- भारत भी इसी तरह की व्यवस्थाएँ अपना सकता है, पर उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता जैसे मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित करना होगा।
निष्कर्ष / आगे की राह:-
हालाँकि सोशल मीडिया ने सूचना तक पहुँच को सामान्य बना दिया है, परंतु इसका दुरुपयोग सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर ख़तरे उत्पन्न करता है। एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण आवश्यक है — जिसमें सख़्त नियामकीय ढाँचे, प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही, नागरिकों में डिजिटल साक्षरता और मज़बूत तथ्य-जाँच तंत्र शामिल हों। क़ानूनों को तकनीक के साथ विकसित होना होगा और एक संतुलित मॉडल की आवश्यकता है, जो सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं दोनों की रक्षा करते हुए डिजिटल युग में लोकतांत्रिक विमर्श को सुरक्षित रख सके।