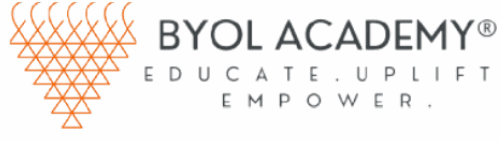छात्रों के लिए नोट्स
लेख का संदर्भ:-
हाल ही में हुए बड़े पैमाने के वैश्विक आईटी आउटेज — जैसे क्राउडस्ट्राइक (CrowdStrike) के हालिया अपडेट की खराबी से उत्पन्न व्यवधान — ने एयरलाइन संचालन, बैंकिंग सेवाओं, मीडिया संस्थानों और यहाँ तक कि सार्वजनिक संस्थाओं को प्रभावित किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र कितने नाजुक हैं और भारत की आईटी अवसंरचना में मज़बूत साइबर रेज़िलियेंस की कितनी अहम ज़रूरत है।
UPSC GS पेपर टॉपिक से संबंध:-
- GS पेपर – 3 : आंतरिक सुरक्षा:-
- साइबर सुरक्षा
- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ
- आंतरिक सुरक्षा में बाहरी राज्य और गैर-राज्य कारकों की भूमिका
लेख के आयाम:-
- वैश्विक स्तर पर आईटी आउटेज का प्रभाव
- भारत के महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे में कमजोरियाँ
- नीतिगत और विनियामक (Regulatory) कमियाँ
- साइबर रेज़िलियेंस तंत्र और ढांचे
- CERT-In, NCX और सार्वजनिक-निजी साझेदारी की भूमिका
- स्वदेशी साइबर सुरक्षा समाधान का महत्व
- साइबर खतरों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग
वर्तमान संदर्भ:-
19 जुलाई 2024 को क्राउडस्ट्राइक (CrowdStrike) की एक ख़राब अपडेट के कारण, जिसने माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स को प्रभावित किया, वैश्विक आईटी आउटेज हुआ और दुनियाभर की आवश्यक सेवाएँ ठप हो गईं। भारत में भी बैंकों, हवाई अड्डों और अस्पतालों में व्यवधान सामने आया। इस घटना ने कुछ वैश्विक तकनीकी विक्रेताओं पर अत्यधिक निर्भरता के ख़तरों को उजागर किया और भारत के लिए एक स्वतंत्र, लचीला और सुरक्षित डिजिटल ढाँचा बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
समाचार की विशेषताएँ:-
- एकल विफलता (Single Point of Failure) से विश्वव्यापी व्यवधान
- भारत में एयरलाइंस, बैंक और मीडिया संस्थान ठप पड़े
- क्राउडस्ट्राइक अपडेट त्रुटि से विंडोज प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापक सिस्टम क्रैश
- व्यवधान ने बैकअप और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की कमी को उजागर किया
- विदेशी सॉफ़्टवेयर पर निर्भरता और साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिमों पर चिंता बढ़ी
व्याख्या:-
प्रश्न 1. हालिया वैश्विक आईटी आउटेज का कारण क्या था और भारत पर इसका क्या असर हुआ?
- यह आउटेज क्राउडस्ट्राइक के ख़राब सॉफ़्टवेयर अपडेट से हुआ, जिसने दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम को प्रभावित किया।
- भारत में इससे नागर विमानन (इंडिगो, एयर इंडिया), बैंकिंग, मीडिया प्रसारण और अस्पताल जैसे क्षेत्रों में व्यवधान हुआ, जिससे सेवाएँ घंटों तक बाधित रहीं।
प्रश्न 2. भारत के लिए ऐसे आउटेज क्यों चिंता का विषय हैं?
- भारत की तेज़ डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया के कारण बैंकिंग, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएँ वैश्विक तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म पर निर्भर हैं।
- स्वदेशी साइबर टूल्स की कमी और विदेशी सॉफ़्टवेयर पर अत्यधिक निर्भरता भारत को बड़े पैमाने पर व्यवधानों के प्रति असुरक्षित बनाती है।
प्रश्न 3. साइबर रेज़िलियेंस क्या है और यह साइबर सुरक्षा से कैसे अलग है?
- साइबर सुरक्षा (Cybersecurity) मुख्य रूप से साइबर हमलों को रोकने पर केंद्रित होती है, जबकि साइबर रेज़िलियेंस (Cyber Resilience) किसी सिस्टम की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह हमलों या विफलताओं का सामना कर सके, उन पर प्रतिक्रिया दे सके और उनसे उबर सके।
- इसमें तैयारी, बैकअप, रीयल-टाइम प्रतिक्रिया और सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना शामिल है।
प्रश्न 4. भारत में साइबर खतरों के प्रबंधन के लिए कौन-से तंत्र मौजूद हैं?
भारत में प्रमुख संस्थाएँ और योजनाएँ हैं :
- CERT-In (इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम) : घटनाओं का प्रबंधन
- NCIIPC (National Critical Information Infrastructure Protection Centre)
- Cyber Crisis Management Plan (CCMP) : आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए
हालाँकि, इन तंत्रों में और बेहतर समन्वय, तकनीकी उन्नयन और तेज़ रीयल-टाइम प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
प्रश्न 5. भारत को साइबर रेज़िलियेंस अवसंरचना विकसित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
- सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अतिरिक्त बैकअप सिस्टम विकसित करना
- स्वदेशी सॉफ़्टवेयर और साइबर सुरक्षा टूल्स को बढ़ावा देना
- तैयारी के लिए साइबर अभ्यास और सिमुलेशन आयोजित करना
- नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCCC) को और मज़बूत करना
- अनिवार्य ब्रीच रिपोर्टिंग हेतु नियामक ढाँचे बनाना
- साइबर जोखिम प्रबंधन हेतु सार्वजनिक-निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना
निष्कर्ष:-
हालिया वैश्विक आईटी आउटेज भारत के लिए एक चेतावनी है कि केवल रिएक्टिव साइबर सुरक्षा पर निर्भर रहने के बजाय उसे प्रोएक्टिव साइबर रेज़िलियेंस ढाँचा अपनाना होगा। डिजिटलीकरण आर्थिक विकास और शासन को गति देता है, लेकिन इसे सुरक्षित, आत्मनिर्भर और त्रुटि-सहनशील अवसंरचना से ही स्थायी बनाया जा सकता है। भारत को साइबर विशेषज्ञों की नई पीढ़ी तैयार करनी होगी, साइबर सुरक्षा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा और सुरक्षित साइबरस्पेस के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग में नेतृत्व करना होगा। सार्वजनिक सुरक्षा और डिजिटल प्रणालियों पर जनता के विश्वास की रक्षा के लिए रणनीतिक निवेश, नीतिगत सुधार और क्षमता निर्माण आवश्यक हैं।