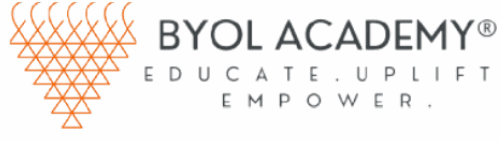छात्रों के लिए नोट्स
लेख का संदर्भ:-
सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA), 1958 मणिपुर में एक विवादास्पद कानून रहा है। इसे “अशांत क्षेत्रों” में सुरक्षा बलों को कानूनी प्रतिरक्षा (Legal Immunity) के साथ संचालन हेतु बनाया गया था। यह कानून मूल रूप से विद्रोह से निपटने के लिए लागू हुआ, लेकिन इस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि इसने मानवाधिकार उल्लंघनों को बढ़ावा दिया और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर किया। 2023 के बाद यह बहस और तेज हो गई, जब नैतिक असंतोष और नागरिकों की मौतों के कारण कानून को समाप्त करने की मांगें बढ़ीं।
UPSC GS पेपर विषय:-
- GS Paper II – शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध
- GS Paper III – आंतरिक सुरक्षा – सशस्त्र बल, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ
लेख के आयाम:-
- AFSPA की संवैधानिक और कानूनी आधारशिला
- केंद्र-राज्य संबंध और नागरिक प्रतिआरोप
- मानवाधिकार चिंताएँ और न्यायिक समीक्षा
- नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भूमिका
- सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता बहस
- मणिपुर में हाल की परिस्थितियाँ
वर्तमान संदर्भ:-
AFSPA को 2022 में मणिपुर के कुछ हिस्सों से आंशिक रूप से हटाया गया था। लेकिन 2023–24 की नई जातीय हिंसा के बाद कई क्षेत्रों को फिर “अशांत क्षेत्र” घोषित किया गया। इसने कानून की आवश्यकता और नैतिकता पर बहस को फिर से जगा दिया, खासकर वहाँ जहाँ राज्य सरकार प्रशासनिक नियंत्रण खोती दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी AFSPA के दुरुपयोग और कथित फर्जी मुठभेड़ों को लेकर दायर याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है।
खबर की मुख्य बातें:-
- हिंसा-प्रभावित हिस्सों में AFSPA का पुनः प्रवर्तन
- NHRC और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता
- नागरिक समाज और पीड़ित परिवारों द्वारा बार-बार कानून हटाने की मांग
- सरकार का पक्ष – सार्वजनिक सुरक्षा और पुलिस की सीमित क्षमता का हवाला
- AFSPA के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय
स्पष्टिकरण (Explainers):-
प्रश्न: AFSPA क्या है और यह कौन से अधिकार देता है?
- AFSPA “अशांत क्षेत्रों” में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देता है। इसमें गिरफ्तारी का अधिकार बिना वारंट, खतरे की आशंका होने पर गोली चलाने का अधिकार, और केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अभियोजन से प्रतिरक्षा शामिल है।
- यह 1958 में पूर्वोत्तर में विद्रोह से निपटने के लिए लागू हुआ और 1980 में मणिपुर तक बढ़ाया गया।
प्रश्न: मणिपुर में AFSPA विवादास्पद क्यों रहा है?
- इस कानून पर कई मानवाधिकार उल्लंघनों – जैसे हिरासत में मौत, फर्जी मुठभेड़ और यातना – के आरोप लगे। 2005 की जस्टिस जीवन रेड्डी समिति ने इसके निरसन की सिफारिश की थी, इसे “दमन का प्रतीक” बताते हुए।
- 2012 में इरोम शर्मिला का लंबा भूख हड़ताल और 2016 का सुप्रीम कोर्ट का 1,528 फर्जी मुठभेड़ों का मामला इस विरोध के प्रमुख उदाहरण हैं।
प्रश्न: AFSPA के संवैधानिक और कानूनी औचित्य क्या हैं?
- AFSPA की वैधता संविधान के अनुच्छेद 355 से आती है, जो केंद्र को राज्यों को “आंतरिक अशांति” से बचाने का दायित्व देता है।
- यह संघ सूची की प्रविष्टि 1 (रक्षा) और प्रविष्टि 2 (सशस्त्र बल) से समर्थित है। धारा 3 के तहत केंद्र सरकार, राज्य की सहमति के बिना भी, किसी क्षेत्र को “अशांत” घोषित कर सकती है। यही संघवाद पर सवाल खड़े करता है।
प्रश्न: AFSPA से जुड़े प्रमुख मानवाधिकार मुद्दे क्या हैं?
- मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि AFSPA सुरक्षा बलों को दण्डमुक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन करता है और प्राकृतिक न्याय व विधिक प्रक्रिया के सिद्धांत को कमजोर करता है।
- UNHRC और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टों में यातना, मनमानी गिरफ्तारी और मानवाधिकार हनन के मामले दर्ज हुए हैं।
प्रश्न: न्यायपालिका ने AFSPA पर क्या कहा है?
- 2016 के एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा और AFSPA के तहत पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं दी जा सकती।
- अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान भी जीवन के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता।
प्रश्न: AFSPA केंद्र-राज्य संबंधों को कैसे प्रभावित करता है?
- केंद्र का एकतरफा अधिकार कि वह बिना राज्य की सहमति के किसी क्षेत्र को “अशांत” घोषित कर सकता है, संघीय संतुलन को प्रभावित करता है।
- मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्यों ने बार-बार इस पर आपत्ति जताई है। 2022 में AFSPA की आंशिक वापसी को विश्वास बहाली का कदम माना गया, लेकिन यह अभी भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है।
प्रश्न: क्या पूर्वोत्तर के किसी हिस्से से AFSPA हटाया गया है?
- हाँ, त्रिपुरा (2015) और मेघालय (2018) से पूरी तरह, जबकि नगालैंड और मणिपुर (2022) के कुछ हिस्सों से AFSPA हटा लिया गया।
- लेकिन 2023–24 की जातीय हिंसा के कारण कुछ हिस्सों में इसे पुनः लागू कर दिया गया, जिससे इसकी चक्रीय और प्रतिक्रियात्मक प्रकृति पर सवाल उठे।
प्रश्न: AFSPA को चुनौती देने में नागरिक समाज की क्या भूमिका रही है?
- इरोम शर्मिला का आंदोलन, EEVFAM जैसे संगठन, और छात्र यूनियनों ने AFSPA विरोधी विमर्श को राष्ट्रीय स्तर पर जीवित रखा।
- कानूनी सक्रियता, अंतर्राष्ट्रीय अभियान और मीडिया रिपोर्टिंग ने लगातार मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर किया और न्याय, सत्य आयोगों तथा विधायी समीक्षा की मांग को बल दिया।
निष्कर्ष / आगे की राह:-
AFSPA मूलतः एक अस्थायी उपाय के रूप में लागू हुआ था, लेकिन इसका लंबे समय तक प्रवर्तन लोकतंत्र, जवाबदेही और विधि के शासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है – बेहतर पुलिसिंग, शांति स्थापना और स्थिर क्षेत्रों से कानून की चरणबद्ध वापसी। शिकायत निवारण के लिए मजबूत कानूनी तंत्र, साथ ही कार्यपालिका और न्यायपालिका की निगरानी आवश्यक है। राज्य की क्षमता को मजबूत करना और शासन में जनता का विश्वास बहाल करना ही पूर्वोत्तर को सैन्यीकृत समाधानों से आगे ले जा सकता है।