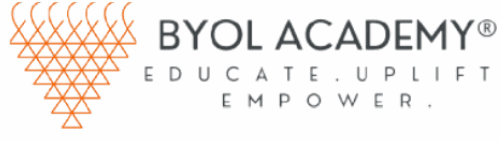छात्रों के लिए नोट्स
लेख का संदर्भ:-
भारत में क्षेत्रीयतावाद विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों से उत्पन्न होता है। एक विशाल और बहुलतावादी देश में स्थानीय आकांक्षाएँ स्वाभाविक हैं, किंतु जब ये राष्ट्रीय एकता और समग्रता के लिए खतरा बन जाती हैं तो यह चुनौती बन जाती है। यह विषय विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि राज्य की मांगों, स्वायत्तता और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर राजनीतिक आंदोलनों में वृद्धि देखी जा रही है।
UPSC GS पेपर से संबंध:-
- सामान्य अध्ययन पेपर II – शासन और राजनीति
- सामान्य अध्ययन पेपर I – भारतीय समाज (विविधता और एकता में विविधता)
- सामान्य अध्ययन पेपर III – आंतरिक सुरक्षा (अलगाववादी प्रवृत्तियों के संदर्भ में)
लेख के आयाम:-
- क्षेत्रीयतावाद के कारण
- क्षेत्रीयतावाद के रूप और प्रकार
- क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करने में संविधान की भूमिका
- राष्ट्रीय एकीकरण पर प्रभाव
- सकारात्मक बनाम नकारात्मक क्षेत्रीयतावाद
- हाल के उदाहरण और केस स्टडी
- केंद्र–राज्य संबंध
- संवैधानिक तंत्र
वर्तमान संदर्भ:-
हाल की घटनाओं जैसे मणिपुर में जातीय संघर्ष, लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग, और महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा विवाद से यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय भावनाएँ पुनर्जीवित हो रही हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय, उप-राष्ट्रीयतावाद और पहचान आधारित राजनीति यह दर्शाती है कि भारतीय संघवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में क्षेत्रीयतावाद अब भी एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
समाचार की विशेषताएँ:-
- जातीय और भाषाई आंदोलन (जैसे गोरखालैंड, बोडोलैंड)
- जातीय क्षेत्रों में स्वायत्तता की मांग (जैसे लद्दाख में छठी अनुसूची)
- गठबंधन राजनीति में क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक अभिव्यक्ति
- राज्यों के बीच सामाजिक–आर्थिक असमानता से उपजी मांगें
- सांस्कृतिक गौरव और संरक्षण (जैसे तमिल, असमिया, पंजाबी पहचान)
- क्षेत्रीय संरक्षण हेतु अनुच्छेद 371 का उपयोग
व्याख्या:-
प्र.1. क्षेत्रीयतावाद क्या है और यह राष्ट्रवाद से कैसे भिन्न है?
- क्षेत्रीयतावाद किसी विशेष क्षेत्र के प्रति उस समय वरीयता या निष्ठा है जब वह पूरे राष्ट्र की अपेक्षा अधिक महत्त्व पा लेता है। यह अक्सर सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक या आर्थिक दावों के माध्यम से प्रकट होता है।
- दूसरी ओर, राष्ट्रवाद का केंद्र राष्ट्र-राज्य की एकता और निष्ठा है। जहाँ राष्ट्रवाद एकीकृत करता है, वहीं अनियंत्रित क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है।
- फिर भी, क्षेत्रीयतावाद स्वभावतः नकारात्मक नहीं है; यह विकेंद्रीकरण और संघीय ढांचे की मजबूती में योगदान दे सकता है यदि यह संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहे।
प्र.2. भारत में क्षेत्रीयतावाद के प्रमुख कारण क्या हैं?
मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
- भाषाई विविधता (जैसे द्रविड़ आंदोलन)
- क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता (जैसे विदर्भ)
- ऐतिहासिक उपेक्षा और अविकास
- जातीय और सांस्कृतिक पहचान (जैसे पूर्वोत्तर भारत)
- वोट बैंक की राजनीति
- प्रशासनिक केन्द्रीकरण, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में उपेक्षा और असंतोष का भाव
ये सभी कारक क्षेत्रीय वंचना की भावना उत्पन्न करते हैं और स्वायत्तता या मान्यता की आकांक्षा को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
प्र.3. भारतीय संविधान क्षेत्रीय आकांक्षाओं को कैसे संबोधित करता है?
संविधान ने एकता और विविधता के बीच संतुलन बनाने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:
- संघीय संरचना, जिसमें एकात्मक पक्ष का झुकाव है
- कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 371)
- जातीय क्षेत्रों के लिए छठी अनुसूची
- पंचायती राज में विकेंद्रीकरण
- कई भाषाओं की संवैधानिक मान्यता (आठवीं अनुसूची)
ये प्रावधान विभिन्न क्षेत्रीय पहचानों को स्थान देते हुए राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखते हैं।
प्र.4. भारत में क्षेत्रीयतावाद के प्रकार कौन-कौन से हैं?
क्षेत्रीयतावाद के प्रकार इस प्रकार हैं:
- राज्य गठन की मांग (जैसे तेलंगाना, गोरखालैंड)
- स्वायत्तता की मांग (जैसे नागालैंड – अनुच्छेद 371A)
- अलगाववादी प्रवृत्तियाँ (जैसे खालिस्तान, नागा विद्रोह)
- अंतर्राज्यीय विवाद (जैसे कावेरी जल विवाद)
- क्षेत्रीय राजनीतिक वर्चस्व (जैसे तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियाँ)
हर प्रकार अलग-अलग स्तर की क्षेत्रीय भावना को दर्शाता है।
प्र.5. भारत के लिए क्षेत्रीयतावाद कैसे चुनौती और शक्ति दोनों हो सकता है?
- चुनौती के रूप में:-
- यह अलगाववादी आंदोलनों, जातीय हिंसा और अंतर्राज्यीय विवादों को जन्म दे सकता है, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण प्रभावित होता है।
- शक्ति के रूप में:-
- यह स्थानीय शासन को सशक्त करता है, अल्पसंख्यक समाजों की रक्षा करता है और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है। रचनात्मक क्षेत्रीयतावाद लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है और भारत की बहुलतावादी परंपरा को समृद्ध बना सकता है।
निष्कर्ष / आगे की राह:-
भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय अखंडता के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। सहकारी संघवाद को मजबूत करना, न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करना, उत्तरदायी शासन और सांस्कृतिक मान्यता प्रदान करना आवश्यक है। क्षेत्रीय पहचान को भारतीय राष्ट्रवाद के विरोध में नहीं बल्कि पूरक रूप में देखा जाना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाना, केन्द्रीकरण को कम करना और वास्तविक शिकायतों का समाधान संवाद व संवैधानिक उपायों के माध्यम से करना ही क्षेत्रीयतावाद को विभाजन की बजाय एकता की शक्ति में बदल सकता है।