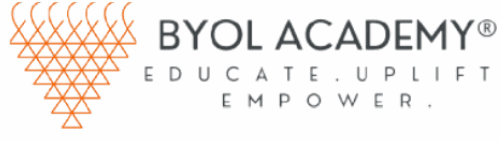छात्रों के लिए नोट्स
लेख का संदर्भ:-
प्रोजेक्ट सीबर्ड भारतीय नौसेना का एक महत्वाकांक्षी सामरिक अवसंरचना कार्यक्रम है, जो कर्नाटक के पश्चिमी तट पर कारवार स्थित आईएनएस कदंबा नौसैनिक अड्डे के विकास पर केंद्रित है। 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद शुरू हुई इस परियोजना को 1980 के दशक के अंत में औपचारिक स्वीकृति मिली। यह परियोजना मुंबई बंदरगाह पर भीड़भाड़ और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने तथा पश्चिमी नौसैनिक बेड़े के लिए उच्च क्षमता वाले केंद्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी।
UPSC जीएस पेपर से संबंधित विषय:-
- जीएस पेपर III – सुरक्षा संबंधी मुद्दे, विशेषकर अवसंरचना विकास, सामरिक क्षमता विस्तार, समुद्री सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़े पहलू।
लेख के आयाम:-
- ऐतिहासिक उत्पत्ति और सामरिक औचित्य
- चरणबद्ध विकास योजना (चरण I, चरण II-A, चरण II-B)
- वर्तमान स्थिति और हाल की उद्घाटन गतिविधियाँ
- मुख्य विशेषताएँ और इंजीनियरिंग उपलब्धियाँ
- हिन्द-प्रशांत संदर्भ में सामरिक महत्व
- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
- भविष्य की रूपरेखा
वर्तमान संदर्भ:-
अप्रैल 2025 में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारवार नौसैनिक अड्डे पर चरण II-A के तहत 2,000 करोड़ रुपये की अवसंरचना का उद्घाटन किया। इसमें नए घाट, आवासीय टॉवर और लॉजिस्टिक सुविधाएँ शामिल हैं, जो 32 युद्धपोतों, पनडुब्बियों और यार्डक्राफ्ट को सहयोग प्रदान कर सकती हैं ([ADU – Aviation Defence Universe][2], [The Economic Times][3])।
- चरण I (2005 तक चालू, 2011 में पूर्ण) – इसमें 10 जहाजों की क्षमता, ब्रेकवॉटर, 10,000 टन शिप लिफ्ट, ड्राई बर्थ, मरम्मत यार्ड, अस्पताल और लगभग 1,000 कर्मियों के लिए आवास शामिल था।
- चरण II-A – इसमें 6 किमी से अधिक लंबा बर्थिंग स्पेस, 75 मीटर ऊँचा और 33,000 वर्ग मीटर का ढका हुआ ड्राई बर्थ (जहाँ एक साथ चार युद्धपोतों की मरम्मत संभव), लगभग 10,000 आवासीय इकाइयों वाला टाउनशिप और 2.7 किमी लंबा रनवे वाला द्वैध-उपयोग नौसैनिक वायु स्टेशन (2025–26 तक संचालन योग्य) शामिल है।
- चरण II-B – इसके पूरा होने पर यह अड्डा 25 किमी क्षेत्र में 50 युद्धपोत/पनडुब्बियाँ और 40 सहायक पोतों की क्षमता वाला, स्वेज नहर के पूर्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा।
समाचार की विशेषताएँ:-
उद्घाटन से स्पष्ट है कि नागरिक-सैन्य अवसंरचना का एकीकरण तेज़ी से हो रहा है – आवास, अस्पताल, वायुक्षेत्र और लॉजिस्टिक समर्थन के साथ।
- आत्मनिर्भर भारत पर जोर – 90% से अधिक सामग्री और उपकरण घरेलू स्रोतों से लिए गए। कार्यान्वयन में एलएंडटी, एईकॉम इंडिया, एसपी ग्रुप, आईटीडी सीमेंटेशन जैसी कंपनियों ने भाग लिया।
- उन्नत अवसंरचना अब INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमानवाहक पोतों को एक साथ नए घाटों पर ठहरने की सुविधा प्रदान करती है। नौसैनिक वायु स्टेशन में एक नागरिक एन्क्लेव भी होगा, जिससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क और रक्षा जरूरतें दोनों पूरी होंगी।
व्याख्यात्मक प्रश्न:-
1. प्रोजेक्ट सीबर्ड की शुरुआत क्यों हुई और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई?
- मुंबई बंदरगाह की भीड़भाड़ और पश्चिमी बेड़े के लिए सुरक्षा जोखिमों ने 1971 युद्ध के बाद नए अड्डे की आवश्यकता को जन्म दिया।
- 1980 के दशक की शुरुआत में एडमिरल ओ.एस. डॉसन ने कारवार तट पर गहरे समुद्र वाले नौसैनिक अड्डे का विचार रखा।
- 1999 में पोखरण-II परमाणु परीक्षणों के बाद इस परियोजना को औपचारिक स्वीकृति मिली। यहाँ गहरे समुद्र के प्राकृतिक लंगर स्थान, विस्तार के लिए पर्याप्त जगह और हवाई खतरों से दूरी जैसे सामरिक लाभ मौजूद थे।
2. विकास के चरण कैसे संरचित हैं और अब तक क्या उपलब्धियाँ हुई हैं?
- चरण I – बुनियादी बंदरगाह अवसंरचना (ब्रेकवॉटर, डॉकिंग पियर, ड्राई बर्थ, मरम्मत यार्ड, अस्पताल, आवास) पूरी की गई।
- चरण II-A – 32 युद्धपोतों और 23 यार्डक्राफ्ट के लिए बर्थिंग, चार युद्धपोतों के लिए ढका हुआ ड्राई बर्थ, 10,000 लोगों के लिए आवासीय टाउनशिप, द्वैध-उपयोग नौसैनिक वायु स्टेशन।
- चरण II-B – 50 युद्धपोत/पनडुब्बियाँ और 40 सहायक पोतों की क्षमता वाला 25 किमी का अड्डा।
3. भारत की समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में यह अड्डा कौन-से सामरिक लाभ प्रदान करता है?
- कारवार अड्डा भारत को अरब सागर और हिंद महासागर की महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी और सुरक्षा में सक्षम बनाता है।
- मुंबई पर निर्भरता कम होती है और विमानवाहक पोतों का एक साथ संचालन संभव होता है। उन्नत मरम्मत और रखरखाव सुविधाओं से जहाजों का डाउनटाइम कम होता है।
- नौसैनिक वायु स्टेशन समुद्री अभियानों को हवाई सहयोग देगा। यह चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति का संतुलन बनाने और हिन्द-प्रशांत रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
4. सीबर्ड से जुड़े नागरिक-सैन्य और आर्थिक आयाम क्या हैं?
- यह परियोजना आवासीय टाउनशिप, अस्पताल और नागरिक सुविधाओं को नौसैनिक संपत्तियों के साथ जोड़ती है। 90% से अधिक सामग्री स्वदेशी है। एलएंडटी, एसपी ग्रुप जैसी कंपनियाँ प्रमुख ठेकेदार हैं।
- 7,000 प्रत्यक्ष और 20,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में भविष्य में कनेक्टिविटी, पर्यटन और लॉजिस्टिक क्षेत्र से आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।
5. प्रमुख इंजीनियरिंग और पर्यावरणीय चुनौतियाँ क्या थीं?
- पहाड़ी तटीय भूभाग और पुनः प्राप्त समुद्री क्षेत्र पर निर्माण एक बड़ी तकनीकी चुनौती थी। बिनागा खाड़ी में व्यापक ड्रेजिंग और चट्टानों को तोड़कर 5 किमी से अधिक लंबे ब्रेकवॉटर का निर्माण हुआ।
- 75 मीटर ऊँचा और 33,000 वर्ग मीटर का ढका हुआ ड्राई बर्थ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि है। पर्यावरण मंत्रालय और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की दिशानिर्देशों को शामिल कर पारिस्थितिक प्रभाव कम करने का प्रयास किया गया, विशेषकर संवेदनशील तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान में रखते हुए।
निष्कर्ष:-
प्रोजेक्ट सीबर्ड भारत की नौसैनिक अवसंरचना में एक क्रांतिकारी छलांग है। इसने कारवार में पश्चिमी बेड़े की क्षमता को मजबूत किया है, मुंबई पर अधिक निर्भरता को घटाया है और हिन्द-प्रशांत रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं से सामंजस्य स्थापित किया है। चरण II-B के बाद यह अड्डा 50 युद्धपोत/पनडुब्बियों, एक नौसैनिक वायु स्टेशन और पूर्ण विकसित टाउनशिप का घर होगा। यह परियोजना सैन्य तैयारी, स्वदेशी औद्योगिक क्षमता, नागरिक सुविधाओं और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करती है। बढ़ती समुद्री प्रतिस्पर्धा के इस दौर में, कारवार का यह आधुनिक अड्डा आने वाले दशकों तक भारत की नौसैनिक स्थिति का केंद्रीय स्तंभ रहेगा।