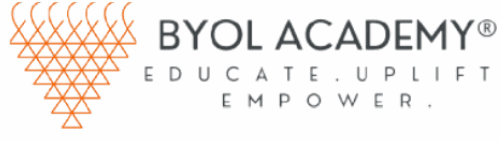छात्रों के लिए नोट्स
लेख का संदर्भ:-
यह लेख भारत की तटीय सुरक्षा योजना (Coastal Security Scheme – CSS) की जटिलताओं पर केंद्रित है, जो समुद्री सीमाओं की निगरानी और देश की विशाल तटरेखा की सुरक्षा को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें योजना के मूलभूत उद्देश्यों, उसके प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही प्रमुख चुनौतियों तथा एक मजबूत व उत्तरदायी तटीय सुरक्षा ढाँचा तैयार करने के उपायों पर चर्चा की गई है। लेख इस तथ्य को रेखांकित करता है कि समुद्री खतरों की प्रकृति बहुआयामी है और विभिन्न एजेंसियों के बीच सहज समन्वय स्थापित करना अत्यंत जटिल कार्य है।
UPSC जीएस पेपर विषय:-
- यह विषय UPSC जीएस पेपर-III:–
- आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित है। विशेष रूप से निम्न उप-विषयों के अंतर्गत प्रासंगिक है:
- सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन।
- विभिन्न सुरक्षा बलों और एजेंसियों की भूमिका एवं उनके दायित्व।
- तटीय सुरक्षा, विशेषकर समुद्र से आने वाले खतरों की संवेदनशीलता और उन्हें रोकने के उपाय।
- आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित है। विशेष रूप से निम्न उप-विषयों के अंतर्गत प्रासंगिक है:
लेख के आयाम:-
इस लेख में निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है:
- संरचनात्मक और अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ: तटीय पुलिस थानों, गश्ती नौकाओं और जेट्टी की कमी।
- मानव संसाधन और प्रशिक्षण की समस्याएँ: पुलिसकर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और विशेष कौशल की कमी।
- एजेंसियों के बीच समन्वय की समस्या: नौसेना, तटरक्षक बल, मरीन पुलिस और अन्य राज्य एजेंसियों के बीच संचार व आदेश संरचना में अस्पष्टता।
- प्रौद्योगिकीगत सीमाएँ: उन्नत निगरानी प्रणालियों की आवश्यकता और विभिन्न तकनीकी प्लेटफ़ॉर्मों का एकीकरण न होना।
- गैर-पारंपरिक खतरे: आतंकवाद, तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और मानव तस्करी जैसे नए खतरे।
वर्तमान संदर्भ:-
2008 के मुंबई आतंकी हमलों ने भारत की समुद्री सीमाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया। इसके बाद तटीय सुरक्षा योजना (CSS) की शुरुआत हुई, ताकि उथले तटीय क्षेत्रों की निगरानी के लिए एक समर्पित बल उपलब्ध कराया जा सके, जो प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य कर सके। हालाँकि, हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा की गई समीक्षाओं में यह सामने आया है कि कई गश्ती नौकाएँ चालू स्थिति में नहीं हैं और विभिन्न तटीय राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पर्याप्त मानवबल की कमी है। इस कारण, इस योजना के कार्यान्वयन और समुद्री निगरानी से जुड़ी चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।
समाचार की विशेषताएँ
भारत के तटीय सुरक्षा ढाँचे में चुनौतियों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- अपर्याप्त अवसंरचना:-
- तटीय पुलिस स्टेशनों, चौकियों और जेट्टी के निर्माण की धीमी गति सबसे बड़ी बाधा है। कई गश्ती नौकाएँ रखरखाव निधि के अभाव में काम नहीं कर पा रही हैं।
- मानव संसाधन की कमी:-
- कई राज्यों में स्वीकृत पद रिक्त हैं। कई जगह बाहरी या प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर निर्भरता है, जिनमें विशेष प्रशिक्षण और प्रेरणा का अभाव होता है।
- कमज़ोर अंतर-एजेंसी समन्वय:-
- नौसेना, तटरक्षक बल, मरीन पुलिस और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संचार व खुफिया साझाकरण अक्सर असंगठित होता है। इससे परिचालन में ऐसे अंतर रह जाते हैं जिनका दुरुपयोग असामाजिक तत्व कर सकते हैं।
- तकनीकी कमियाँ:-
- तटीय निगरानी नेटवर्क (CSN) जैसी प्रणालियाँ मौजूद हैं, लेकिन विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपने प्लेटफ़ॉर्मों का एकीकृत न कर पाने से एक समग्र समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) नहीं बन पाती।
व्याख्या:-
भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस के बीच अंतर coastal security के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- इन तीनों बलों के बीच अंतर भारत के स्तरीय तटीय सुरक्षा मॉडल का मूल है।
- भारतीय नौसेना: गहरे समुद्र की रक्षा और सामरिक युद्ध संचालन की जिम्मेदारी।
- भारतीय तटरक्षक बल: प्रादेशिक जल एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव कार्य।
- मरीन पुलिस: तटवर्ती, उथले जल क्षेत्रों की सुरक्षा और निगरानी।
यह स्तरीय व्यवस्था परस्पर पूरक है, किंतु उनके अधिकार क्षेत्रों के टकराने और खुफिया साझाकरण व संयुक्त अभियानों की स्पष्ट श्रृंखला न होने पर गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- गैर-पारंपरिक खतरे समुद्री सीमा निगरानी को कैसे जटिल बनाते हैं?
- समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ना, मानव और नशीली दवाओं की तस्करी जैसे खतरे पारंपरिक सैन्य रणनीतियों से भिन्न होते हैं।
- ये प्रायः छोटे, पंजीकरणरहित नौकाओं से होते हैं जिन्हें ट्रैक करना कठिन होता है।
- विस्तृत व छिद्रपूर्ण तटरेखा तथा द्वीपों का उपयोग गुप्त गतिविधियों के लिए किया जाता है।
- ये कार्य अक्सर संगठित आपराधिक नेटवर्क से जुड़े होते हैं।
इनसे निपटने के लिए मजबूत निगरानी, खुफिया-आधारित अभियान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। लेकिन रीयल-टाइम खुफिया व एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव इन्हें रोकना कठिन बनाता है।
समुद्री निगरानी में प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभाती है?
प्रौद्योगिकी तटीय निगरानी में गेम-चेंजर साबित हो रही है।
- CSN: राडार, कैमरे और सेंसरों की श्रृंखला से जहाज़ों की गतिविधियों पर नज़र रखता है।
- NC3I नेटवर्क: सभी स्रोतों से डेटा एकीकृत कर एकीकृत समुद्री चित्र प्रस्तुत करता है।
- AIS, उपग्रह चित्रण और UAVs: समुद्री डोमेन जागरूकता को और बेहतर बनाते हैं।
- लेकिन इनका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब सभी एजेंसियों के बीच रीयल-टाइम डेटा साझाकरण का सुगम तंत्र बने।
- तटीय सुरक्षा ढाँचे में मछुआरा समुदाय को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है?
- मछुआरा समुदाय को तटीय सुरक्षा की “आँख और कान” कहा जाता है।
- उनका रोज़ाना तटीय जल में रहना और स्थानीय समुद्री पर्यावरण का गहरा ज्ञान उन्हें खुफिया जुटाने में सहायक बनाता है।
- वे संदिग्ध गतिविधियों को सबसे पहले देख पाते हैं।
- इन्हें पहचान पत्र और संचार उपकरण देने से वे अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाते हैं और प्रशासन को शीघ्र सूचना भी दे सकते हैं।
इसलिए एक मज़बूत तटीय सुरक्षा रणनीति में इनके साथ सतत जुड़ाव और विश्वास निर्माण आवश्यक है।
निष्कर्ष:-
हालाँकि तटीय सुरक्षा योजना (CSS) ने एक मज़बूत सुरक्षा ढाँचे की नींव रखी है, लेकिन कई चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। भारत को वास्तव में अभेद्य समुद्री रक्षा तंत्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
- अवसंरचना और मानवबल की कमी को शीघ्र पूरा करना।
- तटीय पुलिस थानों का निर्माण और प्रशिक्षित मरीन पुलिस की भर्ती को तेज़ करना।
- एकीकृत कमान संरचना तथा साझा खुफिया मंच की स्थापना।
- उन्नत तकनीकों को अपनाकर उन्हें सभी एजेंसियों में सहज एकीकृत करना।
- स्थानीय समुदायों, विशेषकर मछुआरों को सशक्त बनाना।
इन कदमों से भारत एक बहुस्तरीय, सहयोगात्मक और लचीला तटीय सुरक्षा ढाँचा तैयार कर सकेगा, जो भविष्य के सभी खतरों का प्रभावी ढंग से सामना कर पाएगा।