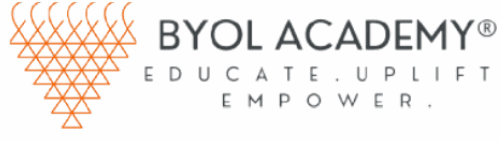छात्रों के लिए नोट्स
लेख की पृष्ठभूमि:-
यह लेख भारत के व्यापक तटीय और समुद्री सुरक्षा दृष्टिकोण की पड़ताल करता है, जिसमें समुद्र से उत्पन्न होने वाले विभिन्न खतरों से निपटने के लिए बहु-स्तरीय रक्षा तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल को परखने, एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने और समग्र प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार के लिए नियमित, बड़े पैमाने पर अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
UPSC जीएस पेपर विषय:-
- यह विषय UPSC GS पेपर-III:-
- आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित उप-विषय शामिल हैं:
- सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन।
- संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।
- विभिन्न सुरक्षा बलों और एजेंसियों की भूमिका एवं उनके कार्यक्षेत्र।
- तटीय सुरक्षा, विशेष रूप से भारत की विशाल तटरेखा पर फोकस।
- आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित उप-विषय शामिल हैं:
लेख के आयाम:-
लेख निम्नलिखित बिंदुओं को समेटता है:
- भारत के लिए तटीय सुरक्षा का सामरिक महत्व।
- तटीय सुरक्षा के खतरे: आतंकवाद, तस्करी, अवैध मछली पकड़ना और समुद्री डकैती।
- भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस तथा अन्य केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों के बीच समन्वय।
- तटरेखा की निगरानी हेतु तकनीकी उन्नति और निगरानी प्रणालियाँ।
- तटीय समुदायों, विशेषकर मछुआरों की भागीदारी, जो सुरक्षा ढाँचे की “आँख और कान” माने जाते हैं।
वर्तमान संदर्भ:-
2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद से भारत में तटीय सुरक्षा एक उच्च-प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया है, क्योंकि आतंकवादियों ने देश में घुसपैठ के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया था। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने समुद्री रक्षा को सुदृढ़ करने के अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास जैसे सी विजिल (Sea Vigil) इसी बढ़ते फोकस का परिणाम हैं। ये अभ्यास संपूर्ण तटीय सुरक्षा ढाँचे की प्रभावशीलता परखने और सभी एजेंसियों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखने का अहम साधन हैं।
समाचार की मुख्य विशेषताएँ:-
राष्ट्रव्यापी तटीय सुरक्षा अभ्यास जैसे सी विजिल की प्रमुख विशेषताएँ:
- पैन-इंडिया दायरा:-
- इसमें भारत की संपूर्ण 11,098 किमी लंबी तटरेखा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) शामिल होते हैं।
- बहु-एजेंसी भागीदारी:-
- इसमें 13 तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, छह केंद्रीय मंत्रालयों और 21 से अधिक केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों के संसाधन और कार्मिक शामिल होते हैं।
- दो-स्तरीय दृष्टिकोण:-
- पहले चरण में तटीय सुरक्षा उपायों का व्यापक ऑडिट किया जाता है। दूसरे चरण में समुद्र से असममित खतरे का सिमुलेशन करते हुए सामरिक अभ्यास किया जाता है।
- व्यापक ऑडिट:-
- इसमें बंदरगाहों, तेल रिग, परमाणु प्रतिष्ठानों और मछली उतारने के केंद्रों जैसी महत्वपूर्ण तटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा जाँच शामिल होती है।
- सभी हितधारकों का एकीकरण:-
- शीर्ष स्तर पर नौसेना और कोस्ट गार्ड से लेकर जमीनी स्तर पर मछुआरों तक, सभी को इस अभ्यास में शामिल किया जाता है ताकि एकजुट और एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।
व्याख्या:-
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे बड़े पैमाने के तटीय सुरक्षा अभ्यास का महत्व क्या है?
- इस तरह का अभ्यास भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संपूर्ण रक्षा तंत्र की वास्तविक जाँच करता है। यह आतंकवादी घुसपैठ से लेकर तस्करी तक सभी खतरों के प्रति एजेंसियों की तैयारी परखता है।
- इसका पैमाना और जटिलता नौसेना, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस और विभिन्न सरकारी विभागों को समन्वित रूप से काम करने के लिए मजबूर करती है। यह तालमेल भारत जैसी लंबी और संवेदनशील तटरेखा वाले देश के लिए आवश्यक है।
- इसके अलावा, यह अभ्यास मौजूदा सुरक्षा ढाँचे में खामियों और कमजोरियों की पहचान करता है, जिससे तकनीक, बुनियादी ढाँचे और प्रशिक्षण में सुधार किया जा सके।
ऐसे अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना अन्य एजेंसियों के साथ किस प्रकार समन्वय करती है?
- भारतीय नौसेना, जो तटीय सुरक्षा की प्रमुख एजेंसी है, अन्य एजेंसियों के साथ केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के माध्यम से समन्वय करती है। सी विजिल जैसे अभ्यास के दौरान, नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय संपूर्ण अभियान की निगरानी करता है।
- मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में स्थापित संयुक्त संचालन केंद्र (Joint Operations Centres – JOCs) वास्तविक समय में समन्वय और सूचना साझाकरण को सक्षम बनाते हैं। इस मॉडल के तहत खुफिया जानकारी तेजी से साझा होती है और किसी भी उभरते खतरे के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया दी जा सकती है, जिससे विभिन्न सुरक्षा बलों के बीच अलगाववादी दृष्टिकोण से बचा जा सके।
इस तटीय सुरक्षा ढाँचे में मछुआरा समुदाय की क्या भूमिका है?
- मछुआरा समुदाय भारत की तटीय सुरक्षा संरचना का अभिन्न अंग है, जिसे अक्सर समुद्री बलों की “आँख और कान” कहा जाता है। उनका व्यापक प्रसार और तटीय जल का गहरा ज्ञान उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने में सक्षम बनाता है।
- इन अभ्यासों के दौरान उन्हें असामान्य नौका गतिविधियों या व्यवहार की पहचान कर अधिकारियों को सूचित करने के लिए जागरूक किया जाता है। सरकार ने उन्हें ट्रांसपोंडर और पहचान पत्र उपलब्ध कराने की पहल की है ताकि उनकी पहचान आसानी से की जा सके और उन्हें सुरक्षा तंत्र में जोड़ा जा सके।
- यह सामुदायिक सहभागिता विश्वास पैदा करती है और एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देती है, जिससे सुरक्षा ढाँचा अधिक मजबूत और प्रभावी बनता है।
निष्कर्ष / आगे की राह:
सी विजिल जैसे राष्ट्रव्यापी तटीय सुरक्षा अभ्यास भारत की अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। इन अभ्यासों ने प्रतिक्रिया क्षमता और एजेंसियों के बीच समन्वय को काफी हद तक मजबूत किया है, फिर भी सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। आगे की राह में क्षमताओं का निरंतर निर्माण शामिल है, जैसे:
उन्नत निगरानी तकनीक (मानवरहित अंडरवॉटर वाहन, सैटेलाइट-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम) का अधिग्रहण।
मरीन पुलिस की संख्या और प्रशिक्षण को मजबूत करना, तथा उन्हें नौसेना और कोस्ट गार्ड के साथ सहज रूप से एकीकृत करना।
तटीय समुदायों तक निरंतर पहुँच और मछुआरों की भूमिका को औपचारिक रूप से सुरक्षा ढाँचे में सम्मिलित करना।
इस प्रकार, एक समग्र और लचीली तटीय रक्षा प्रणाली विकसित की जा सकती है।