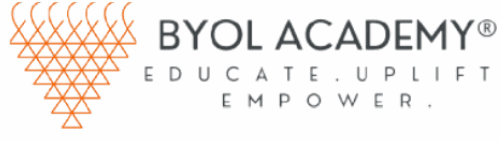(चार एंग्लो-मैसूर युद्ध: हैदर अली, टीपू सुल्तान, तीन एंग्लो-मराठा युद्ध: मराठा संघ का पतन, एंग्लो-सिख युद्ध: रणजीत सिंह, डलहौजी और अधिग्रहण, विस्तार में सैन्य सुधार और कूटनीति की भूमिका, उपनिवेशीय संधि बनाम प्रतिरोध आंदोलन)
| एंग्लो-भारतीय युद्ध भारत के औपनिवेशिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये संघर्ष न केवल ब्रिटिश सैन्य विस्तार को दर्शाते हैं बल्कि स्थानीय प्रतिरोध, कूटनीति, और राजनीतिक रणनीतियों को भी उजागर करते हैं। एंग्लो-मैसूर, एंग्लो-मराठा, और एंग्लो-सिख युद्धों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सैन्य सुधार और कूटनीतिक नीतियों जैसे उपनिवेशीय संधि पर विशेष बल दिया गया है। |
I. एंग्लो-मैसूर युद्ध (1767-1799): प्रतिरोध का उत्थान और पतन
एंग्लो-मैसूर युद्ध चार युद्धों की श्रृंखला थे जो मैसूर राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए, जिनमें हैदर अली और टीपू सुल्तान प्रमुख नेता थे।
- पहला एंग्लो-मैसूर युद्ध (1767-1769): हैदर अली की रणनीतिक कुशलता से शुरुआती जीत हुई, जिससे मैड्रास संधि हुई, जो कब्ज़ाए गए क्षेत्रों को वापस करने वाली थी।
- दूसरा एंग्लो-मैसूर युद्ध (1780-1784): ब्रिटिश धोखे के जवाब में तीव्र प्रतिक्रिया। टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर सैन्य कौशल दिखाया। यह युद्ध मंगलौर संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसने मैसूर की मजबूती को स्वीकार किया।
- तीसरा एंग्लो-मैसूर युद्ध (1790-1792): टीपू सुल्तान को ब्रिटिश, मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के गठबंधन का सामना करना पड़ा। उसे सेरिंगापट्टम संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें मैसूर का आधा हिस्सा देना पड़ा।
- चौथा एंग्लो-मैसूर युद्ध (1799): टीपू सुल्तान की त्रासदीपूर्ण मृत्यु का युद्ध, सिरीरंगपट्टन की लड़ाई में ब्रिटिश विजयी हुए, जिससे मैसूर का अधीनता और राजनीतिक पुनर्गठन हुआ।
महत्त्व: युद्ध टीपू के फ्रांसीसी और ऑटोमन से कूटनीतिक संपर्क, उसकी सैन्य नवाचार, और संप्रभुता की रक्षा में उसकी शहादत को दर्शाते हैं।
II. एंग्लो-मराठा युद्ध (1775-1818): मराठा संघ का विघटन
तीन एंग्लो-मराठा युद्ध मराठा शक्ति संरचना के व्यवस्थित कमजोर होने और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के उदय को दिखाते हैं।
- पहला एंग्लो-मराठा युद्ध (1775-1782): पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार विवाद से उत्पन्न। सल्बाई संधि ने माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में मान्यता दी, जिससे अस्थायी शांति बनी।
- दूसरा एंग्लो-मराठा युद्ध (1803-1805): मराठा सरदारों के बीच आंतरिक कलह के कारण। ब्रिटिशों ने सिंधिया और भोंसले को हराया, दिल्ली जैसे प्रमुख क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया।
- तीसरा एंग्लो-मराठा युद्ध (1817-1818): मराठा संघ का अंत। पेशवा बाजी राव द्वितीय को पराजित कर निर्वासित किया गया, जिससे विशाल क्षेत्रों का अधिग्रहण हुआ।
प्रभाव: ये युद्ध भारत की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक को नष्ट करने और ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ाने में निर्णायक थे।
III. एंग्लो-सिख युद्ध (1845-1849): रणजीत सिंह से अधिग्रहण तक
सिख साम्राज्य, महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में मजबूत था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अस्थिरता उत्पन्न हुई।
- पहला एंग्लो-सिख युद्ध (1845-1846): सिख सेना की बहादुरी के बावजूद खराब नेतृत्व के कारण हार। लाहौर संधि कठोर शर्तें थोपती है।
- दूसरा एंग्लो-सिख युद्ध (1848-1849): मुल्तान में विद्रोह से प्रेरित। ब्रिटिश विजय से पंजाब का पूर्ण अधिग्रहण हुआ।
डलहौजी की भूमिका: उनकी आक्रामक डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स और युद्ध के बाद सीधी अधिग्रहण नीति ने नॉर्थवेस्ट फ्रंटियर पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया।
IV. औपनिवेशिक विस्तार में सैन्य सुधार और कूटनीति
ब्रिटिशों ने भारतीय राज्यों को वश में करने के लिए सैन्य सुधार और कूटनीतिक चालों का संयोजन किया।
- सैन्य सुधार: आधुनिक तोपखाना, व्यवस्थित बटालियन, और यूरोपीय शैली का प्रशिक्षण ब्रिटिशों को रणनीतिक बढ़त देता था।
- कूटनीतिक उपकरण: भारतीय शक्तियों को विभाजित करने के लिए गठबंधन, समझौते और संधियों का इस्तेमाल, जैसे बासेन संधि (1802), जिसने मराठा नेताओं को अलग किया।
V. उपनिवेशीय संधि बनाम प्रतिरोध आंदोलन
- उपनिवेशीय संधि: लॉर्ड वेल्सली द्वारा शुरू की गई, इस नीति ने भारतीय शासकों को अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सैनिकों को रखने के लिए मजबूर किया, जिसका खर्च भारतीयों को वहन करना पड़ता था, जिससे संप्रभुता कमज़ोर हुई।
- प्रतिरोध आंदोलन: इन नीतियों के बावजूद, टीपू सुल्तान, मराठा, और सिख सेनापतियों जैसे रणजोध सिंह मजीठिया ने दृढ़ प्रतिरोध दिखाया।
- तुलना: जबकि उपनिवेशीय संधि ने समझौतों के माध्यम से साम्राज्यवाद को छुपाया, प्रतिरोध आंदोलन स्वायत्तता और राष्ट्रीय गर्व के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं।
निष्कर्ष
अंग्रेज़-भारतीय युद्धों को समझना केवल घटनाओं के कालक्रम से अधिक है; यह ब्रिटिशों द्वारा भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करने और विस्तार करने के लिए अपनाई गई जटिल रणनीतियों को भी उजागर करता है। ये युद्ध सैन्य नवाचार, कूटनीतिक चालबाज़ी और स्थानीय प्रतिरोध के बीच के संवाद को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि कैसे ब्रिटिशों ने शक्तिशाली भारतीय राज्यों को कमजोर करने के लिए बल और राजनीतिक गठबंधनों दोनों का उपयोग किया। यह संघर्ष उन भारतीय शासकों की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को भी रेखांकित करता है जिन्होंने औपनिवेशिक प्रभुत्व का विरोध किया। इन युद्धों का अध्ययन औपनिवेशिक विस्तार की प्रकृति और इसके भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव की हमारी समझ को गहरा करता है। यह ज्ञान औपनिवेशिक इतिहास में साम्राज्यवाद, प्रतिरोध और शासन कला के व्यापक विषयों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
| UPSC मेन्स के लिए कारण-परिणाम संबंधों, प्रमुख व्यक्तित्वों की भूमिका, और प्रतिरोध बनाम कूटनीति के तुलनात्मक अध्ययन पर ध्यान दें। प्रिलिम्स के लिए संधियाँ, तिथियाँ, और प्रमुख युद्ध याद रखें। यह ज्ञान इतिहास, राजनीति, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जोड़ता है, जो सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए बहुविषयक लाभकारी है। |
MCQ
- पहला एंग्लो-मैसूर युद्ध (1767-1769) किस संधि से समाप्त हुआ?
A) सेरिंगापट्टम संधि
B) मैड्रास संधि
C) मंगलौर संधि
D) सल्बाई संधि
उत्तर: B) मैड्रास संधि
व्याख्या: पहला एंग्लो-मैसूर युद्ध मैड्रास संधि से समाप्त हुआ, जिसने कब्ज़ाए गए क्षेत्रों को पुनःस्थापित किया। - सेरिंगापट्टम संधि (1792) किस एंग्लो-मैसूर युद्ध के बाद हुई?
A) पहला
B) दूसरा
C) तीसरा
D) चौथा
उत्तर: C) तीसरा
व्याख्या: तीसरे एंग्लो-मैसूर युद्ध के बाद सेरिंगापट्टम संधि हुई, जिसके तहत टीपू सुल्तान ने आधा क्षेत्र सौंपा। - चौथे एंग्लो-मैसूर युद्ध (1799) के समय मैसूर का शासक कौन था?
A) हैदर अली
B) टीपू सुल्तान
C) पेशवा माधवराव प्रथम
D) रणजीत सिंह
उत्तर: B) टीपू सुल्तान
व्याख्या: टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो-मैसूर युद्ध के समय शासक थे और सिरीरंगपट्टन के युद्ध में मारे गए। - निम्न में से कौन पहला एंग्लो-मराठा युद्ध (1775-1782) का कारण नहीं था?
A) पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार विवाद
B) दक्खन में ब्रिटिश विस्तार की इच्छा
C) बासेन संधि
D) ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध मराठा प्रतिरोध
उत्तर: C) बासेन संधि
व्याख्या: बासेन संधि दूसरी एंग्लो-मराठा युद्ध (1802) के दौरान हुई थी, पहले युद्ध के दौरान नहीं। - दावा (A): सल्बाई संधि (1782) ने ब्रिटिश और मराठाओं के बीच अस्थायी शांति स्थापित की।
कारण (R): इसने माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में मान्यता दी।
A) दोनों A और R सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
B) दोनों A और R सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता।
C) A सही है लेकिन R गलत है।
D) A गलत है लेकिन R सही है।
उत्तर: A) दोनों A और R सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
व्याख्या: सल्बाई संधि ने उत्तराधिकार विवाद को सुलझाया और माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में स्थापित किया, जिससे अस्थायी शांति बनी। - दूसरे एंग्लो-मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिशों ने कौन-कौन से क्षेत्र अपने कब्जे में लिए?
A) मैसूर
B) पंजाब
C) दिल्ली
D) बंगाल
उत्तर: C) दिल्ली
व्याख्या: ब्रिटिशों ने सिंधिया और भोंसले को हराने के बाद दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने अधीन किया। - तीसरे एंग्लो-मराठा युद्ध (1817-1818) का परिणाम क्या रहा?
A) मराठा शक्ति की पुनर्स्थापना
B) ब्रिटिश प्रभाव में कमी
C) मराठा संघ का अंत
D) लाहौर संधि
उत्तर: C) मराठा संघ का अंत
व्याख्या: तीसरे एंग्लो-मराठा युद्ध ने मराठा संघ का अंत किया और ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार किया। - एंग्लो-सिख युद्धों से पहले सिख साम्राज्य को किस सिख शासक ने एकीकृत किया था?
A) डलहौजी
B) रणजीत सिंह
C) रणजोध सिंह मजीठिया
D) हरी सिंह नलवा
उत्तर: B) रणजीत सिंह
व्याख्या: महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य को एकीकृत किया, जिसके बाद उनकी मृत्यु से अस्थिरता आई और युद्ध हुए। - पहला एंग्लो-सिख युद्ध (1845-1846) किस संधि के साथ समाप्त हुआ?
A) अमृतसर संधि
B) लाहौर संधि
C) मंगलौर संधि
D) सल्बाई संधि
उत्तर: B) लाहौर संधि
व्याख्या: पहला एंग्लो-सिख युद्ध लाहौर संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसने सिख साम्राज्य पर कठोर शर्तें थोप दीं। - लॉर्ड वेल्सली द्वारा शुरू की गई कौन सी नीति भारतीय शासकों को अपने खर्च पर ब्रिटिश सैनिकों को रखने के लिए मजबूर करती थी?
A) डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स
B) उपनिवेशीय संधि
C) स्थायी व्यवस्था
D) रायटवारी प्रणाली
उत्तर: B) उपनिवेशीय संधि
व्याख्या: उपनिवेशीय संधि ने शासकों को ब्रिटिश सैनिकों को अपने खर्च पर रखने के लिए मजबूर किया, जिससे उनकी संप्रभुता कम हुई। - दावा (A): टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों का विरोध करने के लिए फ्रांसीसी और ऑटोमन समर्थन माँगा।
कारण (R): टीपू सुल्तान के सैन्य सुधार यूरोपीय युद्धकला से प्रभावित थे।
A) दोनों A और R सही हैं और R, A को समझाता है।
B) दोनों A और R सही हैं लेकिन R, A को समझाता नहीं।
C) A सही है लेकिन R गलत है।
D) दोनों A और R गलत हैं।
उत्तर: B) दोनों A और R सही हैं लेकिन R, A को समझाता नहीं।
व्याख्या: टीपू ने बाहरी गठबंधन की मांग की और अपने सैन्य सुधार भी किए, लेकिन सैन्य सुधार सीधे कूटनीतिक संपर्क को नहीं समझाते। - निम्न युद्ध और उसके परिणाम में सही मिलान कौन सा है?
A) दूसरा एंग्लो-मैसूर युद्ध – मैड्रास संधि
B) पहला एंग्लो-मराठा युद्ध – सल्बाई संधि
C) पहला एंग्लो-सिख युद्ध – मंगलौर संधि
D) चौथा एंग्लो-मैसूर युद्ध – लाहौर संधि
उत्तर: B) पहला एंग्लो-मराठा युद्ध – सल्बाई संधि
व्याख्या: सल्बाई संधि ने पहला एंग्लो-मराठा युद्ध समाप्त किया। - डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स मुख्यतः किसके समय लागू की गई?
A) लॉर्ड वेल्सली
B) लॉर्ड डलहौजी
C) लॉर्ड कॉर्नवालिस
D) लॉर्ड हेस्टिंग्स
उत्तर: B) लॉर्ड डलहौजी
व्याख्या: डलहौजी ने बिना वारिस वाले राज्यों को अपने अधीन करने के लिए डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स का उपयोग किया। - निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य सुधार ब्रिटिशों को एंग्लो-भारतीय युद्धों में बढ़त देता था?
A) केवल सिपाही रेजिमेंट की शुरुआत
B) यूरोपीय शैली के तोपखाने और प्रशिक्षण को अपनाना
C) भारतीय शासकों की गुरिल्ला रणनीतियों का उपयोग
D) केवल भारतीय घुड़सवारों पर निर्भर रहना
उत्तर: B) यूरोपीय शैली के तोपखाने और प्रशिक्षण को अपनाना
व्याख्या: ब्रिटिशों ने आधुनिक तोपखाना और यूरोपीय प्रशिक्षण विधियों को अपनाकर अपनी युद्धक क्षमता बढ़ाई। - दावा (A): उपनिवेशीय संधि भारतीय राज्यों के बीच गठबंधन रोकने का एक कूटनीतिक उपकरण था।
कारण (R): यह भारतीय शासकों को पूर्ण संप्रभुता और अपनी सेनाओं के नियंत्रण की अनुमति देता था।
A) दोनों A और R सही हैं और R, A को समझाता है।
B) दोनों A और R सही हैं लेकिन R, A को समझाता नहीं।
C) A सही है लेकिन R गलत है।
D) दोनों A और R गलत हैं।
उत्तर: C) A सही है लेकिन R गलत है।
व्याख्या: उपनिवेशीय संधि भारतीय राज्यों के गठबंधनों को रोकती थी, लेकिन शासकों की संप्रभुता और सेना नियंत्रण को सीमित करती थी।