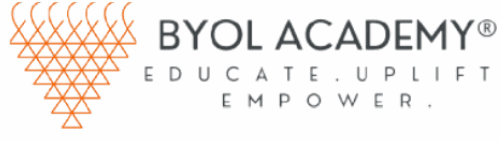वेवेल योजना (1945) और शिमला सम्मेलन की विफलता
परिचय
1945 में लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तावित वेवेल योजना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में राजनीतिक गतिरोध को हल करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। 2 इसका उद्देश्य एक अंतरिम सरकार बनाना था जिसमें विभिन्न राजनीतिक गुटों के भारतीय नेता शामिल हों, जिससे अंततः स्वशासन प्राप्त हो सके। हालाँकि, यह पहल शिमला सम्मेलन में समाप्त हुई, जो वांछित परिणाम देने में विफल रहा।
ऐतिहासिक संदर्भ
- द्वितीय विश्व युद्ध का अंत: 1945 में युद्ध की समाप्ति ने वैश्विक राजनीति को काफी बदल दिया, जिससे ब्रिटेन को अपनी औपनिवेशिक नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया।
- राष्ट्रवाद का उदय: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग से स्वतंत्रता की बढ़ती मांगों ने भारत में राजनीतिक सुधार की तात्कालिकता को दर्शाया।
वेवेल योजना के उद्देश्य
- एक अंतरिम सरकार की स्थापना: योजना में एक प्रतिनिधि अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव था जो एक नया संविधान स्थापित होने तक भारत का प्रबंधन कर सके।
- समावेशिता: सांप्रदायिक तनाव को दूर करने और सभी आवाज़ों को सुना जाना सुनिश्चित करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व का लक्ष्य रखा गया।
- स्वशासन के लिए ढाँचा: भारतीय नेताओं के बीच सहयोगात्मक बातचीत के माध्यम से पूर्ण स्वशासन की दिशा में संक्रमण को सुविधाजनक बनाने का इरादा था।
वेवेल योजना की मुख्य विशेषताएं
- अंतरिम सरकार की संरचना: सुझाव दिया गया कि सरकार में प्रमुख राजनीतिक दलों, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल हों।
- ब्रिटिश की भूमिका: योजना में कहा गया था कि ब्रिटिश संक्रमण के दौरान नियंत्रण बनाए रखेंगे लेकिन एक भारतीय नेतृत्व वाली सरकार की स्थापना का समर्थन करेंगे।
- संवैधानिक विकास: भारत में विविध समुदायों की आकांक्षाओं को दर्शाने वाले एक नए संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किया गया।
शिमला सम्मेलन (जून 1945)
- उद्देश्य: वेवेल योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा करने और प्रमुख भारतीय नेताओं के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए बुलाया गया।
- प्रतिभागी: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक गुटों के नेता शामिल थे।
वेवेल योजना की विफलता के कारण
- आम सहमति का अभाव: राजनीतिक दलों के बीच गहरे मतभेदों ने अंतरिम सरकार की संरचना और शक्तियों पर समझौते को रोक दिया।
- सांप्रदायिक तनाव: मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल पर मुस्लिम लीग के जोर ने कांग्रेस के साथ घर्षण पैदा किया, जिससे बातचीत जटिल हो गई।
- नेतृत्व संघर्ष: नेताओं के बीच व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता और भिन्न एजेंडों ने रचनात्मक संवाद को बाधित किया।
- ब्रिटिश की अनिच्छा: ब्रिटिश सरकार की योजना के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने की अनिच्छा और नियंत्रण बनाए रखने की उसकी इच्छा ने चर्चाओं को और जटिल बना दिया।
शिमला सम्मेलन के बाद
- राजनीतिक गतिरोध जारी: सम्मेलन की विफलता ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ती खाई को उजागर किया और एक एकीकृत राजनीतिक समाधान प्राप्त करने की चुनौतियों को रेखांकित किया।
- विभाजन की ओर बदलाव: एक समझौते तक पहुँचने में असमर्थता ने बाद की वार्ताओं के लिए मंच तैयार किया, जिससे अंततः 1947 में माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन हुआ।
| पहलू | वेवेल योजना (1945) | शिमला सम्मेलन (1945) |
| संदर्भ | द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वशासन को संबोधित करने के लिए प्रस्तावित। | भारत के लिए एक संवैधानिक ढाँचे पर बातचीत करने का लक्ष्य रखा। |
| प्रस्तावक | लॉर्ड वेवेल, तत्कालीन भारत के वायसराय। | लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रमुख भारतीय नेताओं के साथ बुलाया गया। |
| प्रमुख उद्देश्य | एक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करें। भारतीय नेताओं को विभिन्न दलों से शामिल करें। सांप्रदायिक तनावों को संबोधित करें। | एक अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा करें। |
| प्रमुख प्रावधान | एक कार्यकारी परिषद का गठन। विभिन्न समुदायों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व। | मुस्लिम प्रतिनिधित्व और शासन संरचना पर चर्चा केंद्रित। |
| प्रतिभागी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अन्य राजनीतिक समूह। | कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दलों के नेता। |
| मुख्य मुद्दे | सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असहमति। भविष्य की शासन संरचना पर आम सहमति का अभाव। | मुख्य रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच शक्ति-साझाकरण के संबंध में असहमति। |
| परिणाम | मुस्लिम लीग द्वारा अपर्याप्त मुस्लिम प्रतिनिधित्व के कारण अस्वीकृत। | एक समझौते तक पहुँचने में विफल रहा, कोई अंतरिम सरकार स्थापित नहीं हुई। |
| परिणाम | समुदायों के बीच तनाव बढ़ा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस (1946) का मार्ग प्रशस्त किया। | कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गहरे होते विभाजन और अविश्वास को उजागर किया। |
रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह (1946): बंबई, कराची, कलकत्ता
परिचय
1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले प्रतिरोध के अंतिम प्रमुख कृत्यों में से एक था। यह विद्रोह, जो मुख्य रूप से बंबई (अब मुंबई), कराची और कलकत्ता (अब कोलकाता) में हुआ था, नौसैनिक रेटिंग्स के बीच असंतोष और व्यापक राष्ट्रवादी उत्साह के संयोजन से प्रेरित था। इसने न केवल सशस्त्र बलों के भीतर बढ़ती अशांति का संकेत दिया, बल्कि स्वशासन और गरिमा के लिए भारतीय आबादी की व्यापक आकांक्षाओं को भी उजागर किया।
ऐतिहासिक संदर्भ
- युद्ध के बाद का माहौल: द्वितीय विश्व युद्ध के समापन ने ब्रिटेन को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया, जिससे उसके उपनिवेशों से स्वतंत्रता की मांगों में वृद्धि हुई। भारत, जिसने युद्ध प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, में राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि देखी गई।
- औपनिवेशिक असंतोष: इस अवधि में ब्रिटिश शासन के प्रति heightened असंतोष देखा गया, जिसकी विशेषता आर्थिक कठिनाइयाँ, भोजन की कमी और राजनीतिक दमन थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने पहले ही तीव्र उपनिवेश-विरोधी भावनाओं के लिए आधार तैयार कर दिया था।
विद्रोह के कारण
- खराब काम करने की स्थिति: रॉयल इंडियन नेवी में रेटिंग्स को दयनीय रहने की स्थिति, अपर्याप्त भोजन आपूर्ति और न्यूनतम चिकित्सा सुविधाओं का सामना करना पड़ा। खराब गुणवत्ता वाले भोजन की रिपोर्ट, खासकर जहाजों पर, आम थी।
- नस्लीय भेदभाव: ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित भेदभाव ने भारतीय नाविकों के बीच नाराजगी पैदा की। उन्हें कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ा और अक्सर उनके ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में दूसरे दर्जे के कर्मियों के रूप में व्यवहार किया जाता था।
- राजनीतिक जागरण: राष्ट्रवादी आंदोलनों और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के विचारों के प्रभाव ने कई रेटिंग्स को अधिकारों और पहचान की तलाश करने के लिए प्रेरित किया।
- ट्रिगरिंग घटना: विद्रोह का तात्कालिक उत्प्रेरक एचएमआईएस तलवार पर रेटिंग्स को भोजन की गुणवत्ता के विरोध के लिए दंडित करने का ब्रिटिश निर्णय था, जिससे एक विस्फोटक प्रतिक्रिया हुई।
विद्रोह के प्रमुख स्थान
बंबई (मुंबई):
- प्रारंभिक प्रकोप: विद्रोह 18 फरवरी, 1946 को भड़क उठा, जब बंबई बंदरगाह पर कई जहाजों पर रेटिंग्स ने आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने “जय हिंद” और “डाउन विद द ब्रिटिश” जैसे नारे लगाए।
- अशांति का फैलाव: विद्रोह तेजी से कई जहाजों तक फैल गया और इसमें हजारों नौसैनिक कर्मी शामिल थे। रेटिंग्स ने हड़तालें आयोजित कीं, जिससे शहर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।
- नागरिक समर्थन: स्थानीय नागरिकों, जिनमें श्रम संघ और छात्र शामिल थे, ने नाविकों के साथ एकजुटता दिखाई, विरोध प्रदर्शन और हड़तालें आयोजित कीं, जिससे अशांति तेज हो गई।
कराची:
- नौसैनिक अड्डे का महत्व: कराची एक प्रमुख नौसैनिक अड्डा था, और विद्रोह यहां तेजी से फैल गया। रेटिंग्स ने ब्रिटिश अधिकार का विरोध किया, बंबई में व्यक्त भावनाओं को प्रतिध्वनित किया।
- सैन्य प्रतिक्रिया: ब्रिटिश ने सैन्य बल के साथ जवाब दिया, विद्रोह को दबाने और व्यवस्था बहाल करने के लिए सैनिकों को तैनात किया, जिसमें रेटिंग्स के खिलाफ गिरफ्तारी और दंडात्मक उपाय शामिल थे।
कलकत्ता (कोलकाता):
- एकजुटता आंदोलन: विद्रोह ने कलकत्ता में महत्वपूर्ण समर्थन को प्रेरित किया, जहां डॉकवर्कर्स और ट्रेड यूनियनों ने नौसैनिक रेटिंग्स के साथ एकजुटता व्यक्त की। शहर में विरोध प्रदर्शन हुए, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा प्रदर्शित करते थे।
- राजनीतिक प्रभाव: कलकत्ता में अशांति ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला, जिससे नौसैनिक विद्रोह का पूरे भारत में व्यापक श्रम और स्वतंत्रता आंदोलनों के साथ अंतर्संबंध का पता चला।
सरकार की प्रतिक्रिया
- दमन के तरीके: ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह को कुचलने के लिए सैन्य इकाइयों को तैनात किया, विद्रोह के प्रमुख नेताओं और उत्तेजकों की गिरफ्तारी का सहारा लिया। बल के उपयोग का उद्देश्य आगे के असंतोष को डराना और हतोत्साहित करना था।
- बातचीत और वादे: बढ़ती अशांति के बीच, ब्रिटिश सरकार ने कुछ नौसैनिक नेताओं के साथ बातचीत शुरू की। हालांकि, इन चर्चाओं को बड़े पैमाने पर अवास्तविक माना गया और वे नाविकों की मौलिक शिकायतों को संबोधित करने में विफल रहीं।
- जन सहानुभूति: विद्रोह ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नाविकों के लिए व्यापक सहानुभूति बढ़ रही थी। इस सार्वजनिक समर्थन ने राजनीतिक सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया।
विद्रोह के बाद
- दमन और परिणाम: मार्च 1946 की शुरुआत तक, विद्रोह को प्रभावी ढंग से दबा दिया गया था, लेकिन इसके भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकार के लिए स्थायी प्रभाव थे। कार्रवाई से ब्रिटिश सेनाओं के मनोबल में महत्वपूर्ण कमी आई और आगे के विद्रोहों का डर बढ़ गया।
- राजनीतिक प्रभाव: विद्रोह की घटनाओं ने ब्रिटिश शासन की अस्थिर प्रकृति को उजागर किया और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच इस बढ़ती धारणा में योगदान दिया कि भारत की स्वतंत्रता अपरिहार्य थी। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के बिना विद्रोह को कुचलने में विफलता ने ब्रिटिश को भारत में शासन के लिए अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया।
- विरासत और स्मरण: रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को प्रतिरोध के एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में याद किया जाता है जिसने स्वतंत्रता के लिए बाद के आंदोलनों को प्रेरित किया। इसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक ले जाने वाली प्रमुख घटनाओं का एक अग्रदूत के रूप में कार्य किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ साहस और अवज्ञा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।
कैबिनेट मिशन (1946): संघीय योजना, प्रांतों का समूहीकरण
परिचय
1946 का कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में राजनीतिक गतिरोध को हल करने और स्वशासन की दिशा में संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण राजनयिक पहल थी। इस मिशन ने भारत के लिए एक संघीय संरचना का प्रस्ताव किया, जिसमें धार्मिक जनसांख्यिकी के आधार पर प्रांतों का समूहीकरण शामिल था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव भारत को उसकी स्वतंत्रता तक ले जाने वाले राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण थे।
ऐतिहासिक संदर्भ
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गतिशीलता: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ब्रिटेन को भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ा। युद्ध ने ब्रिटिश अधिकार को कमजोर कर दिया था और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ा दिया था।
- राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग स्वतंत्रता के लिए वकालत करने वाले प्रमुख राजनीतिक संस्थाएँ थीं, लेकिन भारत के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण काफी भिन्न थे।
- बातचीत के पिछले प्रयास: 1942 में क्रिप्स मिशन जैसे बातचीत के पिछले प्रयास विफल रहे थे, जिससे ब्रिटिश को भारतीय प्रश्न को हल करने के लिए एक नई रणनीति खोजने के लिए प्रेरित किया गया था।
कैबिनेट मिशन के उद्देश्य
- स्वतंत्रता के लिए एक ढाँचा बनाना: मिशन का उद्देश्य एक ढाँचा स्थापित करना था जो भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा जबकि विभिन्न राजनीतिक गुटों की चिंताओं को संबोधित करेगा।
- समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देना: मिशन ने एक संघीय संरचना बनाने की मांग की जो भारत में विभिन्न समुदायों, विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के विविध हितों को समायोजित करेगी।
कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्ताव
संघीय संरचना:
तीन-स्तरीय प्रणाली: कैबिनेट मिशन ने एक तीन-स्तरीय संघीय प्रणाली का प्रस्ताव किया, जिसमें शामिल थे:
- केंद्र सरकार: रक्षा, विदेश मामलों, संचार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार।
- प्रांतीय सरकारें: प्रत्येक प्रांत को स्थानीय मामलों पर स्वायत्तता होगी, जिससे क्षेत्रीय शासन की अनुमति होगी।
- समूह शासन: धार्मिक जनसांख्यिकी के आधार पर प्रांतों को क्षेत्रों में समूहित किया जाएगा, जिससे सामूहिक शासन की अनुमति होगी।
प्रांतों का समूहीकरण:
- समूह ए: हिंदू-बहुल प्रांत, जिनमें शामिल थे:
- मद्रास (तमिलनाडु)
- बंबई (महाराष्ट्र)
- संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश)
- मध्य प्रांत (मध्य प्रदेश)
- बिहार
- उड़ीसा (ओडिशा)
- समूह बी: मुस्लिम-बहुल प्रांत, जिनमें शामिल थे:
- पंजाब
- बंगाल
- सिंध
- समूह सी: मिश्रित आबादी वाले प्रांत, जैसे:
- उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत (NWFP)
- असम
- वैकल्पिक समूहीकरण: प्रांतों को किसी भी समूह में शामिल होने का विकल्प चुन सकते थे, जिससे उन्हें शासन में कुछ हद तक लचीलापन मिलता था।
संविधान सभा:
- मिशन ने भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया, जिसमें दोनों समूहों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
अंतरिम सरकार:
- स्वतंत्रता के संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतरिम सरकार स्थापित की जाएगी, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दलों, जिनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग शामिल हैं, का प्रतिनिधित्व होगा।
कैबिनेट मिशन के प्रति प्रतिक्रियाएँ
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस: शुरू में प्रस्तावों के प्रति ग्रहणशील, कांग्रेस ने एक संघीय संरचना की आवश्यकता को पहचाना लेकिन प्रांतों के समूहीकरण के संबंध में आरक्षण थे, विशेष रूप से सांप्रदायिक विभाजनों की संभावना के संबंध में।
- अखिल भारतीय मुस्लिम लीग: लीग ने प्रांतों के समूहीकरण के विचार का दृढ़ता से समर्थन किया, इसे मुस्लिम हितों की रक्षा के साधन के रूप में देखा। हालांकि, उन्होंने बाद में प्रस्तावों के प्रति कांग्रेस की प्रतिक्रिया से असंतोष व्यक्त किया।
- अन्य राजनीतिक दल: विभिन्न क्षेत्रीय दलों और समूहों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ थीं, कुछ ने अधिक स्वायत्तता का समर्थन किया जबकि अन्य प्रस्तावित संघीय संरचना के निहितार्थों के बारे में चिंतित थे।
कैबिनेट मिशन की विफलता
- आम सहमति का अभाव: प्रस्तावों की शर्तों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच असहमति के कारण बातचीत टूट गई।
- राजनीतिक पैंतरेबाज़ी: दोनों पक्षों द्वारा बाद की राजनीतिक पैंतरेबाज़ी ने स्थिति को और जटिल बना दिया, कांग्रेस मुस्लिम लीग की एक अलग राज्य की मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी।
- ब्रिटिश वापसी: कैबिनेट मिशन की आम सहमति प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप अंततः ब्रिटिश सरकार ने मिशन को छोड़ने का फैसला किया, जिससे तनाव बढ़ गया और अंततः भारत का विभाजन हुआ।
परिणाम और परिणाम
- सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि: कैबिनेट मिशन की विफलता ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन में योगदान हुआ।
- विभाजन की प्रस्तावना: एक संयुक्त राजनीतिक समाधान बनाने में असमर्थता ने 1947 में भारत के अंततः विभाजन के लिए मंच तैयार किया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ।
- विरासत: कैबिनेट मिशन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बनी हुई है, जो एक विविध समाज में स्वतंत्रता पर बातचीत की जटिलताओं और विभिन्न राजनीतिक आकांक्षाओं को समायोजित करने की चुनौतियों को दर्शाती है।
अंतरिम सरकार का गठन: नेहरू उपराष्ट्रपति के रूप में
परिचय
1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और इसने 1947 में भारत की अंततः स्वतंत्रता के लिए मंच तैयार किया। यह सरकार राजनीतिक वार्ताओं, सांप्रदायिक तनावों और एक प्रतिनिधि सरकार की मांग से चिह्नित एक tumultuous अवधि के दौरान स्थापित की गई थी। 86 जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति के रूप में भूमिका इसकी नीतियों और दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण थी।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का संदर्भ: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ब्रिटेन को भारत को स्वशासन प्रदान करने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश शक्ति की कमजोर स्थिति और भारतीय राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर के कारण।
- कैबिनेट मिशन (1946): कैबिनेट मिशन ने शासन के लिए एक ढाँचा प्रस्तावित किया जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की ओर संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतरिम प्रशासन की स्थापना शामिल थी।
- राजनीतिक परिदृश्य: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग प्रमुख राजनीतिक ताकतें थीं, लेकिन भारत के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण भिन्न थे, जिससे जटिल वार्ताएं हुईं।
अंतरिम सरकार का गठन
- घोषणा: 2 सितंबर, 1946 को, ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता के संक्रमण की देखरेख के लिए एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। यह सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के भारतीय नेताओं से बनी थी।
- संरचना: अंतरिम सरकार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। इसका उद्देश्य भारत के विविध राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाने वाला एक व्यापक गठबंधन बनाना था।
- नेतृत्व: सरकार का नेतृत्व एक गवर्नर-जनरल करता था, जिसमें लॉर्ड वेवेल प्रारंभिक चरण के दौरान इस क्षमता में सेवा करते थे।
जवाहरलाल नेहरू की भूमिका
- उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति: जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था, जिससे वे प्रशासन में प्रमुख आंकड़ों में से एक बन गए।
- जिम्मेदारियां: उपराष्ट्रपति के रूप में, नेहरू विभिन्न विभागों की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे, विशेष रूप से विदेश मामलों और रक्षा से संबंधित, जो इस संक्रमणकालीन चरण के दौरान महत्वपूर्ण थे।
- नीति पर प्रभाव: नेहरू ने सरकार की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास और भारत में विविध समुदायों के बीच एकता की वकालत की।
अंतरिम सरकार द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ
- सांप्रदायिक तनाव: अंतरिम सरकार को बढ़ते सांप्रदायिक तनावों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, जिसने इसकी स्थिरता और प्रभावशीलता को कमजोर करने की धमकी दी।
- मुस्लिम लीग की मांगें: मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने मुस्लिम-बहुल प्रांतों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की और अंततः पाकिस्तान के निर्माण की वकालत की। इसने सरकार के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ खड़ी कीं।
- आंतरिक विवाद: कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों ने प्रभावी शासन और निर्णय लेने में बाधाएँ पैदा कीं।
अंतरिम सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ
- सुधारों की शुरुआत: चुनौतियों के बावजूद, अंतरिम सरकार ने सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुधार शुरू किए।
- संवैधानिक ढाँचा: सरकार ने एक नया संविधान बनाने के लिए आधार तैयार किया, जिसमें भारत में सभी समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व और अधिकारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध: विदेश मामलों पर नेहरू के प्रभाव ने वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति स्थापित करने में मदद की, गुटनिरपेक्षता और अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग की वकालत की।
अंतरिम सरकार का पतन
- विवादों को हल करने में विफलता: भारत के भविष्य के संबंध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विवादों को हल करने में असमर्थता के कारण अंतरिम सरकार के प्रति बढ़ती असंतोष हुआ।
- सत्ता का हस्तांतरण: बढ़ते तनाव और ब्रिटिश वापसी की आसन्न समय सीमा ने सत्ता के हस्तांतरण के लिए बातचीत को प्रेरित किया, जो अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता में समाप्त हुआ।
मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान (16 अगस्त, 1946)
परिचय
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त, 1946 को नामित प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। 109 यह घटना केवल एक प्रदर्शन नहीं थी; इसने पाकिस्तान की मांग से संबंधित राजनीतिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरे होते सांप्रदायिक विभाजन को उजागर किया। 110 प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ मुस्लिम लीग की बढ़ती निराशाओं में निहित था।
ऐतिहासिक संदर्भ
1946 से पहले का राजनीतिक माहौल
- राष्ट्रवादी आंदोलन: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही गति पकड़ रहा था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक गुट उभर रहे थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे शख्सियतों के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से मुक्त एक एकजुट भारत की मांग की।
- मुस्लिम लीग का उद्भव: 1906 में स्थापित, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का शुरुआती उद्देश्य एक एकजुट भारत के भीतर मुस्लिम हितों को बढ़ावा देना था। हालांकि, 1940 के दशक तक, मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के विचार की वकालत की, जिसे उन्होंने पाकिस्तान कहा।
विफल वार्ताएँ
- कैबिनेट मिशन योजना (1946): ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए एक संघीय संरचना का प्रस्ताव किया जो प्रांतों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करेगा जबकि भारत को एकजुट रखेगा। हालांकि, यह योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के अंतर को पाट नहीं पाई। लीग को लगा कि मुसलमानों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सुरक्षा उपायों की उनकी मांगों को अपर्याप्त रूप से संबोधित किया गया था।
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के उद्देश्य
मुस्लिम पहचान पर जोर देना
- राजनीतिक दावा: प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान भारत में मुस्लिम पहचान और राजनीतिक अधिकारों पर जोर देने के लिए किया गया था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुसलमानों के बीच अपने समर्थन की ताकत और उनकी शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता को प्रदर्शित करना था।
पाकिस्तान की मांग
- हिंदू बहुमत से अलगाव: लीग के नेतृत्व का मानना था कि मुसलमान भेदभाव और हाशिए पर रहने का सामना किए बिना एक एकजुट भारत में हिंदुओं के साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते। इसलिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस एक अलग राष्ट्र की मांग को मुखर करने का एक मंच था जहाँ मुसलमान खुद पर शासन कर सकें।
समर्थन का लामबंदी
- जन भागीदारी: लीग ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को प्रदर्शनों और रैलियों में भाग लेने के लिए लामबंद करने की मांग की, ताकि कथित अन्याय के सामने एकता और संकल्प प्रदर्शित किया जा सके।
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घटनाएँ
घोषणा और तैयारी
- घोषणा: 29 जुलाई, 1946 को, मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया। तैयारियों में विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में रैलियों, जुलूसों और बैठकों का आयोजन शामिल था।
प्रारंभिक शांतिपूर्ण सभाएँ
- प्रदर्शन: उस दिन, मुस्लिम लीग की मांगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कलकत्ता (अब कोलकाता) जैसे शहरों में शांतिपूर्ण सभाएँ आयोजित की गईं। माहौल शुरू में हिंसा के बजाय शांतिपूर्ण वकालत की उम्मीद को दर्शाता था।
हिंसा में वृद्धि
- कलकत्ता दंगे: स्थिति तेजी से बिगड़ गई क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। 128 जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ, वह व्यापक दंगे में बदल गया, खासकर कलकत्ता में। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि हिंसा को पहले से मौजूद सांप्रदायिक शत्रुता से बढ़ावा मिला था, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच टकराव हुआ।
- हताहत: दंगों के परिणामस्वरूप अनुमानित 5,000 से 10,000 मौतें हुईं, जिसमें हजारों घायल और विस्थापित हुए। हिंसा की क्रूरता ने राष्ट्र को झकझोर दिया और अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया।
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम
सांप्रदायिक तनाव
- बिगड़ते संबंध: प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ने पूरे भारत में सांप्रदायिक तनावों को तेज कर दिया, जिससे प्रतिशोधी हिंसा का एक चक्र चला। इसने हिंदू-मुस्लिम संबंधों में एक बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें समुदायों के बीच ध्रुवीकरण और अविश्वास में वृद्धि हुई।
मुस्लिम लीग को मजबूत करना
राजनीतिक वैधता
- प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की हिंसक घटनाओं ने मुस्लिम लीग की स्थिति को मुस्लिम हितों के प्राथमिक प्रतिनिधि के रूप में मजबूत किया। लीग ने अराजकता का फायदा उठाया ताकि खुद को मुसलमानों के संरक्षक के रूप में चित्रित किया जा सके, जिससे आगे राजनीतिक वैधता प्राप्त हुई।
जनभावना में बदलाव
विभाजन के लिए बढ़ता समर्थन
- रक्तपात और अराजकता ने कई मुसलमानों के बीच एक बढ़ती हुई भावना में योगदान दिया कि उनकी सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों के लिए एक अलग राष्ट्र आवश्यक था। इस विश्वास ने बाद के महीनों में जोर पकड़ा, जिससे विभाजन के लिए बढ़ती मांगें हुईं।
स्वतंत्रता वार्ताओं पर प्रभाव
- विभाजन प्रक्रिया को तेज करना: प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद के परिणामों ने भारत में राजनीतिक संकट को हल करने की तात्कालिकता को रेखांकित किया। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि एक समाधान की आवश्यकता थी, जिससे अंततः विभाजन और अगस्त 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के लिए बातचीत हुई।
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की विरासत
ऐतिहासिक महत्व
- एक महत्वपूर्ण मोड़: प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जो बातचीत और संवाद से टकराव और हिंसा में संक्रमण को चिह्नित करता है। इसने भारत में सांप्रदायिक राजनीति की जटिलताओं को दर्शाया।
राष्ट्रीय पहचान पर प्रतिबिंब
- सांप्रदायिकता और उसकी चुनौतियाँ: 16 अगस्त, 1946 की घटनाएँ राष्ट्र-निर्माण में सांप्रदायिक पहचानों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की याद दिलाती हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की विरासत समकालीन भारत और पाकिस्तान में सांप्रदायिकता, राष्ट्रवाद और पहचान के बारे में चर्चाओं को प्रभावित करती रहती है।
स्मरण और स्मृति
- स्मरणोत्सव: पाकिस्तान में, 16 अगस्त को राष्ट्र की स्थापना के लिए किए गए बलिदानों पर चिंतन के दिन के रूप में मनाया जाता है। भारत में, यह सांप्रदायिक हिंसा के दुखद परिणामों की याद दिलाता है।
बहुविकल्पीय प्रश्न:-
- कालक्रम प्रश्न निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: A. कैबिनेट मिशन B. क्रिप्स मिशन C. वेवेल योजना (शिमला सम्मेलन) D. अगस्त प्रस्ताव E. रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह विकल्प:
- 1‑3‑2‑4‑5
- 4‑2‑3‑5‑1
- 4‑3‑1‑5‑2
- 5‑2‑3‑4‑1 उत्तर: विकल्प 2 — 4 (1940) → 2 (1942) → 3 (1945) → 5 (फरवरी 1946) → 1 (मार्च 1946) 147
- कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- 1946 में सत्ता के हस्तांतरण पर बातचीत करने के लिए भेजा गया
- मजबूत क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ दो-स्तरीय संघीय योजना प्रस्तावित की
- व्यक्तिगत प्रांतों को संरक्षित किया और प्रांतीय संघों की अनुमति दी
- उपरोक्त सभी उत्तर: सभी कथन सही हैं
- भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? A) आर.जे. मूर B) ए.वी. कैंपबेल C) पेथिक लॉरेंस D) डेविड वार्नर उत्तर: पेथिक लॉरेंस
- निम्नलिखित में से किसके तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था? 152 विकल्प:
- भारत सरकार अधिनियम 1935
- क्रिप्स प्रस्ताव 1942
- कैबिनेट मिशन योजना 1946
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उत्तर: (c) कैबिनेट मिशन योजना, 1946