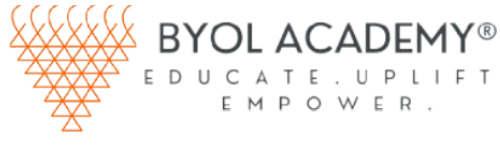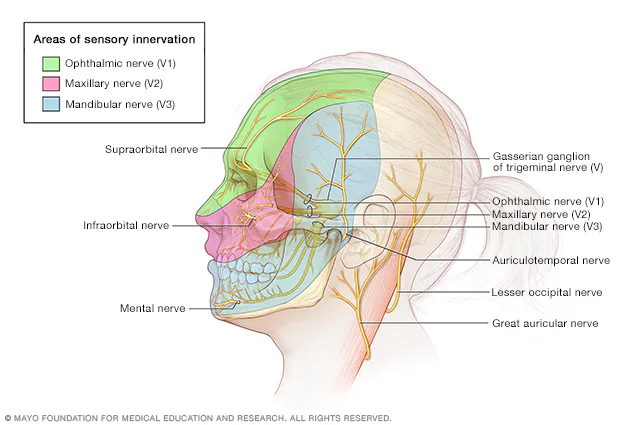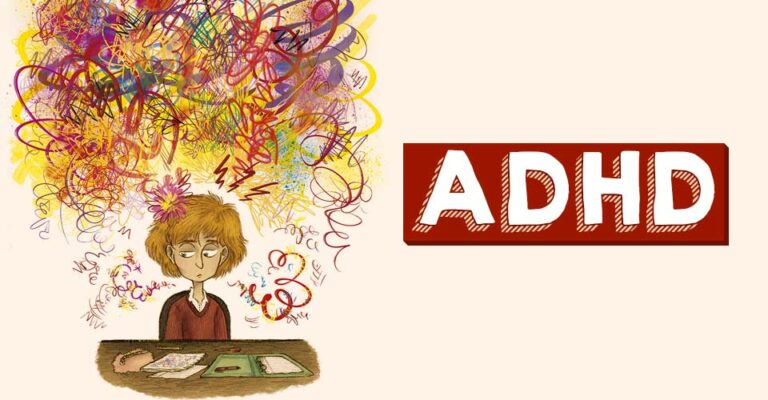परिचय
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 तक चला, राजनीतिक सुधारों को प्राप्त करने के लिए एक सतर्क और संवैधानिक दृष्टिकोण की अवधि थी । इस चरण के नेताओं ने परिवर्तन लाने के लिए अनुनय और कानूनी तरीकों की शक्ति में विश्वास किया । उन्होंने भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व और अधिकार सुरक्षित करने के लिए मौजूदा ब्रिटिश कानूनी ढांचे के भीतर काम करने की मांग की । इस चरण ने जागरूकता बढ़ाकर और भारतीय आवाज़ों के लिए एक मंच बनाकर, बाद के अधिक कट्टरपंथी आंदोलनों की नींव रखी ।
प्रमुख नेता
- गोपाल कृष्ण गोखले
- पृष्ठभूमि: गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता और महात्मा गांधी सहित कई भविष्य के नेताओं के गुरु थे ।
- दर्शन: उन्होंने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, क्रमिक सुधार और कानूनी प्रणाली के भीतर काम करने के महत्व पर जोर दिया ।
- उपलब्धियां: गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गठन में सहायक थे, जिसका उद्देश्य सेवा और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा देना था ।
- दादाभाई नौरोजी
- पृष्ठभूमि: “भारत के वयोवृद्ध” के रूप में जाने जाने वाले नौरोजी एक प्रमुख अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे ।
- दर्शन: उन्होंने ब्रिटिश नीतियों को प्रभावित करने के लिए आर्थिक तर्कों की शक्ति में विश्वास किया और स्वशासन की वकालत की ।
- उपलब्धियां: नौरोजी का “धन के निष्कासन” का सिद्धांत भारत में ब्रिटिश आर्थिक शोषण की समझ में एक मौलिक योगदान था । उन्होंने ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में भी कार्य किया, जहाँ उन्होंने भारतीय अधिकारों की वकालत जारी रखी ।
- फिरोजशाह मेहता
- पृष्ठभूमि: एक वकील और राजनीतिज्ञ, मेहता प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख व्यक्ति थे ।
- दर्शन: उन्होंने स्वशासन और सिविल सेवा के भारतीयकरण की वकालत की, जिसमें भारतीयों को अपने स्वयं के प्रशासन में अधिक भूमिका की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।
- उपलब्धियां: मेहता ने बंबई में नगरपालिका सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कांग्रेस के भीतर संवैधानिक तरीकों के लिए एक मजबूत आवाज थे ।
तकनीकें
उदारवादियों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल किया:
- याचिकाएं:
- विवरण: ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत औपचारिक अनुरोध, जिसमें शिकायतें और मांगें बताई गई थीं ।
- उदाहरण: वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878) को निरस्त करने और नमक कर को कम करने के लिए याचिकाएं ।
- प्रभाव: इन याचिकाओं ने जागरूकता बढ़ाने और सुधारों के लिए एक मामला बनाने में मदद की, हालांकि वे अक्सर तत्काल परिवर्तनों को जन्म नहीं देती थीं ।
- प्रस्ताव:
- विवरण: कांग्रेस सत्रों और अन्य सार्वजनिक बैठकों में पारित औपचारिक बयान, जिसमें सामूहिक राय और मांगें व्यक्त की गईं ।
- उदाहरण: विधान परिषदों के विस्तार और सेवाओं के भारतीयकरण की मांग करने वाले प्रस्ताव ।
- प्रभाव: प्रस्तावों का उपयोग जन समर्थन बनाने और सरकार पर दबाव डालने के लिए किया गया था, जिससे एक संयुक्त राष्ट्रीय राय के गठन में योगदान मिला ।
- प्रतिनिधिमंडल:
- विवरण: मुद्दों पर चर्चा करने और सुधारों की तलाश के लिए ब्रिटिश अधिकारियों से मिलने के लिए भेजे गए प्रतिनिधिमंडल ।
- उदाहरण: भारत के राज्य सचिव और वायसराय को प्रतिनिधिमंडल ।
- प्रभाव: इन बैठकों का उद्देश्य सरकार को सुधारों को लागू करने के लिए मनाना था, हालांकि वे अक्सर सीमित सफलता के साथ मिलीं ।
मांगें
उदारवादियों की मांगों का एक स्पष्ट समूह था, जिसे उन्होंने अपने संवैधानिक तरीकों से पूरा किया:
- विधान परिषदों का विस्तार:
- उद्देश्य: विधायी निकायों में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाना, जिससे भारतीयों को देश के शासन में अधिक कहने का मौका मिले ।
- तर्क: उदारवादियों का मानना था कि अधिक प्रतिनिधित्व से अधिक उत्तरदायी और निष्पक्ष शासन होगा ।
- प्रभाव: 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषदों में गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर इस मांग को आंशिक रूप से संबोधित किया, हालांकि ब्रिटिशों ने प्रमुख निर्णयों पर नियंत्रण बनाए रखा ।
- सेवाओं का भारतीयकरण:
- उद्देश्य: सिविल सेवा और अन्य सरकारी भूमिकाओं में उच्च पदों पर अधिक भारतीयों को नियुक्त करने की मांग करना, ब्रिटिश अधिकारियों के प्रभुत्व को कम करना ।
- तर्क: उदारवादियों ने तर्क दिया कि भारतीय इन पदों को धारण करने में समान रूप से सक्षम थे और उनका बहिष्करण नस्लीय भेदभाव का एक रूप था ।
- प्रभाव: यह मांग सिविल सेवा के भारतीयकरण का अग्रदूत थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद के चरणों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई ।
उपलब्धियां
उदारवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया:
- आर्थिक निष्कासन का खुलासा:
- सिद्धांत: दादाभाई नौरोजी के “धन के निष्कासन” सिद्धांत ने तर्क दिया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन विभिन्न माध्यमों से भारत के धन को निकाल रहा था, जिसमें कच्चे माल का निर्यात, तैयार माल का आयात और ब्रिटिश कंपनियों द्वारा लाभ का प्रेषण शामिल था ।
- सबूत: नौरोजी ने अपने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए विस्तृत आर्थिक डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाया गया ।
- प्रभाव: सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली और इसका उपयोग आर्थिक सुधारों और आर्थिक नीतियों पर अधिक भारतीय नियंत्रण के लिए तर्क देने के लिए किया गया । इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत को जुटाने में भी मदद की ।
- भारतीय राय का गठन:
- मंच: उदारवादियों ने लोगों के बीच राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक चेतना की भावना को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक बैठकें आयोजित कीं, समाचार पत्र प्रकाशित किए और लेख लिखे ।
- उदाहरण: “द टाइम्स ऑफ इंडिया” और “द हिंदू” जैसे समाचार पत्रों की स्थापना, और किताबों और पुस्तिकाओं का प्रकाशन ।
- प्रभाव: ये प्रयास भारतीय आवाज़ों को सुनने के लिए एक मंच बनाने और एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण थे । उन्होंने देश के सामने आने वाले मुद्दों और सुधारों की आवश्यकता के बारे में जनता को शिक्षित करने में मदद की ।
चरमपंथियों द्वारा आलोचना
अपनी उपलब्धियों के बावजूद, उदारवादियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी गुट की आलोचना का सामना करना पड़ा:
- “राजनीतिक भिक्षावृत्ति”:
- आलोचना: बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे चरमपंथी नेताओं ने उदारवादी दृष्टिकोण की आलोचना की कि यह बहुत विनम्र और सुधारों के लिए अंग्रेजों से अपील करने पर निर्भर था ।
- तर्क: उन्होंने उदारवादी तरीकों को “राजनीतिक भिक्षावृत्ति” के रूप में देखा, यह सुझाव देते हुए कि उदारवादी अपने अधिकारों की मांग करने के बजाय अंग्रेजों से टुकड़े मांग रहे थे ।
- प्रभाव: आलोचना ने कांग्रेस के भीतर एक बढ़ते विभाजन को जन्म दिया और अंततः 1907 में सूरत विभाजन का परिणाम हुआ। चरमपंथियों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन और बहिष्कार सहित अधिक मुखर और प्रत्यक्ष कार्रवाई में विश्वास किया ।
तालिका: उदारवादी चरण की प्रमुख घटनाएं और मील के पत्थर (1885-1905)
| वर्ष | घटना | महत्व |
| 1885 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन | भारत में संगठित राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत को चिह्नित किया । |
| 1886 | कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र | उदारवादी दृष्टिकोण के लिए स्वर निर्धारित किया और कांग्रेस को एक राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया । |
| 1892 | भारतीय परिषद अधिनियम | विधान परिषदों में गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, हालांकि अभी भी सीमित थी । |
| 1893 | दादाभाई नौरोजी ने “धन के निष्कासन” सिद्धांत प्रस्तुत किया | अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया, व्यापक स्वीकृति प्राप्त की । |
| 1895 | गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की | सेवा और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा दिया । |
| 1905 | बंगाल का विभाजन | व्यापक विरोध प्रदर्शनों और चरमपंथी गुट के उदय का कारण बना । |
| 1906 | अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन | बढ़ती सांप्रदायिक तनाव और अधिक समावेशी राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला । |
| 1907 | सूरत विभाजन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और चरमपंथी गुटों में विभाजित हो गई, जिससे कांग्रेस अस्थायी रूप से कमजोर हो गई लेकिन नई रणनीतियों और नेताओं को जन्म दिया । |
स्थिर भाग
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
- उद्देश्य: विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाना ।
- प्रावधान:
- इंपीरियल विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई ।
- कुछ सदस्यों को निर्वाचित होने की अनुमति दी गई, हालांकि बहुमत अभी भी नामांकित थे ।
- परिषदों को बजट पर चर्चा करने और सरकारी अधिकारियों से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई ।
- प्रभाव: यद्यपि यह एक कदम आगे था, अधिनियम ने भारतीय सदस्यों को पर्याप्त शक्ति प्रदान नहीं की, और अंग्रेजों ने प्रमुख निर्णयों पर नियंत्रण बनाए रखा । हालांकि, यह शासन में भारतीय प्रतिनिधित्व की क्रमिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था ।
दादाभाई नौरोजी का “धन के निष्कासन” सिद्धांत
- अवधारणा: नौरोजी ने तर्क दिया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन विभिन्न माध्यमों से भारत के धन को निकाल रहा था, जिसमें कच्चे माल का निर्यात, तैयार माल का आयात और ब्रिटिश कंपनियों द्वारा लाभ का प्रेषण शामिल था ।
- सबूत: उन्होंने अपने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए विस्तृत आर्थिक डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाया गया ।
- प्रभाव: सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली और इसका उपयोग आर्थिक सुधारों और आर्थिक नीतियों पर अधिक भारतीय नियंत्रण के लिए तर्क देने के लिए किया गया । इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत को जुटाने में भी मदद की और राष्ट्रीय आंदोलन में भविष्य के आर्थिक तर्कों की नींव रखी ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
- गठन: 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादाभाई नौरोजी और अन्य द्वारा स्थापित ।
- उद्देश्य: भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करना और देश की बेहतरी के लिए काम करना ।
- तरीके: शुरू में, INC ने याचिकाओं, प्रस्तावों और प्रतिनिधिमंडलों जैसे संवैधानिक तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया ।
- उपलब्धियां:
- भारत के सामने आने वाले आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।
- एक राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण किया और भारतीयों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया ।
- भारतीय राय के गठन और एक राजनीतिक चेतना के विकास में योगदान दिया ।
सूरत विभाजन (1907)
- संदर्भ: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में सूरत सत्र में उदारवादी और चरमपंथी गुटों में विभाजित हो गई ।
- कारण:
- उदारवादियों और चरमपंथियों के बीच तरीकों और लक्ष्यों में अंतर ।
- उदारवादियों ने संवैधानिक तरीकों का समर्थन किया, जबकि चरमपंथियों ने अधिक कट्टरपंथी और प्रत्यक्ष कार्रवाई की वकालत की ।
- प्रभाव:
- विभाजन ने कांग्रेस को अस्थायी रूप से कमजोर कर दिया लेकिन नए नेताओं और रणनीतियों के उदय का भी कारण बना ।
- इसने राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर बढ़ते विभाजन और भारतीयों के विविध राजनीतिक विचारों को संबोधित करने के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ।
विस्तृत विश्लेषण
| पहलू | विवरण |
| राजनीतिक संदर्भ | उदारवादी चरण एक ऐसे संदर्भ में उभरा जहां ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार अपेक्षाकृत स्थिर और महत्वपूर्ण सुधारों के प्रति प्रतिरोधी थी। उदारवादियों का मानना था कि कानूनी और संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करके, वे धीरे-धीरे ब्रिटिश नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं और भारतीयों के लिए अधिक अधिकार सुरक्षित कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण इस विश्वास में निहित था कि ब्रिटिश स्वाभाविक रूप से दुर्भावनापूर्ण नहीं थे और भारत के सर्वोत्तम हितों में कार्य करने के लिए मनाए जा सकते थे । |
| आर्थिक संदर्भ | अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण इस चरण के दौरान एक प्रमुख मुद्दा था। दादाभाई नौरोजी के “धन के निष्कासन” सिद्धांत ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली आर्थिक तर्क प्रदान किया। सिद्धांत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिटिश नीतियां कैसे भारत के संसाधनों को व्यवस्थित रूप से निकाल रही थीं, जिससे गरीबी और अल्पविकास हो रहा था। यह आर्थिक आलोचना सुधारों के लिए एक मामला बनाने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत को जुटाने में महत्वपूर्ण थी । |
| सामाजिक संदर्भ | उदारवादियों ने सामाजिक मुद्दों को भी संबोधित किया, जैसे शिक्षा की आवश्यकता और सेवाओं का भारतीयकरण। गोपाल कृष्ण गोखले का शिक्षा और क्रमिक सुधार पर जोर एक अधिक सूचित और सक्षम भारतीय नेतृत्व के निर्माण के उद्देश्य से था। सेवाओं के भारतीयकरण की मांग नस्लीय भेदभाव और सिविल सेवा में उच्च पदों से भारतीयों के बहिष्कार की प्रतिक्रिया थी । |
| राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव | उदारवादी चरण ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जागरूकता बढ़ाकर और भारतीय आवाज़ों के लिए एक मंच बनाकर, उदारवादियों ने बाद के अधिक कट्टरपंथी आंदोलनों की नींव रखी। आर्थिक शोषण को उजागर करने और अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत करने के उनके प्रयासों ने भारतीय लोगों के बीच राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक चेतना की भावना पैदा करने में मदद की । |
| सीमाएं और आलोचनाएं | अपनी उपलब्धियों के बावजूद, उदारवादियों को कई सीमाओं और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा: <br> – सीमित सफलता: संवैधानिक तरीके अक्सर तत्काल या पर्याप्त परिवर्तनों को जन्म नहीं देते थे, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे । <br> – चरमपंथियों द्वारा आलोचना: चरमपंथी नेताओं ने उदारवादी दृष्टिकोण को बहुत निष्क्रिय और अप्रभावी माना। उनका मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अधिक मुखर और प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक थी । <br> – सांप्रदायिक तनाव: उदारवादी चरण में सांप्रदायिक तनाव का उदय भी देखा गया, जैसा कि 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन से प्रमाणित होता है। इसने अधिक समावेशी और प्रतिनिधि राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला । |
निष्कर्ष
उदारवादी चरण (1885-1905) भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अवधि थी । इस चरण के नेताओं ने अपने संवैधानिक तरीकों और स्पष्ट मांगों के माध्यम से, बाद के अधिक कट्टरपंथी आंदोलनों की नींव रखी । चरमपंथियों ने उनके दृष्टिकोण की आलोचना की, लेकिन उदारवादी लोगों को जागरूक करने, एक राष्ट्रीय मंच बनाने और परिवर्तनों के लिए दबाव डालने में महत्वपूर्ण थे । उनके प्रयास राष्ट्रीय आंदोलन के भविष्य को आकार देने और आने वाले वर्षों में अधिक मुखर कार्यों के लिए जमीन तैयार करने में सहायक थे ।
बहुविकल्पीय प्रश्न:
- ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस अधिनियम ने उदारवादी चरण के दौरान विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाया?
ए) भारतीय परिषद अधिनियम 1861
बी) भारतीय परिषद अधिनियम 1892
सी) भारत सरकार अधिनियम 1919
डी) भारतीय परिषद अधिनियम 1909
उत्तर: बी) भारतीय परिषद अधिनियम 1892
स्पष्टीकरण: 1892 के अधिनियम ने विधान परिषदों का विस्तार किया और कुछ सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की अनुमति दी, जिससे कुछ उदारवादी मांगों को संबोधित किया गया । - उदारवादियों द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया गया था?
ए) सशस्त्र विद्रोह
बी) बहिष्कार और स्वदेशी
सी) याचिकाएं और प्रस्ताव
डी) सविनय अवज्ञा
उत्तर: सी) याचिकाएं और प्रस्ताव
स्पष्टीकरण: उदारवादी सुधारों को लाने के लिए याचिकाओं, भाषणों और प्रस्तावों जैसे संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे ।
उदारवादियों ने शासन की किन दो शाखाओं के पृथक्करण पर जोर दिया?
ए) विधायी और कार्यकारी
बी) न्यायपालिका और कार्यकारी
सी) विधायी और न्यायपालिका
डी) सैन्य और सिविल सेवा
उत्तर: बी) न्यायपालिका और कार्यकारी
स्पष्टीकरण: उनका मानना था कि न्यायपालिका को कार्यकारी से अलग करने से निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित होगा ।