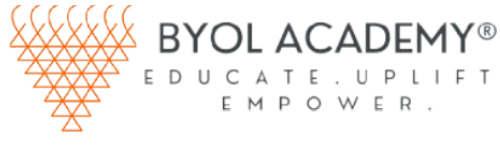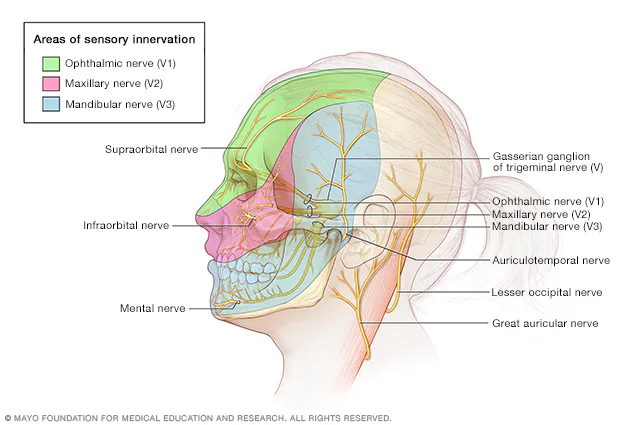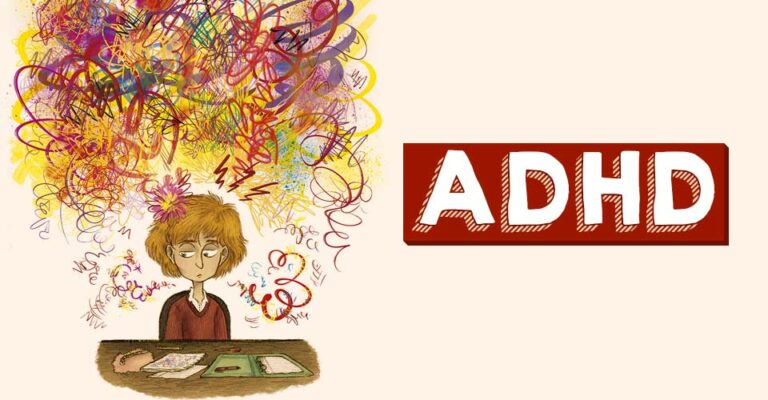- बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक (1939)
- भारत से पलायन, धुरी शक्तियों के साथ गठबंधन
- आजाद हिंद सरकार (1943) सिंगापुर में बनी
- आईएनए: इंफाल, कोहिमा में अभियान
- आईएनए परीक्षण (1945-46): भारी आक्रोश, नौसेना विद्रोह शुरू हुआ
सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक (1939)
पृष्ठभूमि
राजनीतिक संदर्भ: 1930 के दशक के अंत तक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की वकालत करने वाला प्रमुख संगठन था। हालाँकि, आंतरिक विभाजन स्पष्ट होते जा रहे थे, विशेष रूप से उदारवादी और कट्टरपंथी गुटों के बीच।
सुभाष चंद्र बोस: कांग्रेस के भीतर एक प्रमुख नेता, बोस स्वतंत्रता प्राप्त करने के अपने कट्टरपंथी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, जो महात्मा गांधी के अहिंसा और सविनय अवज्ञा के दर्शन के बिल्कुल विपरीत था।
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन
कांग्रेस से इस्तीफा: अप्रैल 1939 में, कांग्रेस के त्रिपुरी सत्र के दौरान, बोस को गांधी के समर्थकों से महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया।
स्थापना: जुलाई 1939 में, बोस ने औपचारिक रूप से फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य कांग्रेस की रणनीतियों से असंतुष्ट विभिन्न उपनिवेश-विरोधी गुटों को एकजुट करना था।
उद्देश्य
पूर्ण स्वतंत्रता: प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करना था।
सामाजिक न्याय: फॉरवर्ड ब्लॉक ने सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने की मांग की, ऐसे सुधारों पर जोर दिया जिससे श्रमिकों और किसानों को लाभ होगा।
साम्राज्य-विरोधी ताकतों की एकता: ब्लॉक का उद्देश्य सभी साम्राज्य-विरोधी तत्वों को मजबूत करना था, न कि केवल कांग्रेस के भीतर के लोगों को।
संरचना
नेतृत्व: बोस अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें श्रम और किसान संगठनों सहित विविध पृष्ठभूमि के सदस्यों वाली एक समिति का समर्थन प्राप्त था।
सदस्यता: ब्लॉक ने वामपंथियों, समाजवादियों और कम्युनिस्टों सहित विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को आकर्षित किया, जो इसके समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है।
वैचारिक अभिविन्यास
समाजवाद: फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया, जिसमें हाशिए के समुदायों के अधिकारों और आर्थिक सुधारों की वकालत की गई।
उग्रवादी प्रतिरोध: कांग्रेस के अहिंसक रुख के विपरीत, ब्लॉक ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध के लिए एक अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया।
गतिविधियाँ और लामबंदी
विरोध और रैलियां: ब्लॉक ने विभिन्न विरोध और रैलियों का आयोजन किया, जिससे सामाजिक अन्याय और सुधारों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई।
अभियान: पहल श्रम अधिकारों, भूमि सुधारों और उपनिवेश-विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर समर्थन जुटाना था।
चुनौतियाँ और विरोध
आंतरिक विभाजन: फॉरवर्ड ब्लॉक को विविध वामपंथी गुटों के बीच एकता बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
दमन: ब्रिटिश अधिकारियों ने ब्लॉक को एक खतरे के रूप में देखा, जिससे गिरफ्तारियाँ और उसकी गतिविधियों पर कार्रवाई हुई।
प्रभाव और विरासत
वामपंथी राजनीति पर प्रभाव: यद्यपि फॉरवर्ड ब्लॉक ने कांग्रेस के समान प्रभाव का स्तर हासिल नहीं किया, फिर भी इसने स्वतंत्रता के बाद के भारत में वामपंथी आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया।
बोस का दृष्टिकोण: समाजवाद और सामाजिक न्याय के संबंध में बोस के विचारों ने भारतीय राजनीति में गूंजना जारी रखा, जिससे भविष्य की राजनीतिक विचारधाराओं और आंदोलनों को प्रभावित किया।
भारत से पलायन और धुरी शक्तियों के साथ गठबंधन
पृष्ठभूमि
औपनिवेशिक संदर्भ: 1930 के दशक के अंत और 1940 के दशक की शुरुआत तक, भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ रहा था। विभिन्न गुट स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियों की खोज कर रहे थे।
द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव: 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने से एक जटिल भू-राजनीतिक वातावरण का निर्माण हुआ। कई भारतीय नेताओं ने संघर्ष को भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का लाभ उठाने के अवसर के रूप में देखा।
सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण
कट्टरपंथी दृष्टिकोण: सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता, का मानना था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसक प्रतिरोध आवश्यक था। उन्होंने ब्रिटेन का विरोध करने वाली विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन बनाने की मांग की।
धुरी शक्तियाँ: बोस ने धुरी शक्तियों – मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी और इंपीरियल जापान – को भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में संभावित सहयोगियों के रूप में देखा क्योंकि वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध करते थे।
भारत से पलायन (1941)
पलायन की परिस्थितियाँ: 1941 में, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा घर में नजरबंद किए जाने के बाद, बोस ने भारत से एक साहसी पलायन किया। वह अपने इच्छित गंतव्य तक पहुँचने के लिए अफगानिस्तान और जर्मनी सहित विभिन्न देशों से होकर गुजरे।
जर्मनी की यात्रा: बोस के पलायन में गुप्त आंदोलनों और वेश बदलने की एक श्रृंखला शामिल थी, अंततः उन्हें जर्मनी ले जाया गया, जहाँ उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन पर चर्चा करने के लिए जर्मन अधिकारियों से मुलाकात की।
धुरी शक्तियों के साथ गठबंधन
जर्मनी के साथ बातचीत: जर्मनी पहुँचने पर, बोस ने नाज़ियों से सैन्य और रसद सहायता मांगी। उनका उद्देश्य जर्मन संसाधनों की मदद से एक भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन करना था, यह मानते हुए कि अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य अभियान संभव होगा।
जापान के साथ सहयोग: जर्मनी में अपने समय के बाद, बोस 1943 में जापान चले गए, जहाँ उन्हें अपने उद्देश्य के लिए अधिक प्रत्यक्ष समर्थन मिला। जापानी सरकार एशिया में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को अस्थिर करने में रुचि रखती थी और बोस के प्रयासों में सहायता करने के लिए सहमत हुई।
भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन:
स्थापना: 1942 में, जापानी समर्थन से, बोस ने औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की स्थापना की। INA में भारतीय युद्धबंदी और प्रवासी शामिल थे जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए थे।
उद्देश्य
- उद्देश्य: INA का उद्देश्य सैन्य कार्रवाई के माध्यम से ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराना था, जिसमें एक निर्वासन में सरकार बनाने और देश के भीतर और बाहर दोनों जगह भारतीयों से समर्थन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
अभियान और सैन्य कार्रवाई
सैन्य अभियान: बोस के नेतृत्व में INA ने दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सेना के साथ कई सैन्य अभियानों में भाग लिया। उल्लेखनीय अभियानों में भारत में ब्रिटिश-अधिकृत क्षेत्रों पर आक्रमण शामिल था।
वैचारिक प्रचार: बोस ने INA को प्रचार के माध्यम से बढ़ावा दिया, जिसमें भारतीयों के बीच एकता के महत्व पर जोर दिया गया और संघर्ष को स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया गया।
सामना की गई चुनौतियाँ
सीमित संसाधन: INA को सीमित संसाधनों, खराब आपूर्ति लाइनों और जापानी सेना के साथ समन्वय की जटिलताओं सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
युद्ध के बाद के परिणाम: 1945 में जापान की हार के बाद, INA को वैधता के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई सदस्यों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे ऐसे मुकदमे हुए जिन्हें व्यापक जन सहानुभूति और आंदोलन के लिए समर्थन मिला।
विरासत और प्रभाव
राष्ट्रवादी भावना: बोस के धुरी शक्तियों के साथ गठबंधन और INA के उनके नेतृत्व ने कई भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। उनका कट्टरपंथी दृष्टिकोण अन्य नेताओं की अधिक उदारवादी रणनीतियों के विपरीत था और स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधनों के बारे में चर्चाएं खोलीं।
भविष्य के आंदोलनों पर प्रभाव: यद्यपि बोस के प्रयासों से तत्काल स्वतंत्रता नहीं मिली, फिर भी उन्होंने भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया और उपनिवेशवाद के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष पर विमर्श में योगदान दिया।
आजाद हिंद सरकार (1943) सिंगापुर में बनी
पृष्ठभूमि
ऐतिहासिक संदर्भ: आजाद हिंद सरकार, जिसे स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार के रूप में भी जाना जाता है, का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था जब भारत अभी भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। युद्ध ने एक अद्वितीय राजनीतिक वातावरण बनाया जिसने विभिन्न राष्ट्रवादी गुटों को स्वतंत्रता के लिए नए रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया।
सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व: सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की वकालत की और धुरी शक्तियों से समर्थन मांगा।
आजाद हिंद सरकार का गठन
घोषणा: 21 अक्टूबर, 1943 को, बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की। यह एक निर्वासन में सरकार के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम था।
स्थान: सरकार जापानी-अधिकृत सिंगापुर में स्थापित की गई थी, जिसने बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के लिए एक रणनीतिक आधार के रूप में कार्य किया।
उद्देश्य
पूर्ण स्वतंत्रता: आजाद हिंद सरकार का प्राथमिक लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था।
राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना: इसका उद्देश्य भारत और विदेश दोनों में भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना था, जो औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ एकता को प्रोत्साहित करता था।
सामाजिक और आर्थिक सुधार: सरकार ने सामाजिक अन्याय को संबोधित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की मांग की, जिसमें समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित एक स्वतंत्र भारत की परिकल्पना की गई थी।
सरकार की संरचना
नेतृत्व: सुभाष चंद्र बोस ने सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य किया, जिसमें राष्ट्रपति का पद धारण किया। उन्हें सैन्य नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के सदस्यों वाली एक परिषद का समर्थन प्राप्त था।
मंत्रिमंडल संरचना: मंत्रिमंडल में रक्षा, विदेश मामले और वित्त जैसे विभिन्न विभागों के लिए जिम्मेदार विभिन्न मंत्री शामिल थे, जो एक व्यापक शासन संरचना को दर्शाता है।
मान्यता और समर्थन
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता: आजाद हिंद सरकार ने अन्य राष्ट्रों, विशेष रूप से ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध करने वालों से मान्यता प्राप्त करने की मांग की। हालाँकि, इसे धुरी शक्तियों के साथ अपने जुड़ाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
INA से समर्थन: भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसका बोस ने नेतृत्व किया, ने सरकार का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उसके दावों को सैन्य शक्ति और वैधता मिली।
सैन्य अभियान
INA अभियान: आजाद हिंद सरकार ने भारत में ब्रिटिश सेना के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना के साथ समन्वय किया। INA का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्रों को मुक्त करना था।
इंफाल और कोहिमा की लड़ाई: यद्यपि INA ने जापानी सेना के साथ महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भाग लिया, फिर भी इसे झटके लगे, विशेष रूप से इंफाल और कोहिमा की लड़ाई में, जिसने इसकी प्रगति को बाधित किया।
चुनौतियाँ और सीमाएँ
सीमित संसाधन: सरकार बाधाओं के तहत संचालित होती थी, जिसमें पर्याप्त संसाधनों, सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी थी।
जापानी नियंत्रण: जापानी सेना पर निर्भरता ने तनाव पैदा किया और आजाद हिंद सरकार की स्वायत्तता को सीमित कर दिया, जिससे इसकी वैधता के बारे में सवाल उठे।
गिरावट और विघटन
द्वितीय विश्व युद्ध का अंत: 1945 में जापान की हार के साथ, आजाद हिंद सरकार ने अपना समर्थन आधार खो दिया, जिससे इसकी गिरावट हुई।
विघटन: जापान के आत्मसमर्पण के बाद, सरकार प्रभावी रूप से भंग कर दी गई, और कई INA नेताओं को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया।
विरासत और प्रभाव
प्रतिरोध का प्रतीक: आजाद हिंद सरकार स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक बन गई, जिसने राष्ट्रवादियों की भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित किया।
युद्ध के बाद का प्रभाव: युद्ध के बाद INA सैनिकों के मुकदमे ने महत्वपूर्ण जन सहानुभूति प्राप्त की, जिससे भारत की स्वतंत्रता के लिए गति मिली, जिसे 1947 में प्राप्त किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA): इंफाल और कोहिमा में अभियान
पृष्ठभूमि
द्वितीय विश्व युद्ध का संदर्भ: भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA), जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था, का गठन धुरी शक्तियों, मुख्य रूप से जापान के समर्थन से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था।
सामरिक महत्व: 1944 में इंफाल और कोहिमा में अभियान बड़े जापानी यू-गो आक्रामक का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा करना था, जिसे ब्रिटिश आपूर्ति लाइनों को बाधित करने और भारत में आगे बढ़ने की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था।
अभियानों के उद्देश्य
सामरिक स्थानों पर कब्जा: प्राथमिक लक्ष्य इंफाल और कोहिमा शहरों पर कब्जा करना था, जो प्रमुख आपूर्ति मार्गों पर नियंत्रण सक्षम करेगा और INA और जापानी सेना की रसद क्षमताओं में सुधार करेगा।
ब्रिटिश सेना को बाधित करना: इन स्थानों पर कब्जा करके, INA का उद्देश्य क्षेत्र में ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति को कमजोर करना और उपनिवेशवाद के खिलाफ भारतीयों के बीच एक व्यापक विद्रोह को प्रेरित करना था।
इंफाल में अभियान
प्रारंभिक हमला: अभियान मार्च 1944 में शुरू हुआ, जिसमें जापानी और INA सैनिकों ने इंफाल पर हमला किया। योजना में दो-तरफा हमला शामिल था, जिसमें एक बल पूर्व से और दूसरा उत्तर से आगे बढ़ रहा था।
सामना की गई चुनौतियाँ: अभियान को कठिन इलाके, रसद संबंधी मुद्दों और ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल सेनाओं से भयंकर प्रतिरोध सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने इंफाल और उसके आसपास अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी।
गतिरोध और पीछे हटना: जैसे-जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, INA और जापानी सेना को आपूर्ति की कमी और बढ़ती हताहतों का सामना करना पड़ा। जून 1944 तक, आक्रामक रुक गया, और अंततः, INA को सुदृढीकरण की कमी और घटते संसाधनों के कारण पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
कोहिमा में अभियान
ब्रिटिश सेना द्वारा सामरिक रक्षा: कोहिमा महत्वपूर्ण था क्योंकि यह ब्रिटिश सेना के लिए एक प्रमुख रक्षात्मक स्थिति के रूप में कार्य करता था। कोहिमा के लिए लड़ाई इंफाल में लड़ाई के तुरंत बाद शुरू हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने इसके महत्व को पहचाना।
तीव्र लड़ाई: कोहिमा में लड़ाई क्रूर करीबी मुकाबले से चिह्नित थी। भारतीय और अन्य राष्ट्रमंडल सैनिकों द्वारा मजबूत किए गए अंग्रेजों ने दृढ़ रक्षा की, जिससे दोनों पक्षों को भारी हताहत हुए।
मोड़: लड़ाई बर्मा अभियान के व्यापक संदर्भ में एक मोड़ बन गई। ब्रिटिश सेना कोहिमा को संभालने में कामयाब रही, और अप्रैल 1944 तक, INA की स्थिति तेजी से अस्थिर हो गई।
अभियानों के परिणाम
INA की हार: इंफाल और कोहिमा पर कब्जा करने में विफलता INA और जापानी सेना के लिए एक महत्वपूर्ण हार थी। अभियानों के परिणामस्वरूप कर्मियों और मनोबल दोनों के संदर्भ में भारी नुकसान हुआ।
INA पर प्रभाव: इन अभियानों में मिली विफलताओं ने INA की सैन्य क्षमताओं को कमजोर कर दिया और इसके प्रभाव को कम कर दिया। कई सैनिक हार से हतोत्साहित हो गए, और संगठन को एकजुटता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
विरासत और महत्व
प्रतिरोध का प्रतीक: सैन्य विफलताओं के बावजूद, अभियानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध की कथा में योगदान दिया। उन्होंने INA के संकल्प और भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को उजागर किया।
युद्ध के बाद की भावना: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद INA सदस्यों के मुकदमे ने महत्वपूर्ण जन सहानुभूति और आक्रोश जगाया, जिससे भारत में उपनिवेशवाद-विरोधी भावना बढ़ी। इन अभियानों के दौरान किए गए बलिदानों ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में भूमिका निभाई।
INA परीक्षण (1945-46): भारी आक्रोश और नौसेना विद्रोह
पृष्ठभूमि
द्वितीय विश्व युद्ध का संदर्भ: भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA), जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ने युद्ध के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1945 में जापान की हार के बाद, कई INA सैनिकों को ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया।
परीक्षणों का गठन: 1945 के अंत में, ब्रिटिश सरकार ने कई INA अधिकारियों के लिए मुकदमे चलाने का फैसला किया, उन पर राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देशद्रोह का आरोप लगाया। इन परीक्षणों का उद्देश्य उपनिवेश-विरोधी भावनाओं और कार्यों के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में कार्य करना था।
INA परीक्षण
परीक्षण कार्यवाही: परीक्षण नवंबर 1945 में शुरू हुए और इसमें प्रमुख INA नेता शामिल थे, जिनमें मेजर जनरल शाह नवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों शामिल थे।
INA नेताओं के खिलाफ आरोप: अभियुक्तों पर देशद्रोह, साजिश और ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगे। कार्यवाही में उच्च सार्वजनिक रुचि और मीडिया कवरेज था।
जन भावना: परीक्षण राष्ट्रवादी भावनाओं का एक केंद्र बिंदु बन गए, जिसमें भारतीय आबादी के बीच INA नेताओं के लिए व्यापक समर्थन था। कई लोगों ने परीक्षणों को अन्यायपूर्ण और अंग्रेजों द्वारा एक दमनकारी उपाय के रूप में देखा।
भारी आक्रोश
जन विरोध: जैसे ही परीक्षणों की खबर फैली, पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्रों, श्रमिकों और राजनीतिक नेताओं ने INA के साथ एकजुटता में प्रदर्शनों, रैलियों और हड़तालों का आयोजन किया।
राष्ट्रवादी लामबंदी: परीक्षणों ने समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया, जिससे राष्ट्रवादी उत्साह में वृद्धि हुई। विभिन्न राजनीतिक गुटों के प्रमुख नेताओं ने परीक्षणों की निंदा की, जिससे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विविध समूहों को एकजुट किया गया।
मीडिया कवरेज: समाचार पत्रों और प्रकाशनों ने परीक्षणों को बड़े पैमाने पर कवर किया, जिसमें INA नेताओं की बहादुरी पर प्रकाश डाला गया और उन्हें स्वतंत्रता के संघर्ष में नायकों के रूप में चित्रित किया गया। इस मीडिया चित्रण ने जन आक्रोश को और हवा दी।
1946 का नौसेना विद्रोह
पृष्ठभूमि
पृष्ठभूमि: भारतीय नौसेना के भीतर असंतोष खराब कामकाजी परिस्थितियों, कम वेतन और नस्लीय भेदभाव के कारण बढ़ रहा था। INA परीक्षणों ने इस मौजूदा अशांति के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया।
उत्प्रेरक घटना: 18 फरवरी, 1946 को, मुंबई (तब बॉम्बे) में एचएमएस तलवार पर सवार नाविकों ने आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया, जिसमें INA कैदियों के साथ किए गए व्यवहार का विरोध किया गया और बेहतर परिस्थितियों की मांग की गई।
विद्रोह का प्रसार: विद्रोह अन्य जहाजों और नौसेना ठिकानों में तेजी से फैल गया, जिसमें हजारों नाविक शामिल थे। यह ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों से चिह्नित था, जिन्हें अक्सर हिंसा और धमकी का सामना करना पड़ता था।
सरकारी प्रतिक्रिया
विद्रोह का दमन: ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य कर्मियों को तैनात करके बल के साथ प्रतिक्रिया दी। स्थिति हिंसक झड़पों में बढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को हताहत हुए।
बातचीत के प्रयास: विद्रोह के पैमाने और व्यापक अशांति के जवाब में, ब्रिटिश सरकार ने नाविकों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन विश्वास गंभीर रूप से कम हो गया था।
परीक्षणों और विद्रोह की विरासत
स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव: INA परीक्षणों और नौसेना विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ बढ़ती असंतोष और भारतीयों की उत्पीड़न का विरोध करने की इच्छा को प्रदर्शित किया।
ब्रिटिश नीति में बदलाव: घटनाओं के कारण भारत में ब्रिटिश नीतियों का पुनर्मूल्यांकन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सुधारों की आवश्यकता को पहचाना और भारतीय स्व-शासन की दिशा में एक संक्रमण पर विचार करना शुरू कर दिया।
प्रतिरोध का प्रतीक: परीक्षण और विद्रोह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए, जिसने भविष्य के आंदोलनों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में भारतीयों के बीच एकता के महत्व पर जोर दिया।
MCQ:-
1. [2019-सेट डी, प्रश्न 51]
प्रश्न: भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- INA का गठन 1942 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था।
- INA ने ब्रिटिश के खिलाफ जापानी सेना के साथ लड़ाई लड़ी।
- INA परीक्षण दिल्ली के लाल किले में हुए थे।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
विकल्प:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b) केवल 2 और 3
2. [2018-सेट डी, प्रश्न 29]
प्रश्न: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें:
- रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह
- भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया
- INA परीक्षण
- तेभागा आंदोलन
उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है?
विकल्प:
(a) 2-1-3-
(b) 2-3-1-4
(c) 4-2-1-3
(d) 1-2-3-4
उत्तर: (b) 2-3-1-4
3. [2014-सेट ए, प्रश्न 27]
प्रश्न: 1945 का ‘लाल किला परीक्षण’ किससे संबंधित है:
(a) INA अधिकारियों का परीक्षण
(b) भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का परीक्षण
(c) रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों का परीक्षण
(d) सुभाष चंद्र बोस का परीक्षण
उत्तर: (a) INA अधिकारियों का परीक्षण
4. [2011-सेट ए, प्रश्न 48]
प्रश्न: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, निम्नलिखित में से किसने “फ्री इंडियन लीजन” नामक एक सेना खड़ी की?
विकल्प:
(a) लाला हरदयाल
(b) रास बिहारी बोस
(c) सुभाष चंद्र बोस
(d) वी.डी. सावरकर
उत्तर: (c) सुभाष चंद्र बोस
5. [2009-सेट ए, प्रश्न 93]
प्रश्न: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) 1943 में अस्तित्व में आई:
(a) जापान में
(b) तब बर्मा में
(c) सिंगापुर में
(d) तब मलाया में
उत्तर: (c) सिंगापुर